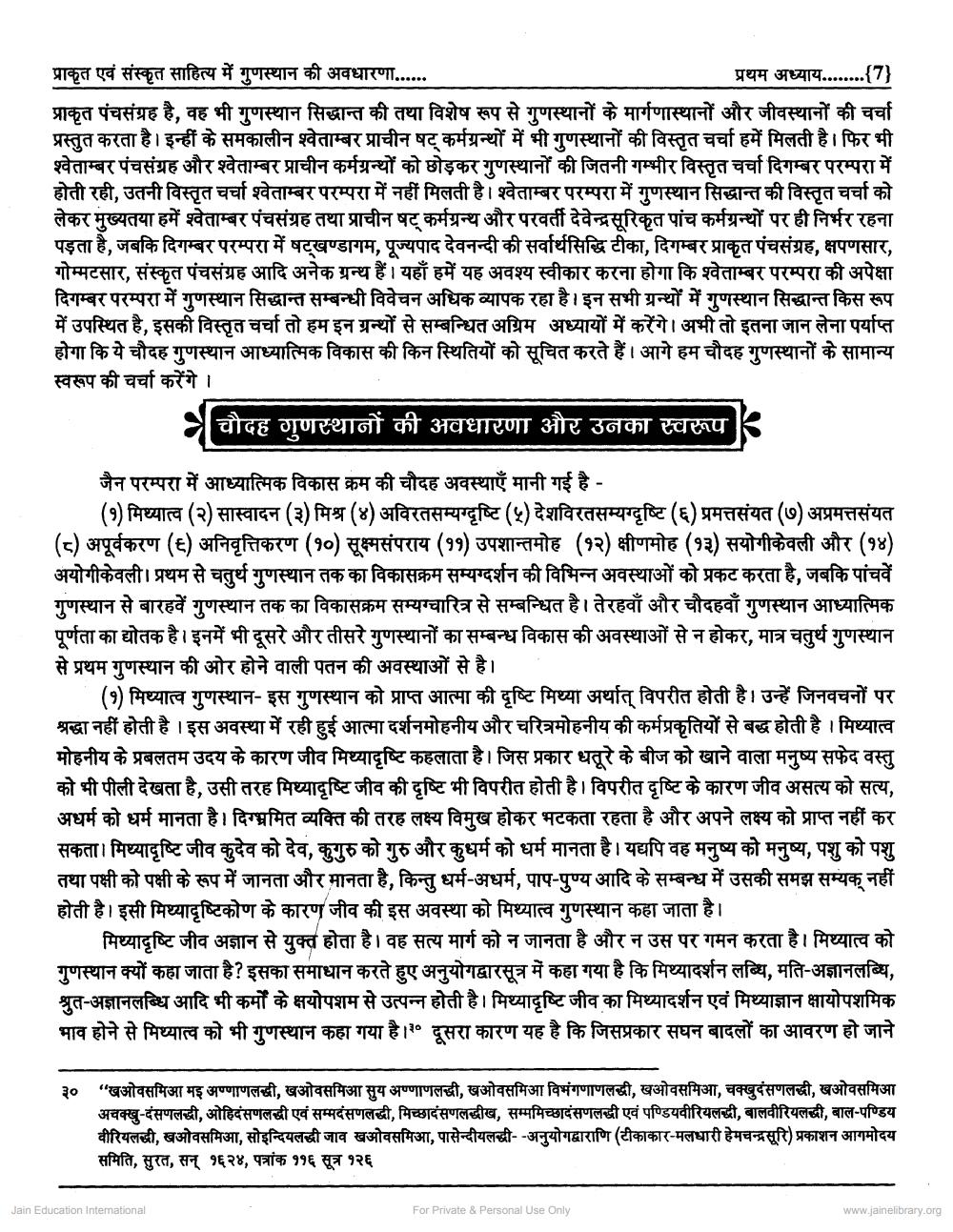________________
प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में गुणस्थान की अवधारणा........
प्रथम अध्याय.....{7} प्राकृत पंचसंग्रह है, वह भी गुणस्थान सिद्धान्त की तथा विशेष रूप से गुणस्थानों के मार्गणास्थानों और जीवस्थानों की चर्चा प्रस्तुत करता है। इन्हीं के समकालीन श्वेताम्बर प्राचीन षट् कर्मग्रन्थों में भी गुणस्थानों की विस्तृत चर्चा हमें मिलती है। फिर भी श्वेताम्बर पंचसंग्रह और श्वेताम्बर प्राचीन कर्मग्रन्थों को छोड़कर गुणस्थानों की जितनी गम्भीर विस्तृत चर्चा दिगम्बर परम्परा में होती रही, उतनी विस्तृत चर्चा श्वेताम्बर परम्परा में नहीं मिलती है। श्वेताम्बर परम्परा में गुणस्थान सिद्धान्त की विस्तृत चर्चा को लेकर मुख्यतया हमें श्वेताम्बर पंचसंग्रह तथा प्राचीन षट् कर्मग्रन्थ और परवर्ती देवेन्द्रसूरिकृत पांच कर्मग्रन्थों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जबकि दिगम्बर परम्परा में षट्खण्डागम, पूज्यपाद देवनन्दी की सर्वार्थसिद्धि टीका, दिगम्बर प्राकृत पंचसंग्रह, क्षपणसार, गोम्मटसार, संस्कृत पंचसंग्रह आदि अनेक ग्रन्थ हैं। यहाँ हमें यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि श्वेताम्बर परम्परा की अपेक्षा दिगम्बर परम्परा में गुणस्थान सिद्धान्त सम्बन्धी विवेचन अधिक व्यापक रहा है। इन सभी ग्रन्थों में गुणस्थान सिद्धान्त किस रूप में उपस्थित है, इसकी विस्तृत चर्चा तो हम इन ग्रन्थों से सम्बन्धित अग्रिम अध्यायों में करेंगे। अभी तो इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि ये चौदह गुणस्थान आध्यात्मिक विकास की किन स्थितियों को सूचित करते हैं। आगे हम चौदह गुणस्थानों के सामान्य स्वरूप की चर्चा करेंगे ।
चौदह गुणस्थानों की अवधारणा और उनका स्वरूप
जैन परम्परा में आध्यात्मिक विकास क्रम की चौदह अवस्थाएँ मानी गई है.
-
(१) मिथ्यात्व (२) सास्वादन (३) मिश्र (४) अविरतसम्यग्दृष्टि (५) देशविरतसम्यग्दृष्टि (६) प्रमत्तसंयत (७) अप्रमत्तसंयत (८) अपूर्वकरण (६) अनिवृत्तिकरण (१०) सूक्ष्मसंपराय ( ११ ) उपशान्तमोह (१२) क्षीणमोह (१३) सयोगीकेवली और (१४) अयोगीकेवली। प्रथम से चतुर्थ गुणस्थान तक का विकासक्रम सम्यग्दर्शन की विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करता है, जबकि पांचवें गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक का विकासक्रम सम्यग्चारित्र से सम्बन्धित है । तेरहवाँ और चौदहवाँ गुणस्थान आध्यात्मिक पूर्णता का द्योतक है। इनमें भी दूसरे और तीसरे गुणस्थानों का सम्बन्ध विकास की अवस्थाओं से न होकर, मात्र चतुर्थ गुणस्थान प्रथम गुणस्थान की ओर होने वाली पतन की अवस्थाओं से है ।
३०
(१) मिथ्यात्व गुणस्थान- इस गुणस्थान को प्राप्त आत्मा की दृष्टि मिथ्या अर्थात् विपरीत होती है। उन्हें जिनवचनों पर श्रद्धा नहीं होती है । इस अवस्था में रही हुई आत्मा दर्शनमोहनीय और चरित्रमोहनीय की कर्मप्रकृतियों से बद्ध होती है । मिथ्यात्व मोहनीय के प्रबलतम उदय के कारण जीव मिथ्यादृष्टि कहलाता है। जिस प्रकार धतूरे के बीज को खाने वाला मनुष्य 'सफेद वस्तु को भी पीली देखता है, उसी तरह मिथ्यादृष्टि जीव की दृष्टि भी विपरीत होती है। विपरीत दृष्टि के कारण जीव असत्य को सत्य, अधर्म को धर्म मानता है। दिग्भ्रमित व्यक्ति की तरह लक्ष्य विमुख होकर भटकता रहता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। मिथ्यादृष्टि जीव कुदेव को देव, कुगुरु को गुरु और कुधर्म को धर्म मानता है। यद्यपि वह मनुष्य को मनुष्य, पशु को पशु तथा पक्षी को पक्षी के रूप में जानता और मानता है, किन्तु धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य आदि के सम्बन्ध में उसकी समझ सम्यक् नहीं होती है। इसी मिथ्यादृष्टिकोण के कारण जीव की इस अवस्था को मिथ्यात्व गुणस्थान कहा जाता |
मिथ्यादृष्टि जीव अज्ञान से युक्त होता है। वह सत्य मार्ग को न जानता है और न उस पर गमन करता है । मिथ्यात्व को गुणस्थान क्यों कहा जाता है ? इसका समाधान करते हुए अनुयोगद्वारसूत्र में कहा गया है कि मिथ्यादर्शन लब्धि, मति - अज्ञानलब्धि, श्रुत- अज्ञानलब्धि आदि भी कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होती है। मिथ्यादृष्टि जीव का मिथ्यादर्शन एवं मिथ्याज्ञान क्षायोपशमिक भाव होने से मिथ्यात्व को भी गुणस्थान कहा गया है। दूसरा कारण यह है कि जिसप्रकार सघन बादलों का आवरण हो जाने
“खओवसमिआ मइ अण्णाणली, खओवसमिआ सुय अण्णाणलद्धी, खओवसमिआ विभंगणाणलद्धी, खओवसमिआ, चक्खुदंसणलद्धी, खओवसमिआ अचक्खु - दंसणलद्धी, ओहिदंसणलद्धी एवं सम्मदंसणलद्धी, मिच्छादंसणलद्धीख, सम्ममिच्छादंसणलद्धी एवं पण्डियवीरियलन्दी, बालवीरियलद्धी, बाल-पण्डिय वीरियलद्धी, खओवसमिआ, सोइन्दियलद्धी जाव खओवसमिआ, पासेन्दीयली- अनुयोगद्वाराणि (टीकाकार-मलधारी हेमचन्द्रसूरि ) प्रकाशन आगमोदय समिति, सुरत, सन् १६२४, पत्रांक ११६ सूत्र १२६
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org