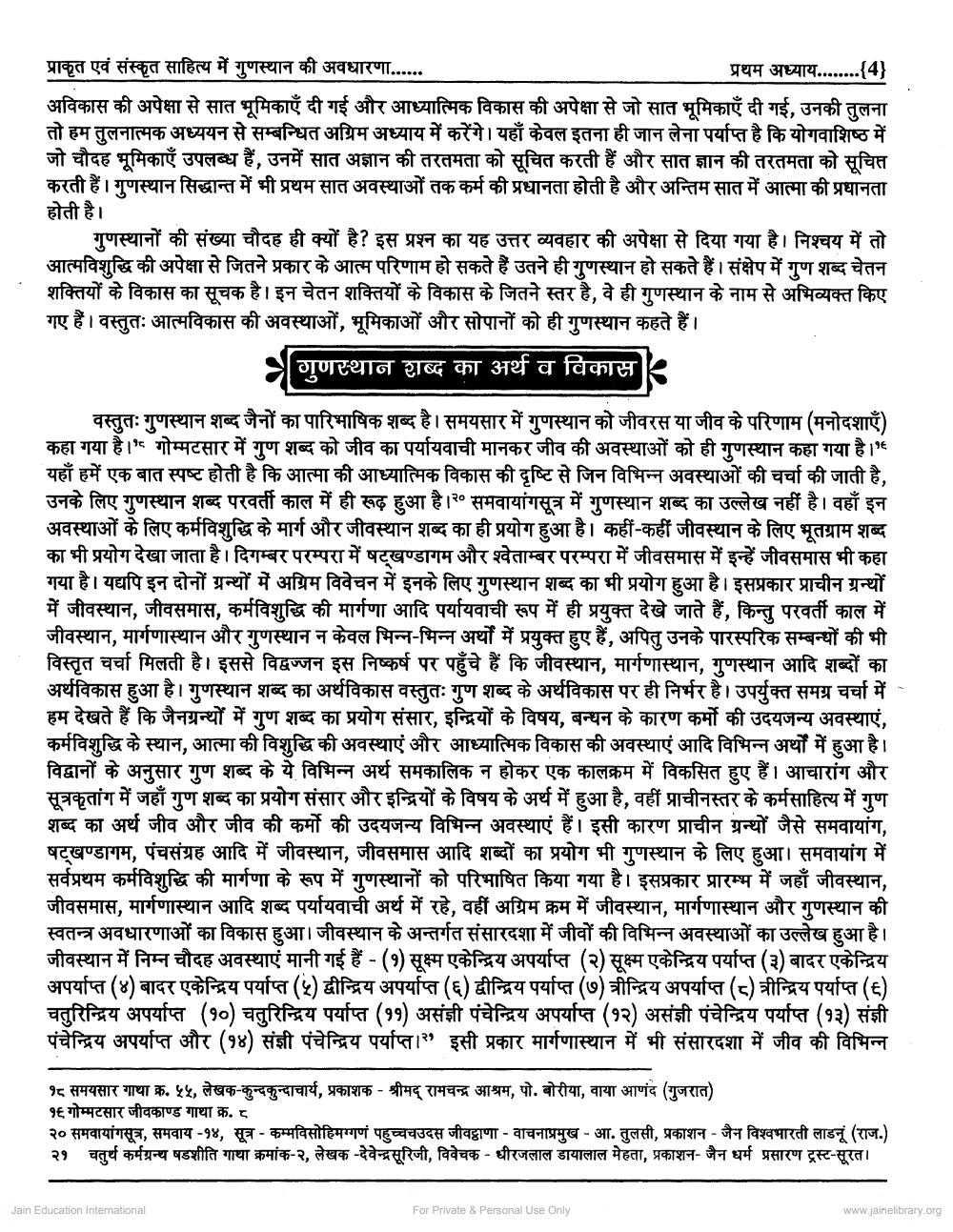________________
प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में गुणस्थान की अवधारणा......
प्रथम अध्याय........{4} अविकास की अपेक्षा से सात भूमिकाएँ दी गई और आध्यात्मिक विकास की अपेक्षा से जो सात भूमिकाएँ दी गई, उनकी तुलना तो हम तुलनात्मक अध्ययन से सम्बन्धित अग्रिम अध्याय में करेंगे। यहाँ केवल इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि योगवाशिष्ठ में जो चौदह भूमिकाएँ उपलब्ध हैं, उनमें सात अज्ञान की तरतमता को सूचित करती हैं और सात ज्ञान की तरतमता को सूचित करती हैं। गुणस्थान सिद्धान्त में भी प्रथम सात अवस्थाओं तक कर्म की प्रधानता होती है और अन्तिम सात में आत्मा की प्रधानता होती है।
गुणस्थानों की संख्या चौदह ही क्यों है? इस प्रश्न का यह उत्तर व्यवहार की अपेक्षा से दिया गया है। निश्चय में तो आत्मविशद्धि की अपेक्षा से जितने प्रकार के आत्म परिणाम हो सकते हैं उतने ही गुणस्थान हो सकते हैं। संक्षेप में गुण शब्द चेतन शक्तियों के विकास का सूचक है। इन चेतन शक्तियों के विकास के जितने स्तर है, वे ही गुणस्थान के नाम से अभिव्यक्त किए गए हैं। वस्तुतः आत्मविकास की अवस्थाओं, भूमिकाओं और सोपानों को ही गुणस्थान कहते हैं।
गुणस्थान शब्द का अर्थ व विकास
वस्तुतः गुणस्थान शब्द जैनों का पारिभाषिक शब्द है। समयसार में गुणस्थान को जीवरस या जीव के परिणाम (मनोदशाएँ) कहा गया है। गोम्मटसार में गुण शब्द को जीव का पर्यायवाची मानकर जीव की अवस्थाओं को ही गुणस्थान कहा गया है।१६ यहाँ हमें एक बात स्पष्ट होती है कि आत्मा की आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से जिन विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा की जाती है, उनके लिए गुणस्थान शब्द परवर्ती काल में ही रूढ़ हुआ है।२० समवायांगसूत्र में गुणस्थान शब्द का उल्लेख नहीं है। वहाँ इन अवस्थाओं के लिए कर्मविशुद्धि के मार्ग और जीवस्थान शब्द का ही प्रयोग हुआ है। कहीं-कहीं जीवस्थान के लिए भूतग्राम शब्द का भी प्रयोग देखा जाता है। दिगम्बर परम्परा में षट्खण्डागम और श्वेताम्बर परम्परा में जीवसमास में इन्हें जीवसमास भी कहा गया है। यद्यपि इन दोनों ग्रन्थों में अग्रिम विवेचन में इनके लिए गुणस्थान शब्द का भी प्रयोग हुआ है। इसप्रकार प्राचीन ग्रन्थों में जीवस्थान, जीवसमास, कर्मविशुद्धि की मार्गणा आदि पर्यायवाची रूप में ही प्रयुक्त देखे जाते हैं, किन्तु परवर्ती काल में जीवस्थान, मार्गणास्थान और गुणस्थान न केवल भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं, अपितु उनके पारस्परिक सम्बन्धों की भी
मलती है। इससे विद्वज्जन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जीवस्थान, मार्गणास्थान, गुणस्थान आदि शब्दों का अर्थविकास हुआ है। गुणस्थान शब्द का अर्थविकास वस्तुतः गुण शब्द के अर्थविकास पर ही निर्भर है। उपर्युक्त समग्र चर्चा में - हम देखते हैं कि जैनग्रन्थों में गुण शब्द का प्रयोग संसार, इन्द्रियों के विषय, बन्धन के कारण कर्मों की उदयजन्य अवस्थाएं, कर्मविशुद्धि के स्थान, आत्मा की विशुद्धि की अवस्थाएं और आध्यात्मिक विकास की अवस्थाएं आदि विभिन्न अर्थों में हुआ है। विद्वानों के अनुसार गुण शब्द के ये विभिन्न अर्थ समकालिक न होकर एक कालक्रम में विकसित हुए हैं। आचारांग और सूत्रकृतांग में जहाँ गुण शब्द का प्रयोग संसार और इन्द्रियों के विषय के अर्थ में हुआ है, वहीं प्राचीनस्तर के कर्मसाहित्य में गुण शब्द का अर्थ जीव और जीव की कर्मो की उदयजन्य विभिन्न अवस्थाएं हैं। इसी कारण प्राचीन ग्रन्थों जैसे समवायांग, षट्खण्डागम, पंचसंग्रह आदि में जीवस्थान, जीवसमास आदि शब्दों का प्रयोग भी गुणस्थान के लिए हुआ। समवायांग में सर्वप्रथम कर्मविशुद्धि की मार्गणा के रूप में गुणस्थानों को परिभाषित किया गया है। इसप्रकार प्रारम्भ में जहाँ जीवस्थान, जीवसमास, मार्गणास्थान आदि शब्द पर्यायवाची अर्थ में रहे, वहीं अग्रिम क्रम में जीवस्थान, मार्गणास्थान और गणस्थान की स्वतन्त्र अवधारणाओं का विकास हुआ। जीवस्थान के अन्तर्गत संसारदशा में जीवों की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख हुआ है। जीवस्थान में निम्न चौदह अवस्थाएं मानी गई हैं - (१) सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त (२) सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त (३) बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त (४) बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त (५) द्वीन्द्रिय अपर्याप्त (६) द्वीन्द्रिय पर्याप्त (७) त्रीन्द्रिय अपर्याप्त (८) त्रीन्द्रिय पर्याप्त (E) चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त (१०) चतुरिन्द्रिय पर्याप्त (११) असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त (१२) असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त (१३) संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त और (१४) संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त।" इसी प्रकार मार्गणास्थान में भी संसारदशा में जीव की विभिन्न
१८ समयसार गाथा क्र. ५५, लेखक-कुन्दकुन्दाचार्य, प्रकाशक - श्रीमद् रामचन्द्र आश्रम, पो. बोरीया, वाया आणंद (गुजरात) १६ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा क्र.८ २० समवायांगसूत्र, समवाय -१४, सूत्र - कम्मविसोहिमग्गणं पहुच्चचउदस जीवट्ठाणा - वाचनाप्रमुख - आ. तुलसी, प्रकाशन - जैन विश्वभारती लाडनूं (राज.) २१ चतुर्थ कर्मग्रन्थ षडशीति गाथा क्रमांक-२, लेखक -देवेन्द्रसूरिजी, विवेचक - धीरजलाल डायालाल मेहता, प्रकाशन- जैन धर्म प्रसारण ट्रस्ट-सूरत।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org