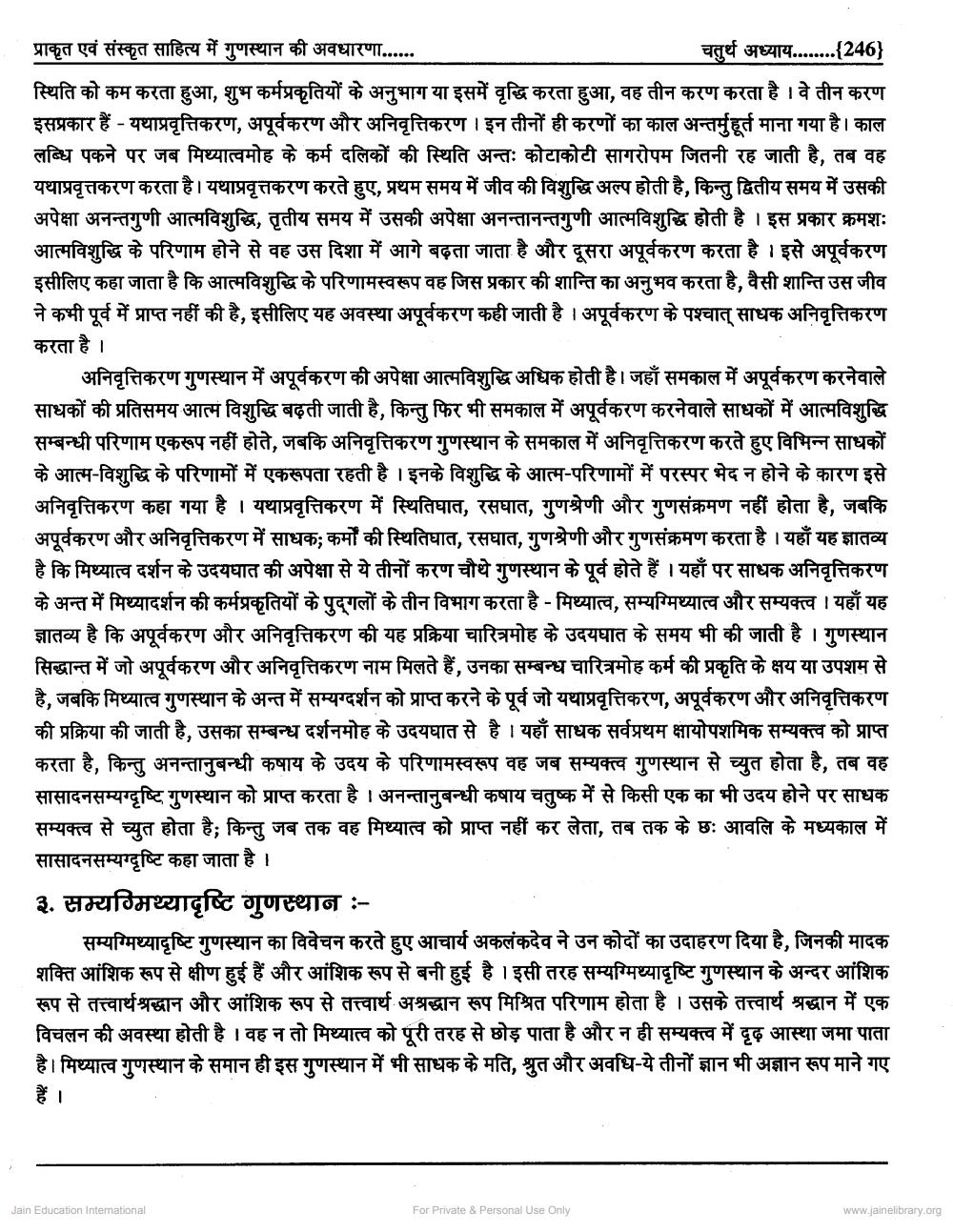________________
प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में गणस्थान की अवधारणा......
चतुर्थ अध्याय........{246} स्थिति को कम करता हुआ, शुभ कर्मप्रकृतियों के अनुभाग या इसमें वृद्धि करता हुआ, वह तीन करण करता है । वे तीन करण इसप्रकार हैं - यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण । इन तीनों ही करणों का काल अन्तर्मुहूर्त माना गया है। काल लब्धि पकने पर जब मिथ्यात्वमोह के कर्म दलिकों की स्थिति अन्तः कोटाकोटी सागरोपम जितनी रह जाती है, तब वह यथाप्रवृत्तकरण करता है। यथाप्रवृत्तकरण करते हुए, प्रथम समय में जीव की विशुद्धि अल्प होती है, किन्तु द्वितीय समय में उसकी अपेक्षा अनन्तगुणी आत्मविशुद्धि, तृतीय समय में उसकी अपेक्षा अनन्तानन्तगुणी आत्मविशुद्धि होती है । इस प्रकार क्रमशः आत्मविशुद्धि के परिणाम होने से वह उस दिशा में आगे बढ़ता जाता है और दूसरा अपूर्वकरण करता है । इसे अपूर्वकरण इसीलिए कहा जाता है कि आत्मविशुद्धि के परिणामस्वरूप वह जिस प्रकार की शान्ति का अनुभव करता है, वैसी शान्ति उस जीव ने कभी पूर्व में प्राप्त नहीं की है, इसीलिए यह अवस्था अपूर्वकरण कही जाती है । अपूर्वकरण के पश्चात् साधक अनिवृत्तिकरण करता है।
अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में अपूर्वकरण की अपेक्षा आत्मविशुद्धि अधिक होती है। जहाँ समकाल में अपूर्वकरण करनेवाले साधकों की प्रतिसमय आत्म विशुद्धि बढ़ती जाती है, किन्तु फिर भी समकाल में अपूर्वकरण करनेवाले साधकों में आत्मविशुद्धि सम्बन्धी परिणाम एकरूप नहीं होते, जबकि अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के समकाल में अनिवृत्तिकरण करते हुए विभिन्न साधकों के आत्म-विशुद्धि के परिणामों में एकरूपता रहती है । इनके विशुद्धि के आत्म-परिणामों में परस्पर भेद न होने के कारण इसे अनिवृत्तिकरण कहा गया है । यथाप्रवृत्तिकरण में स्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणी और गुणसंक्रमण नहीं होता है, जबकि अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में साधक; कर्मों की स्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणी और गुणसंक्रमण करता है । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि मिथ्यात्व दर्शन के उदयघात की अपेक्षा से ये तीनों करण चौथे गुणस्थान के पूर्व होते हैं । यहाँ पर साधक अनिवृत्तिकरण के अन्त में मिथ्यादर्शन की कर्मप्रकृतियों के पुद्गलों के तीन विभाग करता है - मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण की यह प्रक्रिया चारित्रमोह के उदयघात के समय भी की जाती है । गुणस्थान सिद्धान्त में जो अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नाम मिलते हैं, उनका सम्बन्ध चारित्रमोह कर्म की प्रकृति के क्षय या उपशम से है, जबकि मिथ्यात्व गुणस्थान के अन्त में सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने के पूर्व जो यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण की प्रक्रिया की जाती है, उसका सम्बन्ध दर्शनमोह के उदयघात से है । यहाँ साधक सर्वप्रथम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, किन्तु अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय के परिणामस्वरूप वह जब सम्यक्त्व गुणस्थान से च्युत होता है, तब वह सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थान को प्राप्त करता है । अनन्तानुबन्धी कषाय चतुष्क में से किसी एक का भी उदय होने पर साधक सम्यक्त्व से च्युत होता है; किन्तु जब तक वह मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक के छः आवलि के मध्यकाल में सासादनसम्यग्दृष्टि कहा जाता है । ३. सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान :
सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान का विवेचन करते हुए आचार्य अकलंकदेव ने उन कोदों का उदाहरण दिया है, जिनकी मादक शक्ति आंशिक रूप से क्षीण हुई हैं और आंशिक रूप से बनी हुई है । इसी तरह सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान के अन्दर आंशिक रूप से तत्त्वार्थश्रद्धान और आंशिक रूप से तत्त्वार्थ अश्रद्धान रूप मिश्रित परिणाम होता है । उसके तत्त्वार्थ श्रद्धान में एक विचलन की अवस्था होती है । वह न तो मिथ्यात्व को पूरी तरह से छोड़ पाता है और न ही सम्यक्त्व में दृढ़ आस्था जमा पाता है। मिथ्यात्व गुणस्थान के समान ही इस गुणस्थान में भी साधक के मति, श्रुत और अवधि-ये तीनों ज्ञान भी अज्ञान रूप माने गए
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org