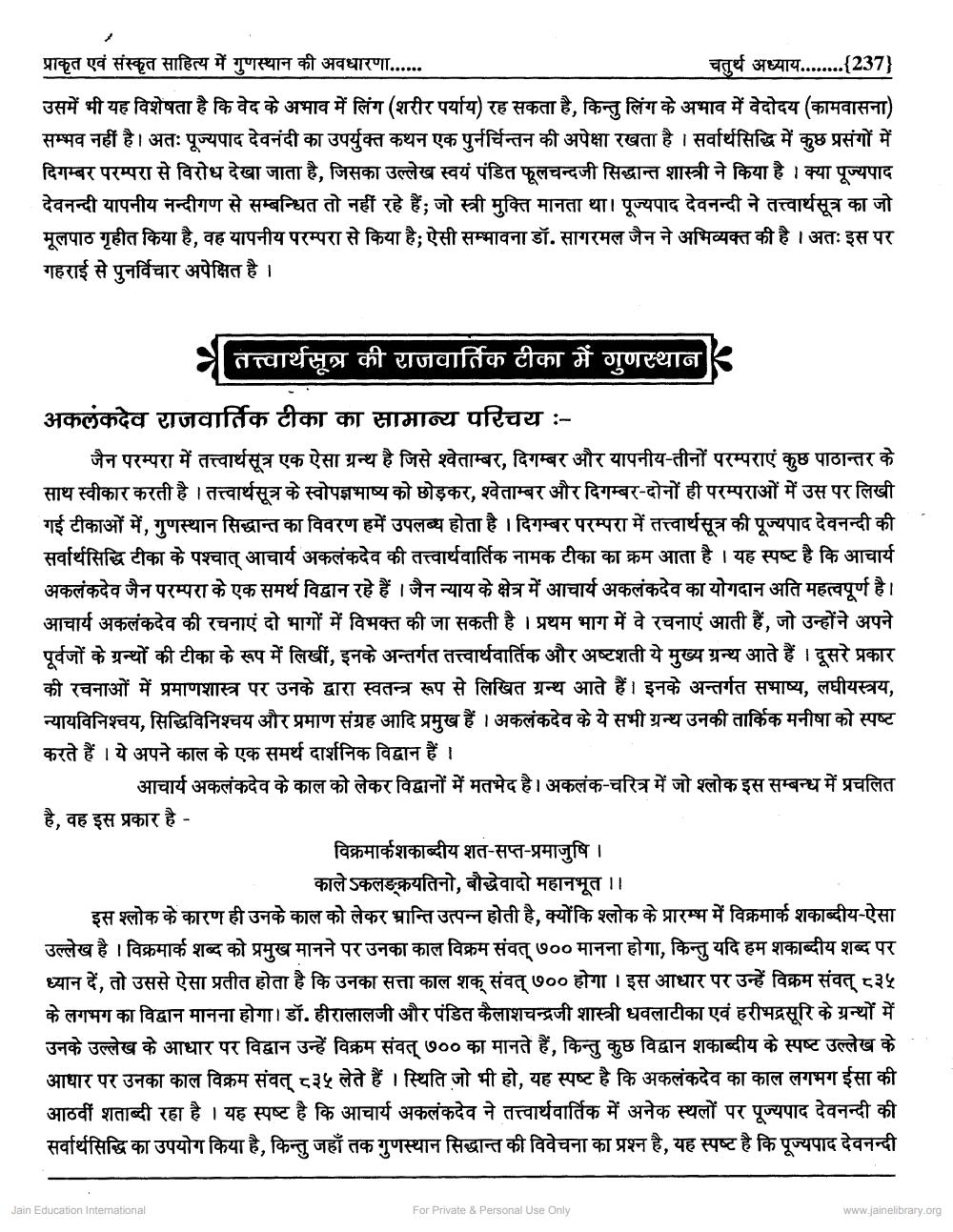________________
प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में गुणस्थान की अवधारणा......
चतुर्थ अध्याय........{237} उसमें भी यह विशेषता है कि वेद के अभाव में लिंग (शरीर पर्याय) रह सकता है, किन्तु लिंग के अभाव में वेदोदय (कामवासना) सम्भव नहीं है। अतः पूज्यपाद देवनंदी का उपर्युक्त कथन एक पुर्नचिन्तन की अपेक्षा रखता है । सर्वार्थसिद्धि में कुछ प्रसंगों में दिगम्बर परम्परा से विरोध देखा जाता है, जिसका उल्लेख स्वयं पंडित फूलचन्दजी सिद्धान्त शास्त्री ने किया है । क्या पूज्यपाद देवनन्दी यापनीय नन्दीगण से सम्बन्धित तो नहीं रहे हैं; जो स्त्री मुक्ति मानता था। पूज्यपाद देवनन्दी ने तत्त्वार्थसूत्र का जो मूलपाठ गृहीत किया है, वह यापनीय परम्परा से किया है; ऐसी सम्भावना डॉ. सागरमल जैन ने अभिव्यक्त की है । अतः इस पर गहराई से पुनर्विचार अपेक्षित है ।
तत्त्वार्थसूत्र की राजवार्तिक टीका में गुणस्थान अकलंकदेव राजवार्तिक टीका का सामान्य परिचय :
जैन परम्परा में तत्त्वार्थसूत्र एक ऐसा ग्रन्थ है जिसे श्वेताम्बर, दिगम्बर और यापनीय-तीनों परम्पराएं कुछ पाठान्तर के साथ स्वीकार करती है । तत्त्वार्थसूत्र के स्वोपज्ञभाष्य को छोड़कर, श्वेताम्बर और दिगम्बर-दोनों ही परम्पराओं में उस पर लिखी गई टीकाओं में, गुणस्थान सिद्धान्त का विवरण हमें उपलब्ध होता है । दिगम्बर परम्परा में तत्त्वार्थसूत्र की पूज्यपाद देवनन्दी की सर्वार्थसिद्धि टीका के पश्चात् आचार्य अकलंकदेव की तत्त्वार्थवार्तिक नामक टीका का क्रम आता है । यह स्पष्ट है कि आचार्य अकलंकदेव जैन परम्परा के एक समर्थ विद्वान रहे हैं । जैन न्याय के क्षेत्र में आचार्य अकलंकदेव का योगदान अति महत्वपूर्ण है। आचार्य अकलंकदेव की रचनाएं दो भागों में विभक्त की जा सकती है । प्रथम भाग में वे रचनाएं आती हैं, जो उन्होंने अपने पूर्वजों के ग्रन्थों की टीका के रूप में लिखीं, इनके अन्तर्गत तत्त्वार्थवार्तिक और अष्टशती ये मुख्य ग्रन्थ आते हैं । दूसरे प्रकार की रचनाओं में प्रमाणशास्त्र पर उनके द्वारा स्वतन्त्र रूप से लिखित ग्रन्थ आते हैं। इनके अन्तर्गत सभाष्य, लघीयस्त्रय, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय और प्रमाण संग्रह आदि प्रमुख हैं। अकलंकदेव के ये सभी ग्रन्थ उनकी तार्किक मनीषा को स्पष्ट करते हैं । ये अपने काल के एक समर्थ दार्शनिक विद्वान हैं।
आचार्य अकलंकदेव के काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अकलंक-चरित्र में जो श्लोक इस सम्बन्ध में प्रचलित है, वह इस प्रकार है
विक्रमार्कशकाब्दीय शत-सप्त-प्रमाजुषि ।
कालेऽकलङ्कयतिनो, बौद्धेवादो महानभूत ।। इस श्लोक के कारण ही उनके काल को लेकर भ्रान्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि श्लोक के प्रारम्भ में विक्रमार्क शकाब्दीय-ऐसा उल्लेख है । विक्रमार्क शब्द को प्रमुख मानने पर उनका काल विक्रम संवत् ७०० मानना होगा, किन्तु यदि हम शकाब्दीय शब्द पर ध्यान दें, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका सत्ता काल शक संवत् ७०० होगा। इस आधार पर उन्हें विक्रम संवत् ८३५ के लगभग का विद्वान मानना होगा। डॉ.हीरालालजी और पंडित कैलाशचन्द्रजी शास्त्री धवलाटीका एवं हरीभद्रसूरि के ग्रन्थों में उनके उल्लेख के आधार पर विद्वान उन्हें विक्रम संवत् ७०० का मानते हैं, किन्तु कुछ विद्वान शकाब्दीय के स्पष्ट उल्लेख के आधार पर उनका काल विक्रम संवत् ८३५ लेते हैं । स्थिति जो भी हो, यह स्पष्ट है कि अकलंकदेव का काल लगभग ईसा की आठवीं शताब्दी रहा है । यह स्पष्ट है कि आचार्य अकलंकदेव ने तत्त्वार्थवार्तिक में अनेक स्थलों पर पूज्यपाद देवनन्दी की सर्वार्थसिद्धि का उपयोग किया है, किन्तु जहाँ तक गुणस्थान सिद्धान्त की विवेचना का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि पूज्यपाद देवनन्दी
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org