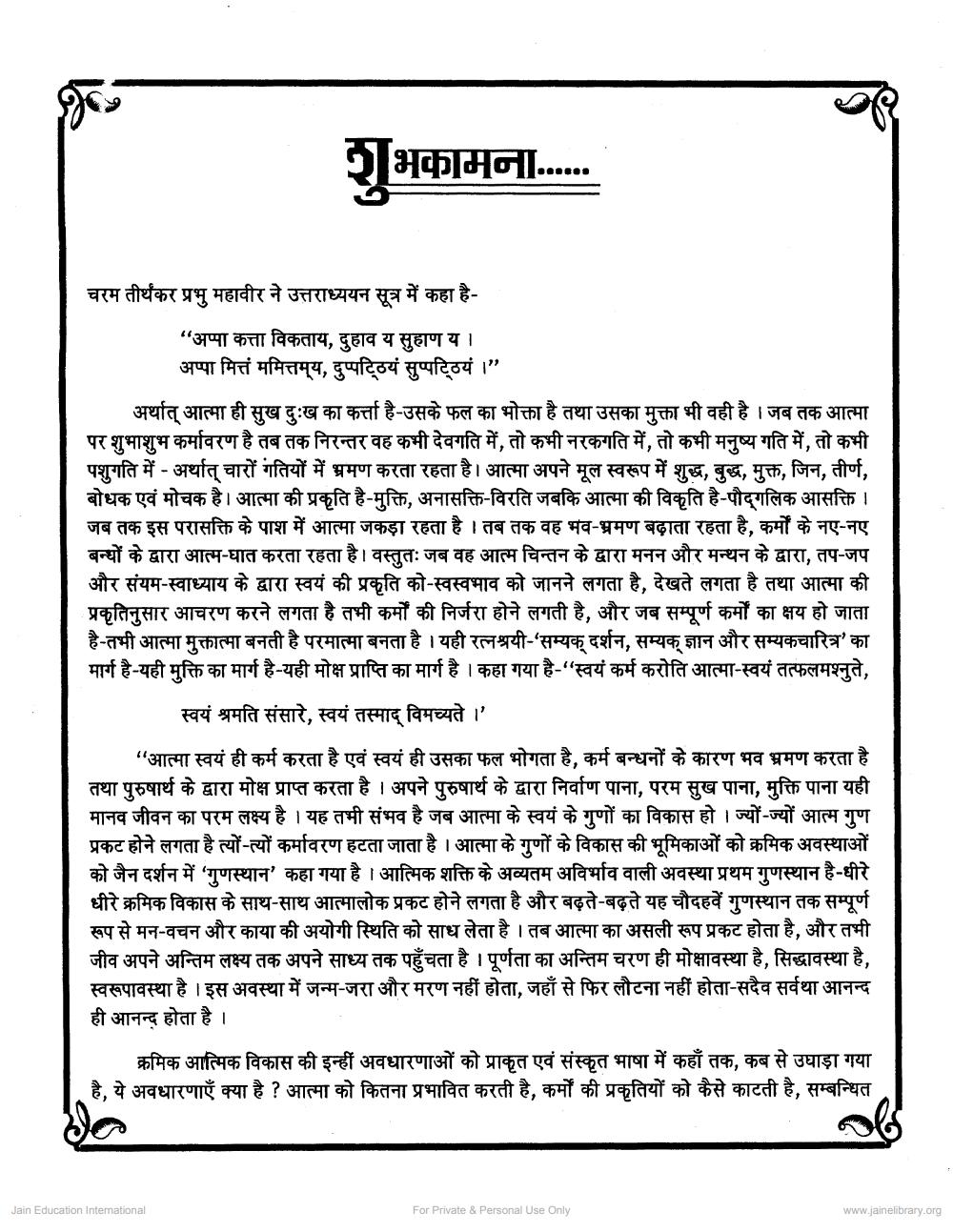________________
शुभकामना.
चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है
"अप्पा कत्ता विकताय, दुहाव य सुहाण य ।
अप्पा मित्तं ममित्तम्य, दुप्पट्ठियं सुप्पट्ठियं ।" अर्थात् आत्मा ही सुख दुःख का कर्ता है-उसके फल का भोक्ता है तथा उसका मुक्ता भी वही है । जब तक आत्मा पर शुभाशुभ कर्मावरण है तब तक निरन्तर वह कभी देवगति में, तो कभी नरकगति में, तो कभी मनुष्य गति में, तो कभी पशुगति में - अर्थात् चारों गतियों में भ्रमण करता रहता है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, जिन, तीर्ण, बोधक एवं मोचक है। आत्मा की प्रकृति है-मुक्ति, अनासक्ति-विरति जबकि आत्मा की विकृति है-पौद्गलिक आसक्ति । जब तक इस परासक्ति के पाश में आत्मा जकड़ा रहता है । तब तक वह भव-भ्रमण बढ़ाता रहता है, कर्मों के नए-नए बन्धों के द्वारा आत्म-घात करता रहता है। वस्तुतः जब वह आत्म चिन्तन के द्वारा मनन और मन्थन के द्वारा, तप-जप
और संयम-स्वाध्याय के द्वारा स्वयं की प्रकृति को-स्वस्वभाव को जानने लगता है, देखते लगता है तथा आत्मा की प्रकृतिनुसार आचरण करने लगता है तभी कर्मों की निर्जरा होने लगती है, और जब सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है-तभी आत्मा मुक्तात्मा बनती है परमात्मा बनता है। यही रत्नश्रयी-'सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यकचारित्र' का मार्ग है-यही मुक्ति का मार्ग है-यही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। कहा गया है-"स्वयं कर्म करोति आत्मा-स्वयं तत्फलमश्नुते,
स्वयं श्रमति संसारे, स्वयं तस्माद विमच्यते ।'
"आत्मा स्वयं ही कर्म करता है एवं स्वयं ही उसका फल भोगता है, कर्म बन्धनों के कारण भव भ्रमण करता है तथा पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है । अपने पुरुषार्थ के द्वारा निर्वाण पाना, परम सुख पाना, मुक्ति पाना यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है । यह तभी संभव है जब आत्मा के स्वयं के गुणों का विकास हो । ज्यों-ज्यों आत्म गुण प्रकट होने लगता है त्यों-त्यों कर्मावरण हटता जाता है । आत्मा के गुणों के विकास की भूमिकाओं को क्रमिक अवस्थाओं को जैन दर्शन में 'गणस्थान' कहा गया है । आत्मिक शक्ति के अव्यतम अविर्भाव वाली अवस्था प्रथम गुणस्थान है-धीरे धीरे क्रमिक विकास के साथ-साथ आत्मालोक प्रकट होने लगता है और बढ़ते-बढ़ते यह चौदहवें गुणस्थान तक सम्पूर्ण रूप से मन-वचन और काया की अयोगी स्थिति को साध लेता है । तब आत्मा का असली रूप प्रकट होता है, और तभी जीव अपने अन्तिम लक्ष्य तक अपने साध्य तक पहुँचता है । पूर्णता का अन्तिम चरण ही मोक्षावस्था है, सिद्धावस्था है, स्वरूपावस्था है । इस अवस्था में जन्म-जरा और मरण नहीं होता, जहाँ से फिर लौटना नहीं होता-सदैव सर्वथा आनन्द ही आनन्द होता है।
क्रमिक आत्मिक विकास की इन्हीं अवधारणाओं को प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में कहाँ तक, कब से उघाड़ा गया है, ये अवधारणाएँ क्या है ? आत्मा को कितना प्रभावित करती है, कर्मों की प्रकृतियों को कैसे काटती है, सम्बन्धित
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org