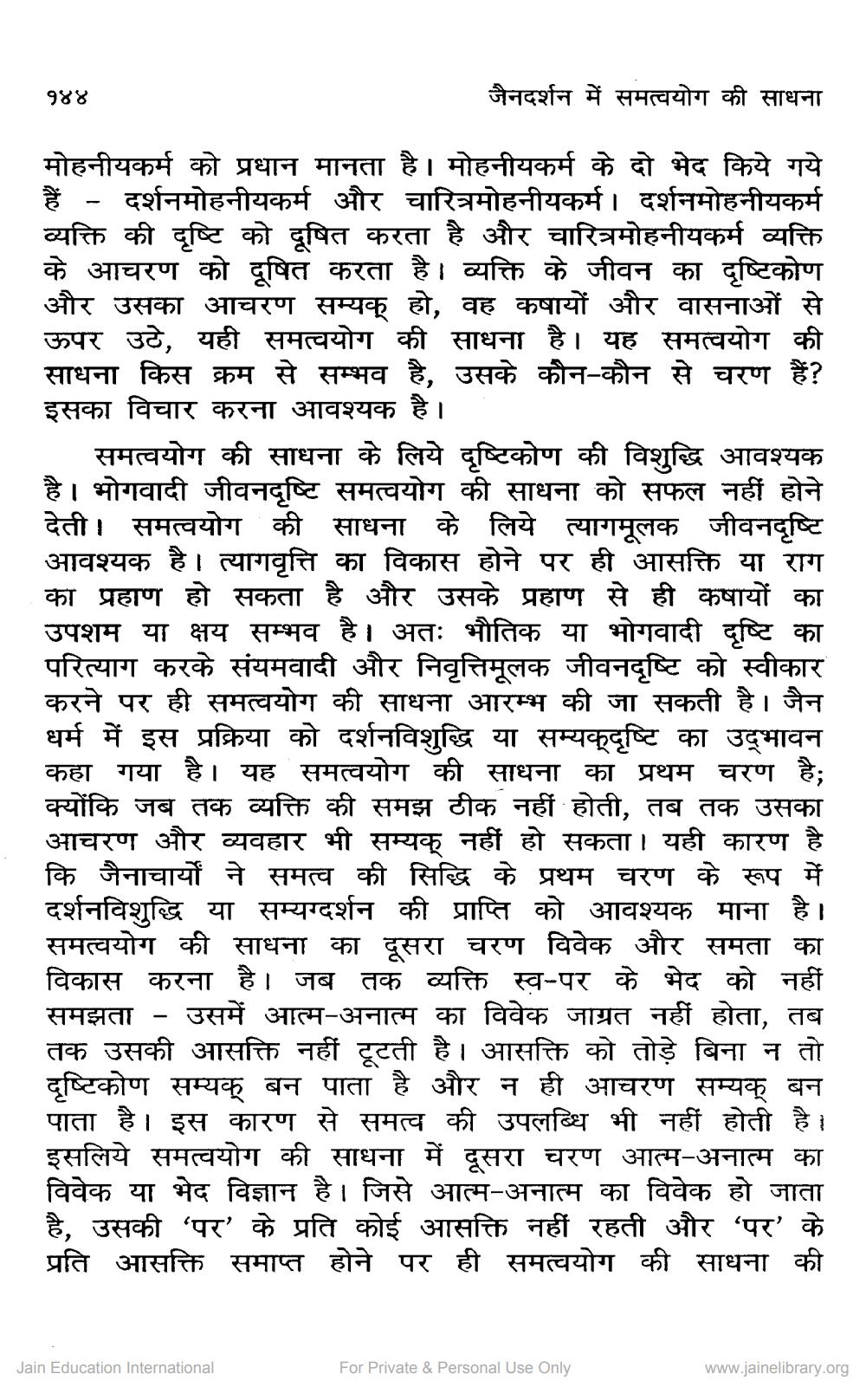________________
१४४
जैनदर्शन में समत्वयोग की साधना
मोहनीयकर्म को प्रधान मानता है। मोहनीयकर्म के दो भेद किये गये हैं - दर्शनमोहनीयकर्म और चारित्रमोहनीयकर्म। दर्शनमोहनीयकर्म व्यक्ति की दृष्टि को दूषित करता है और चारित्रमोहनीयकर्म व्यक्ति के आचरण को दूषित करता है। व्यक्ति के जीवन का दृष्टिकोण और उसका आचरण सम्यक हो, वह कषायों और वासनाओं से ऊपर उठे, यही समत्वयोग की साधना है। यह समत्वयोग की साधना किस क्रम से सम्भव है, उसके कौन-कौन से चरण हैं? इसका विचार करना आवश्यक है।
समत्वयोग की साधना के लिये दृष्टिकोण की विशुद्धि आवश्यक है। भोगवादी जीवनदृष्टि समत्वयोग की साधना को सफल नहीं होने देती। समत्वयोग की साधना के लिये त्यागमूलक जीवनदृष्टि आवश्यक है। त्यागवृत्ति का विकास होने पर ही आसक्ति या राग का प्रहाण हो सकता है और उसके प्रहाण से ही कषायों का उपशम या क्षय सम्भव है। अतः भौतिक या भोगवादी दृष्टि का परित्याग करके संयमवादी और निवृत्तिमूलक जीवनदृष्टि को स्वीकार करने पर ही समत्वयोग की साधना आरम्भ की जा सकती है। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को दर्शनविशुद्धि या सम्यकदृष्टि का उद्भावन कहा गया है। यह समत्वयोग की साधना का प्रथम चरण है; क्योंकि जब तक व्यक्ति की समझ ठीक नहीं होती, तब तक उसका आचरण और व्यवहार भी सम्यक नहीं हो सकता। यही कारण है कि जैनाचार्यों ने समत्व की सिद्धि के प्रथम चरण के रूप में दर्शनविशुद्धि या सम्यग्दर्शन की प्राप्ति को आवश्यक माना है। समत्वयोग की साधना का दूसरा चरण विवेक और समता का विकास करना है। जब तक व्यक्ति स्व-पर के भेद को नहीं समझता - उसमें आत्म-अनात्म का विवेक जाग्रत नहीं होता, तब तक उसकी आसक्ति नहीं टूटती है। आसक्ति को तोड़े बिना न तो दृष्टिकोण सम्यक् बन पाता है और न ही आचरण सम्यक् बन पाता है। इस कारण से समत्व की उपलब्धि भी नहीं होती है। इसलिये समत्वयोग की साधना में दूसरा चरण आत्म-अनात्म का विवेक या भेद विज्ञान है। जिसे आत्म-अनात्म का विवेक हो जाता है, उसकी 'पर' के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती और 'पर' के प्रति आसक्ति समाप्त होने पर ही समत्वयोग की साधना की
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org