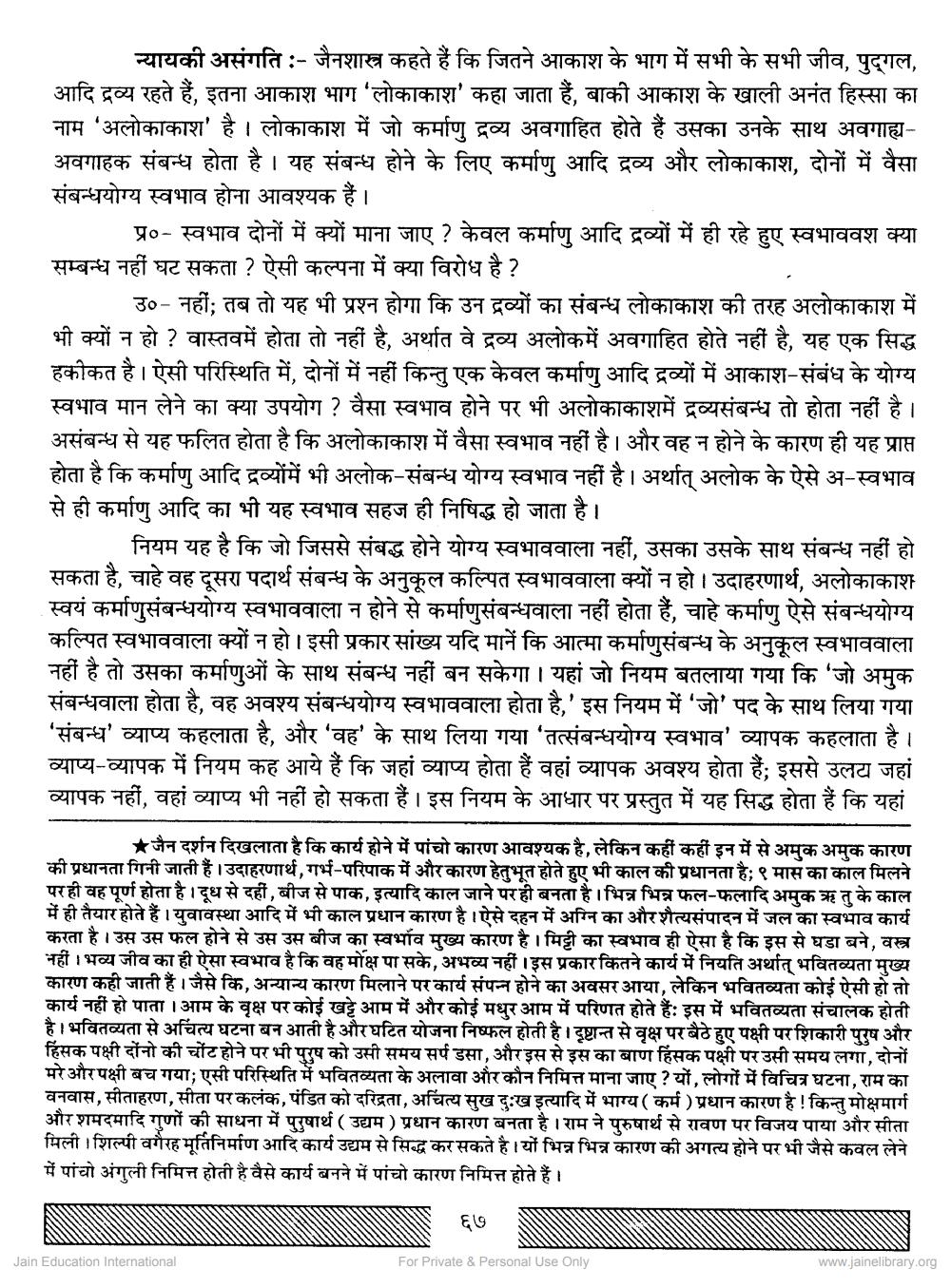________________
न्यायकी असंगति :- जैनशास्त्र कहते हैं कि जितने आकाश के भाग में सभी के सभी जीव, पुद्गल, आदि द्रव्य रहते हैं, इतना आकाश भाग 'लोकाकाश' कहा जाता हैं, बाकी आकाश के खाली अनंत हिस्सा का नाम 'अलोकाकाश' है । लोकाकाश में जो कर्माणु द्रव्य अवगाहित होते हैं उसका उनके साथ अवगाह्यअवगाहक संबन्ध होता है । यह संबन्ध होने के लिए कर्माणु आदि द्रव्य और लोकाकाश, दोनों में वैसा संबन्धयोग्य स्वभाव होना आवश्यक हैं।
प्र०- स्वभाव दोनों में क्यों माना जाए? केवल कर्माणु आदि द्रव्यों में ही रहे हुए स्वभाववश क्या सम्बन्ध नहीं घट सकता? ऐसी कल्पना में क्या विरोध है?
उ.- नहीं; तब तो यह भी प्रश्न होगा कि उन द्रव्यों का संबन्ध लोकाकाश की तरह अलोकाकाश में भी क्यों न हो? वास्तवमें होता तो नहीं है, अर्थात वे द्रव्य अलोकमें अवगाहित होते नहीं है, यह एक सिद्ध हकीकत है। ऐसी परिस्थिति में, दोनों में नहीं किन्तु एक केवल कर्माणु आदि द्रव्यों में आकाश-संबंध के योग्य स्वभाव मान लेने का क्या उपयोग ? वैसा स्वभाव होने पर भी अलोकाकाशमें द्रव्यसंबन्ध तो होता नहीं है। असंबन्ध से यह फलित होता है कि अलोकाकाश में वैसा स्वभाव नहीं है। और वह न होने के कारण ही यह प्राप्त होता है कि कर्माणु आदि द्रव्योंमें भी अलोक-संबन्ध योग्य स्वभाव नहीं है। अर्थात् अलोक के ऐसे अ-स्वभाव से ही कर्माण आदि का भी यह स्वभाव सहज ही निषिद्ध हो जाता है।
___ नियम यह है कि जो जिससे संबद्ध होने योग्य स्वभाववाला नहीं, उसका उसके साथ संबन्ध नहीं हो सकता है, चाहे वह दूसरा पदार्थ संबन्ध के अनुकूल कल्पित स्वभाववाला क्यों न हो। उदाहरणार्थ, अलोकाकाश स्वयं कर्माणुसंबन्धयोग्य स्वभाववाला न होने से कर्माणुसंबन्धवाला नहीं होता हैं, चाहे कर्माणु ऐसे संबन्धयोग्य कल्पित स्वभाववाला क्यों न हो। इसी प्रकार सांख्य यदि मानें कि आत्मा कर्माणुसंबन्ध के अनुकूल स्वभाववाला नहीं है तो उसका कर्माणुओं के साथ संबन्ध नहीं बन सकेगा। यहां जो नियम बतलाया गया कि 'जो अमुक संबन्धवाला होता है, वह अवश्य संबन्धयोग्य स्वभाववाला होता है, इस नियम में 'जो' पद के साथ लिया गया 'संबन्ध' व्याप्य कहलाता है, और 'वह' के साथ लिया गया 'तत्संबन्धयोग्य स्वभाव' व्यापक कहलाता है। व्याप्य-व्यापक में नियम कह आये हैं कि जहां व्याप्य होता हैं वहां व्यापक अवश्य होता है; इससे उलटा जहां व्यापक नहीं, वहां व्याप्य भी नहीं हो सकता हैं । इस नियम के आधार पर प्रस्तुत में यह सिद्ध होता हैं कि यहां
★जैन दर्शन दिखलाता है कि कार्य होने में पांचो कारण आवश्यक है, लेकिन कहीं कहीं इन में से अमुक अमुक कारण की प्रधानता गिनी जाती हैं। उदाहरणार्थ,गर्भ-परिपाक में और कारण हेतुभूत होते हुए भी काल की प्रधानता है; ९ मास का काल मिलने पर ही वह पूर्ण होता है। दूध से दहीं, बीज से पाक, इत्यादि काल जाने पर ही बनता है । भिन्न भिन्न फल-फलादि अमुक ऋतु के काल में ही तैयार होते हैं । युवावस्था आदि में भी काल प्रधान कारण है। ऐसे दहन में अग्नि का और शैत्यसंपादन में जल का स्वभाव कार्य करता है। उस उस फल होने से उस उस बीज का स्वभाव मुख्य कारण है। मिट्टी का स्वभाव ही ऐसा है कि इस से घडा बने, वस्त्र नहीं । भव्य जीव का ही ऐसा स्वभाव है कि वह मोक्ष पा सके, अभव्य नहीं। इस प्रकार कितने कार्य में नियति अर्थात् भवितव्यता मुख्य कारण कही जाती हैं। जैसे कि, अन्यान्य कारण मिलाने पर कार्य संपन्न होने का अवसर आया, लेकिन भवितव्यता कोई ऐसी हो तो कार्य नहीं हो पाता । आम के वृक्ष पर कोई खट्टे आम में और कोई मधुर आम में परिणत होते हैं: इस में भवितव्यता संचालक होती है। भवितव्यता से अचिंत्य घटना बन आती है औरघटित योजना निष्फल होती है। दृष्टान्त से वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी पर शिकारी पुरुष और हिंसक पक्षी दोंनो की चोंट होने पर भी पुरुष को उसी समय सर्प डसा, और इस से इस का बाण हिंसक पक्षी पर उसी समय लगा, दोनों मरे और पक्षी बच गया; एसी परिस्थिति में भवितव्यता के अलावा और कौन निमित्त माना जाए? यों,लोगों में विचित्र घटना,राम का वनवास,सीताहरण, सीता पर कलंक, पंडित को दरिद्रता, अचिंत्य सुख दुःख इत्यादि में भाग्य (कर्म) प्रधान कारण है ! किन्तु मोक्षमार्ग
और शमदमादि गुणों की साधना में पुरुषार्थ (उद्यम) प्रधान कारण बनता है। राम ने पुरुषार्थ से रावण पर विजय पाया और सीता मिली। शिल्पी वगैरह मूर्तिनिर्माण आदि कार्य उद्यम से सिद्ध कर सकते है। यों भिन्न भिन्न कारण की अगत्य होने पर भी जैसे कवल लेने में पांचो अंगुली निमित्त होती है वैसे कार्य बनने में पांचो कारण निमित्त होते हैं।
७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.