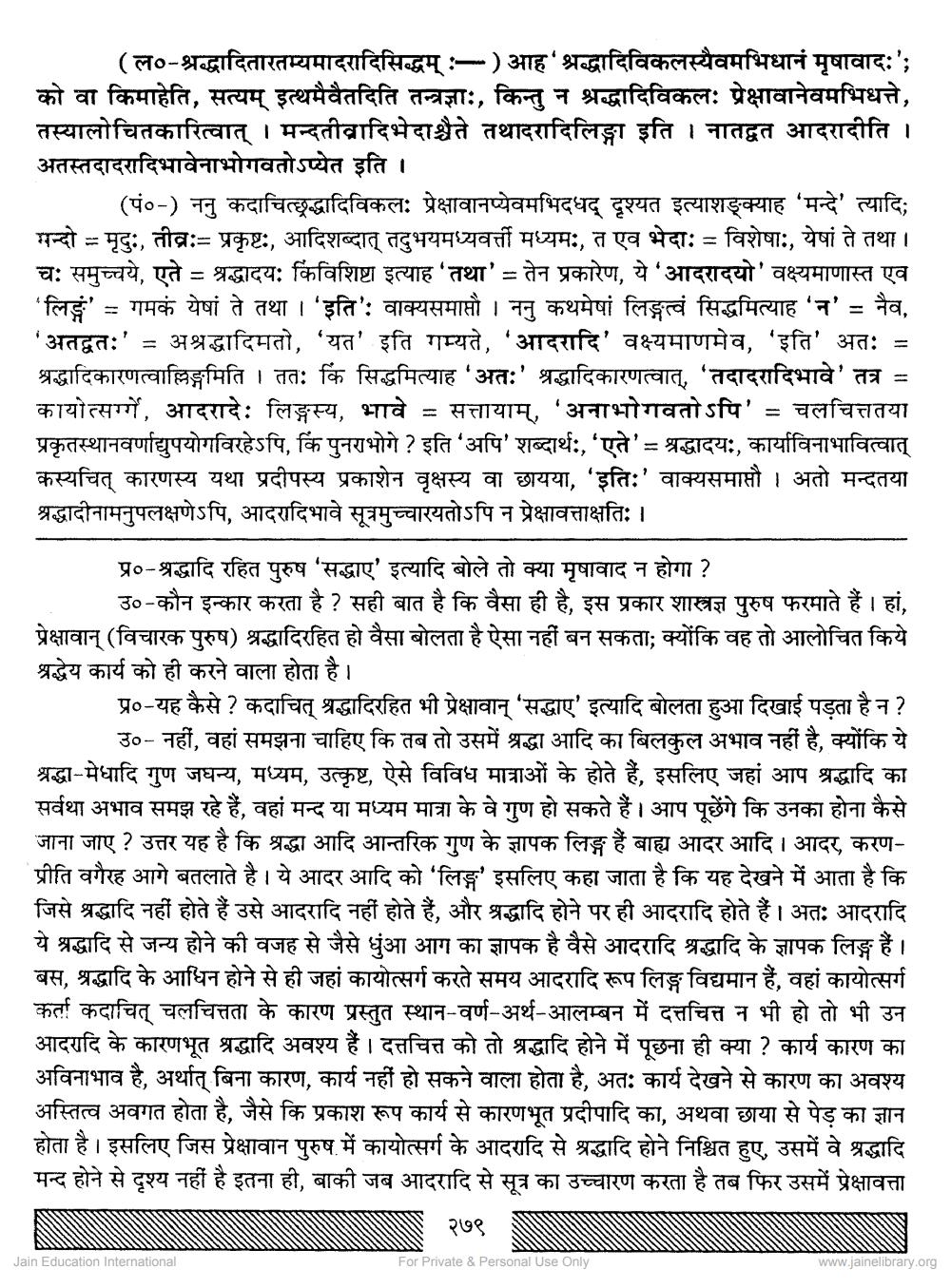________________
(ल०-श्रद्धादितारतम्यमादरादिसिद्धम् :-) आह श्रद्धादिविकलस्यैवमभिधानं मृषावादः'; को वा किमाहेति, सत्यम् इत्थमैवैतदिति तन्त्रज्ञाः, किन्तु न श्रद्धादिविकलः प्रेक्षावानेवमभिधत्ते, तस्यालोचितकारित्वात् । मन्दतीवादिभेदाश्चैते तथादरादिलिङ्गा इति । नातद्वत आदरादीति । अतस्तदादरादिभावेनाभोगवतोऽप्येत इति ।
(पं०-) ननु कदाचित्छ्रद्धादिविकल: प्रेक्षावानप्येवमभिदधद् दृश्यत इत्याशङ्क्याह 'मन्दे' त्यादि; मन्दो = मृदुः, तीव्र:= प्रकृष्टः, आदिशब्दात् तदुभयमध्यवर्ती मध्यमः, त एव भेदाः = विशेषाः, येषां ते तथा। चः समुच्चये, एते = श्रद्धादयः किविशिष्टा इत्याह 'तथा' = तेन प्रकारेण, ये 'आदरादयो' वक्ष्यमाणास्त एव 'लिङ्गं' = गमकं येषां ते तथा । 'इति': वाक्यसमाप्तौ । ननु कथमेषां लिङ्गत्वं सिद्धमित्याह 'न' = नैव, 'अतद्वतः' = अश्रद्धादिमतो, 'यत' इति गम्यते, 'आदरादि' वक्ष्यमाणमेव, 'इति' अतः = श्रद्धादिकारणत्वाल्लिङ्गमिति । ततः किं सिद्धमित्याह 'अतः' श्रद्धादिकारणत्वात्, 'तदादरादिभावे' तत्र = कायोत्सर्गे, आदरादेः लिङ्गस्य, भावे = सत्तायाम्, 'अनाभोगवतोऽपि' = चलचित्ततया प्रकृतस्थानवर्णाधुपयोगविरहेऽपि, किं पुनराभोगे? इति 'अपि' शब्दार्थः, 'एते' = श्रद्धादयः, कार्याविनाभावित्वात् कस्यचित् कारणस्य यथा प्रदीपस्य प्रकाशेन वृक्षस्य वा छायया, 'इतिः' वाक्यसमाप्तौ । अतो मन्दतया श्रद्धादीनामनुपलक्षणेऽपि, आदरादिभावे सूत्रमुच्चारयतोऽपि न प्रेक्षावत्ताक्षतिः ।
प्र०-श्रद्धादि रहित पुरुष 'सद्धाए' इत्यादि बोले तो क्या मृषावाद न होगा?
उ०-कौन इन्कार करता है ? सही बात है कि वैसा ही है, इस प्रकार शास्त्रज्ञ पुरुष फरमाते हैं । हां, प्रेक्षावान् (विचारक पुरुष) श्रद्धादिरहित हो वैसा बोलता है ऐसा नहीं बन सकता; क्योंकि वह तो आलोचित किये श्रद्धेय कार्य को ही करने वाला होता है।
प्र०-यह कैसे? कदाचित् श्रद्धादिरहित भी प्रेक्षावान् ‘सद्धाए' इत्यादि बोलता हुआ दिखाई पड़ता है न?
उ०- नहीं, वहां समझना चाहिए कि तब तो उसमें श्रद्धा आदि का बिलकुल अभाव नहीं है, क्योंकि ये श्रद्धा-मेधादि गुण जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ऐसे विविध मात्राओं के होते हैं, इसलिए जहां आप श्रद्धादि का सर्वथा अभाव समझ रहे हैं, वहां मन्द या मध्यम मात्रा के वे गुण हो सकते हैं। आप पूछेगे कि उनका होना कैसे जाना जाए ? उत्तर यह है कि श्रद्धा आदि आन्तरिक गुण के ज्ञापक लिङ्ग हैं बाह्य आदर आदि । आदर, करणप्रीति वगैरह आगे बतलाते है । ये आदर आदि को 'लिङ्ग' इसलिए कहा जाता है कि यह देखने में आता है कि जिसे श्रद्धादि नहीं होते हैं उसे आदरादि नहीं होते हैं, और श्रद्धादि होने पर ही आदरादि होते हैं। अतः आदरादि ये श्रद्धादि से जन्य होने की वजह से जैसे धुंआ आग का ज्ञापक है वैसे आदरादि श्रद्धादि के ज्ञापक लिङ्ग हैं। बस, श्रद्धादि के आधिन होने से ही जहां कायोत्सर्ग करते समय आदरादि रूप लिङ्ग विद्यमान हैं, वहां कायोत्सर्ग कर्ता कदाचित् चलचित्तता के कारण प्रस्तुत स्थान-वर्ण-अर्थ-आलम्बन में दत्तचित्त न भी हो तो भी उन आदरादि के कारणभूत श्रद्धादि अवश्य हैं । दत्तचित्त को तो श्रद्धादि होने में पूछना ही क्या ? कार्य कारण का अविनाभाव है, अर्थात् बिना कारण, कार्य नहीं हो सकने वाला होता है, अतः कार्य देखने से कारण का अवश्य अस्तित्व अवगत होता है, जैसे कि प्रकाश रूप कार्य से कारणभूत प्रदीपादि का, अथवा छाया से पेड़ का ज्ञान होता है। इसलिए जिस प्रेक्षावान पुरुष में कायोत्सर्ग के आदरादि से श्रद्धादि होने निश्चित हुए, उसमें वे श्रद्धादि मन्द होने से दृश्य नहीं है इतना ही, बाकी जब आदरादि से सूत्र का उच्चारण करता है तब फिर उसमें प्रेक्षावत्ता
२७९
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org