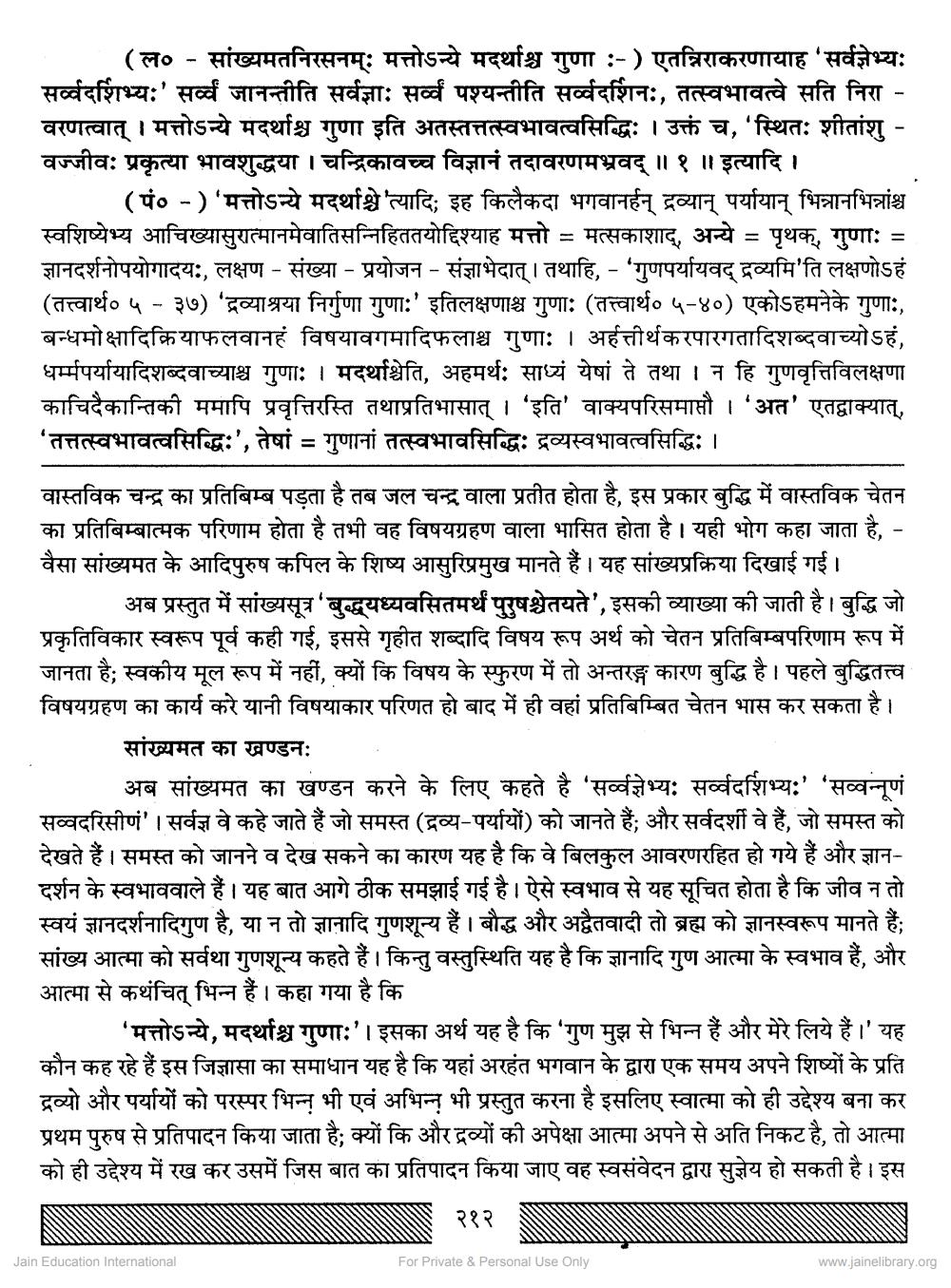________________
=
( ल० सांख्यमतनिरसनम्ः मत्तोऽन्ये मदर्थाश्च गुणा :-) एतन्निराकरणायाह 'सर्वज्ञेभ्यः सर्व्वदशिभ्यः' सर्व्वं जानन्तीति सर्वज्ञाः सर्व्वं पश्यन्तीति सर्व्वदर्शिनः, तत्स्वभावत्वे सति निरा वरणत्वात् । मत्तोऽन्ये मदर्थाश्च गुणा इति अतस्तत्तत्स्वभावत्वसिद्धिः । उक्तं च, 'स्थितः शीतांशु वज्जीवः प्रकृत्या भावशुद्धया । चन्द्रिकावच्च विज्ञानं तदावरणमभ्रवद् ॥ १ ॥ इत्यादि । ( पं० - ) 'मत्तोऽन्ये मदर्थाचे 'त्यादि; इह किलैकदा भगवानर्हन् द्रव्यान् पर्यायान् भिन्नानभिन्नांश्च स्वशिष्येभ्य आचिख्यासुरात्मानमेवातिसन्निहिततयोद्दिश्याह मत्तो = मत्सकाशाद्, अन्ये पृथक, गुणाः ज्ञानदर्शनोपयोगादय:, लक्षण संख्या प्रयोजन - संज्ञाभेदात् । तथाहि - 'गुणपर्यायवद् द्रव्यमिति लक्षणोऽहं (तत्त्वार्थ० ५ - ३७) 'द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा:' इतिलक्षणाश्च गुणा: (तत्त्वार्थ० ५ - ४०) एकोऽहमनेके गुणाः, बन्धमोक्षादिक्रियाफलवानहं विषयावगमादिफलाश्च गुणाः । अर्हत्तीर्थकरपारगतादिशब्दवाच्योऽहं, धर्म्मपर्यायादिशब्दवाच्याश्च गुणाः । मदर्थाश्चेति, अहमर्थः साध्यं येषां ते तथा । न हि गुणवृत्तिविलक्षणा काचिदैकान्तिकी ममापि प्रवृत्तिरस्ति तथाप्रतिभासात् । 'इति' वाक्यपरिसमाप्तौ । 'अत' एतद्वाक्यात्, 'तत्तत्स्वभावत्वसिद्धिः', तेषां = गुणानां तत्स्वभावसिद्धिः द्रव्यस्वभावत्वसिद्धिः ।
-
-
वास्तविक चन्द्र का प्रतिबिम्ब पड़ता है तब जल चन्द्र वाला प्रतीत होता है, इस प्रकार बुद्धि में वास्तविक चेतन का प्रतिबिम्बात्मक परिणाम होता है तभी वह विषयग्रहण वाला भासित होता है । यही भोग कहा जाता है, - वैसा सांख्यमत के आदिपुरुष कपिल के शिष्य आसुरिप्रमुख मानते हैं। यह सांख्यप्रक्रिया दिखाई गई ।
अब प्रस्तुत में सांख्यसूत्र 'बुद्ध्यध्यवसितमर्थं पुरुषश्चेतयते', इसकी व्याख्या की जाती है। बुद्धि जो प्रकृतिविकार स्वरूप पूर्व कही गई, इससे गृहीत शब्दादि विषय रूप अर्थ को चेतन प्रतिबिम्बपरिणाम रूप में जानता है; स्वकीय मूल रूप में नहीं, क्यों कि विषय के स्फुरण में तो अन्तरङ्ग कारण बुद्धि है। पहले बुद्धितत्त्व विषयग्रहण का कार्य करे यानी विषयाकार परिणत हो बाद में ही वहां प्रतिबिम्बित चेतन भास कर सकता है।
Jain Education International
=
सांख्यमत का खण्डनः
अब सांख्यमत का खण्डन करने के लिए कहते है 'सर्व्वज्ञेभ्यः सर्व्वदर्शिभ्यः' 'सव्वन्नूगं सव्वदरिसीणं' । सर्वज्ञ वे कहे जाते हैं जो समस्त (द्रव्य-पर्यायों) को जानते हैं; और सर्वदर्शी वे हैं, जो समस्त को देखते हैं। समस्त को जानने व देख सकने का कारण यह है कि वे बिलकुल आवरणरहित हो गये हैं और ज्ञानदर्शन के स्वभाववाले हैं। यह बात आगे ठीक समझाई गई है। ऐसे स्वभाव से यह सूचित होता है कि जीव न तो स्वयं ज्ञानदर्शनादिगुण है, या न तो ज्ञानादि गुणशून्य हैं। बौद्ध और अद्वैतवादी तो ब्रह्म को ज्ञानस्वरूप मानते हैं; सांख्य आत्मा को सर्वथा गुणशून्य कहते हैं । किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि ज्ञानादि गुण आत्मा के स्वभाव हैं, और आत्मा से कथंचित् भिन्न हैं । कहा गया है कि
'मत्तोऽन्ये, मदर्थाश्च गुणाः' । इसका अर्थ यह है कि 'गुण मुझ से भिन्न हैं और मेरे लिये हैं।' यह कह रहे हैं इस जिज्ञासा का समाधान यह है कि यहां अरहंत भगवान के द्वारा एक समय अपने शिष्यों के प्रति द्रव्यो और पर्यायों को परस्पर भिन्न भी एवं अभिन्न भी प्रस्तुत करना है इसलिए स्वात्मा को ही उद्देश्य बना कर प्रथम पुरुष से प्रतिपादन किया जाता है; क्यों कि और द्रव्यों की अपेक्षा आत्मा अपने से अति निकट है, तो आत्मा को ही उद्देश्य में रख कर उसमें जिस बात का प्रतिपादन किया जाए वह स्वसंवेदन द्वारा सुज्ञेय हो सकती है। इस
२१२
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org