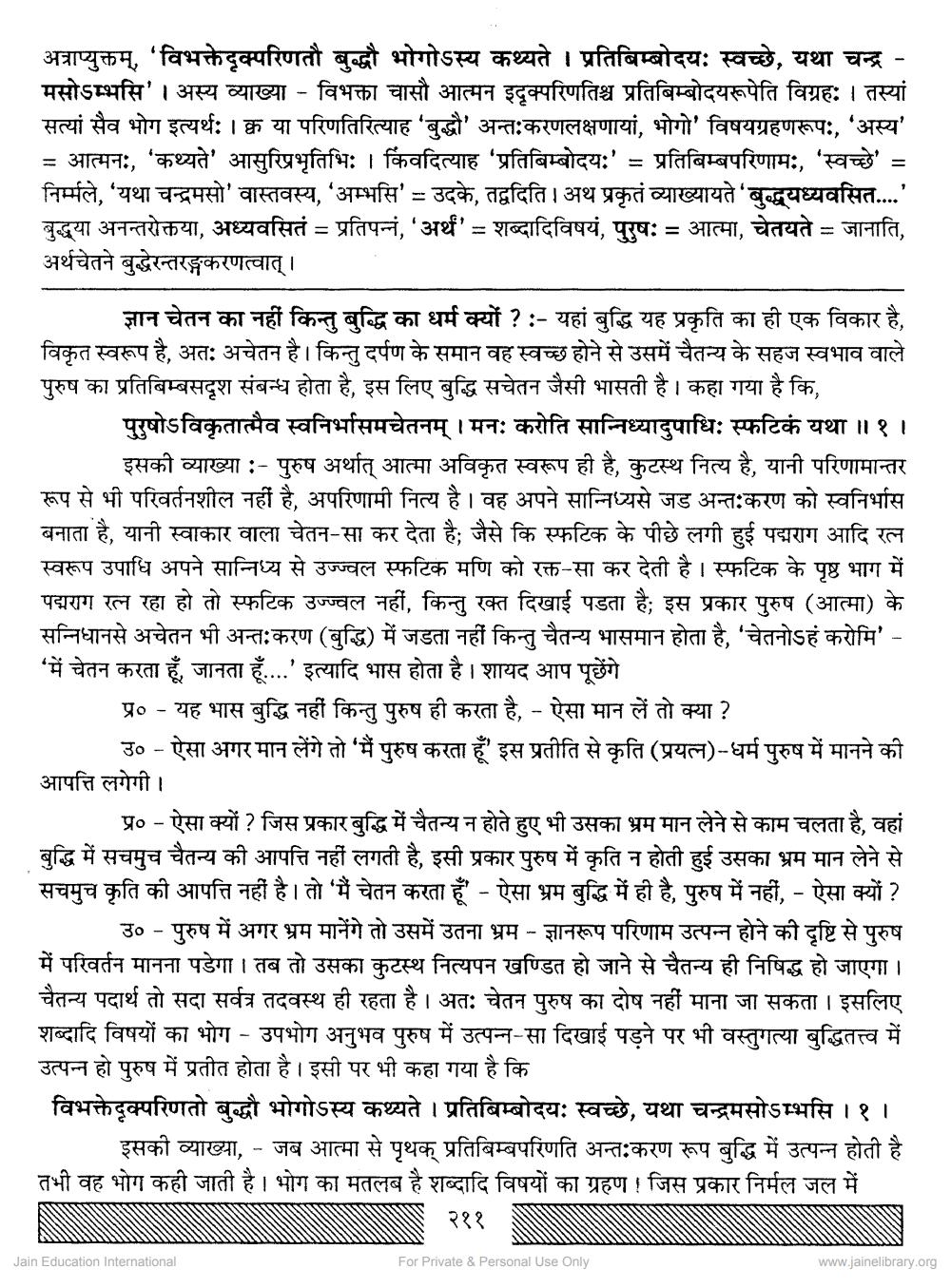________________
अत्राप्युक्तम्, 'विभक्तेदृक्परिणतौ बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते । प्रतिबिम्बोदयः स्वच्छे, यथा चन्द्र - मसोऽम्भसि' । अस्य व्याख्या - विभक्ता चासौ आत्मन इदृक्परिणतिश्च प्रतिबिम्बोदयरूपेति विग्रहः । तस्यां सत्यां सैव भोग इत्यर्थः । क्व या परिणतिरित्याह 'बुद्धौ' अन्तःकरणलक्षणायां, भोगो' विषयग्रहणरूपः, 'अस्य' = आत्मनः, 'कथ्यते' आसुरिप्रभृतिभिः । किंवदित्याह 'प्रतिबिम्बोदयः' = प्रतिबिम्बपरिणामः, 'स्वच्छे' = निर्मले, 'यथा चन्द्रमसो' वास्तवस्य, 'अम्भसि' = उदके, तद्वदिति । अथ प्रकृतं व्याख्यायते 'बुद्ध्यध्यवसित....' बुद्धया अनन्तरोक्तया, अध्यवसितं = प्रतिपन्नं, 'अर्थ' = शब्दादिविषयं, पुरुषः = आत्मा, चेतयते = जानाति, अर्थचेतने बुद्धेरन्तरङ्गकरणत्वात् ।
ज्ञान चेतन का नहीं किन्तु बुद्धि का धर्म क्यों ? :- यहां बुद्धि यह प्रकृति का ही एक विकार है, विकृत स्वरूप है, अत: अचेतन है। किन्तु दर्पण के समान वह स्वच्छ होने से उसमें चैतन्य के सहज स्वभाव वाले पुरुष का प्रतिबिम्बसदृश संबन्ध होता है, इस लिए बुद्धि सचेतन जैसी भासती है। कहा गया है कि,
पुरुषोऽविकृतात्मैव स्वनिर्भासमचेतनम् । मनः करोति सान्निध्यादुपाधिः स्फटिकं यथा ॥१॥
इसकी व्याख्या :- पुरुष अर्थात् आत्मा अविकृत स्वरूप ही है, कुटस्थ नित्य है, यानी परिणामान्तर रूप से भी परिवर्तनशील नहीं है, अपरिणामी नित्य है। वह अपने सान्निध्यसे जड अन्तःकरण को स्वनिर्भास बनाता है, यानी स्वाकार वाला चेतन-सा कर देता है; जैसे कि स्फटिक के पीछे लगी हुई पद्मराग आदि रत्न स्वरूप उपाधि अपने सान्निध्य से उज्ज्वल स्फटिक मणि को रक्त-सा कर देती है। स्फटिक के पृष्ठ भाग में पद्मराग रत्न रहा हो तो स्फटिक उज्ज्वल नहीं, किन्तु रक्त दिखाई पडता है; इस प्रकार पुरुष (आत्मा) के सन्निधानसे अचेतन भी अन्तःकरण (बुद्धि) में जडता नहीं किन्तु चैतन्य भासमान होता है, 'चेतनोऽहं करोमि' - ‘में चेतन करता हूँ, जानता हूँ....' इत्यादि भास होता है। शायद आप पूछेगे
प्र० - यह भास बुद्धि नहीं किन्तु पुरुष ही करता है, - ऐसा मान लें तो क्या ?
उ० - ऐसा अगर मान लेंगे तो 'मैं पुरुष करता हूँ' इस प्रतीति से कृति (प्रयत्न)-धर्म पुरुष में मानने की आपत्ति लगेगी।
प्र० - ऐसा क्यों ? जिस प्रकार बुद्धि में चैतन्य न होते हुए भी उसका भ्रम मान लेने से काम चलता है, वहां बुद्धि में सचमुच चैतन्य की आपत्ति नहीं लगती है, इसी प्रकार पुरुष में कृति न होती हुई उसका भ्रम मान लेने से सचमुच कृति की आपत्ति नहीं है। तो 'मैं चेतन करता हूँ' - ऐसा भ्रम बुद्धि में ही है, पुरुष में नहीं, - ऐसा क्यों?
उ० - पुरुष में अगर भ्रम मानेंगे तो उसमें उतना भ्रम - ज्ञानरूप परिणाम उत्पन्न होने की दृष्टि से पुरुष में परिवर्तन मानना पडेगा। तब तो उसका कुटस्थ नित्यपन खण्डित हो जाने से चैतन्य ही निषिद्ध हो जाएगा। चैतन्य पदार्थ तो सदा सर्वत्र तदवस्थ ही रहता है। अत: चेतन पुरुष का दोष नहीं माना जा सकता । इसलिए शब्दादि विषयों का भोग - उपभोग अनुभव पुरुष में उत्पन्न-सा दिखाई पड़ने पर भी वस्तुगत्या बुद्धितत्त्व में उत्पन्न हो पुरुष में प्रतीत होता है। इसी पर भी कहा गया है कि विभक्तेदृक्परिणतो बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते । प्रतिबिम्बोदयः स्वच्छे, यथा चन्द्रमसोऽम्भसि । १ ।
इसकी व्याख्या, - जब आत्मा से पृथक् प्रतिबिम्बपरिणति अन्तःकरण रूप बुद्धि में उत्पन्न होती है तभी वह भोग कही जाती है। भोग का मतलब है शब्दादि विषयों का ग्रहण ! जिस प्रकार निर्मल जल में
२११
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org