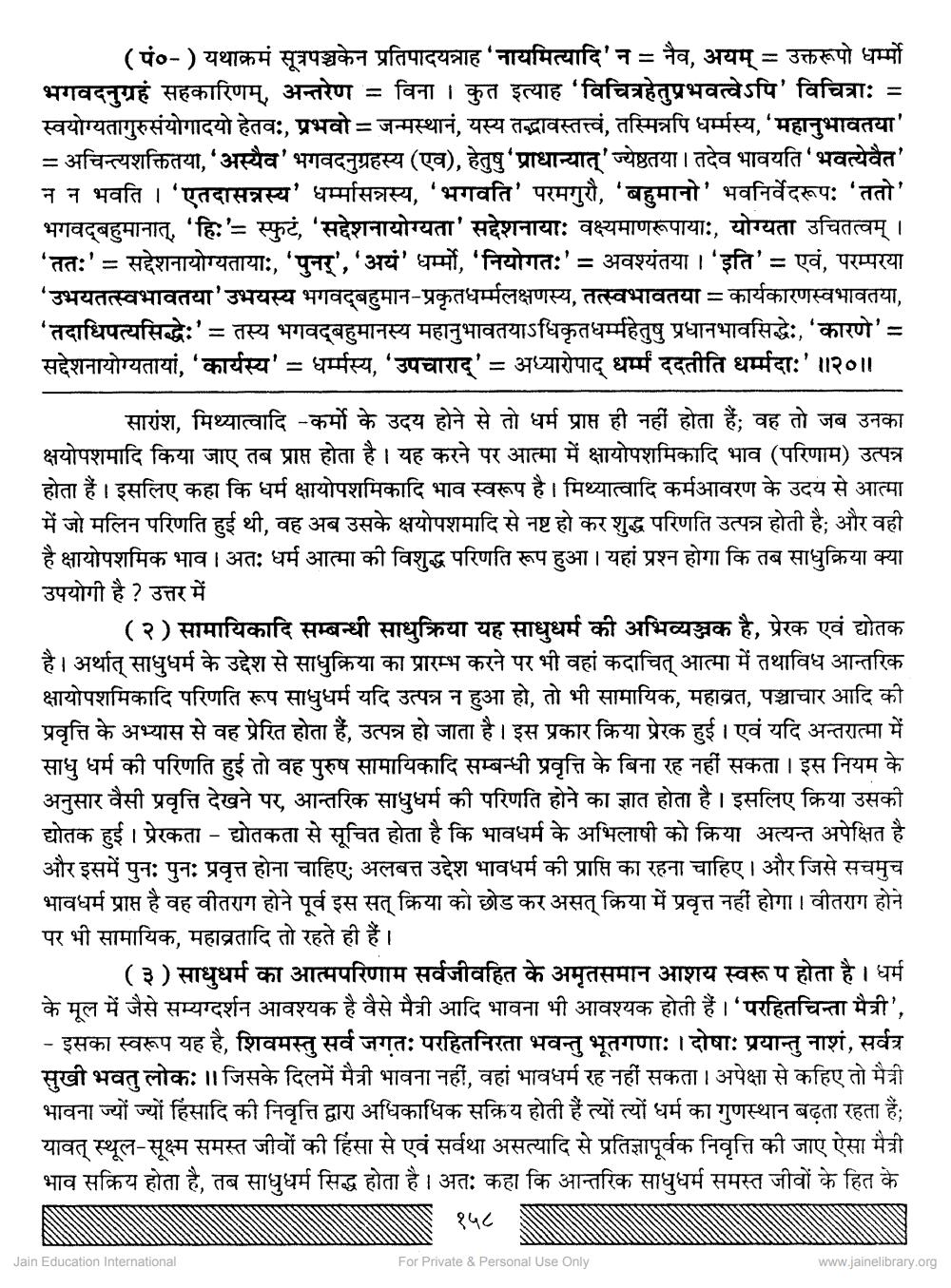________________
(पं०-) यथाक्रमं सूत्रपञ्चकेन प्रतिपादयन्नाह ‘नायमित्यादि' न = नैव, अयम् = उक्तरूपो धर्मो भगवदनुग्रहं सहकारिणम्, अन्तरेण = विना । कुत इत्याह 'विचित्रहेतुप्रभवत्वेऽपि' विचित्राः = स्वयोग्यतागुरुसंयोगादयो हेतवः, प्रभवो = जन्मस्थानं, यस्य तद्भावस्तत्त्वं, तस्मिन्नपि धर्मस्य, 'महानुभावतया' = अचिन्त्यशक्तितया, अस्यैव' भगवदनुग्रहस्य (एव), हेतुषु 'प्राधान्यात्' ज्येष्ठतया । तदेव भावयति भवत्येवैत' न न भवति । 'एतदासन्नस्य' धर्मासनस्य, 'भगवति' परमगुरौ, 'बहुमानो' भवनिर्वेदरूपः 'ततो' भगवद्बहुमानात्, 'हि.'= स्फुटं, 'सद्देशनायोग्यता' सद्देशनायाः वक्ष्यमाणरूपायाः, योग्यता उचितत्वम् । 'ततः' = सद्देशनायोग्यतायाः, 'पुनर्', 'अयं' धर्मो, 'नियोगतः' = अवश्यंतया । 'इति' = एवं, परम्परया 'उभयतत्स्वभावतया' उभयस्य भगवद्बहुमान-प्रकृतधर्मलक्षणस्य, तत्स्वभावतया = कार्यकारणस्वभावतया, 'तदाधिपत्यसिद्धेः' = तस्य भगवद्बहुमानस्य महानुभावतयाऽधिकृतधर्महेतुषु प्रधानभावसिद्धेः, 'कारणे' = सद्देशनायोग्यतायां, 'कार्यस्य' = धर्मास्य, 'उपचाराद्' = अध्यारोपाद् धर्मं ददतीति धर्मदाः' ॥२०॥
सारांश, मिथ्यात्वादि -कर्मो के उदय होने से तो धर्म प्राप्त ही नहीं होता हैं; वह तो जब उनका क्षयोपशमादि किया जाए तब प्राप्त होता है। यह करने पर आत्मा में क्षायोपशमिकादि भाव (परिणाम) उत्पन्न होता हैं। इसलिए कहा कि धर्म क्षायोपशमिकादि भाव स्वरूप है। मिथ्यात्वादि कर्मआवरण के उदय से आत्मा में जो मलिन परिणति हुई थी, वह अब उसके क्षयोपशमादि से नष्ट हो कर शुद्ध परिणति उत्पन्न होती है; और वही है क्षायोपशमिक भाव । अत: धर्म आत्मा की विशुद्ध परिणति रूप हुआ। यहां प्रश्न होगा कि तब साधुक्रिया क्या उपयोगी है ? उत्तर में
(२) सामायिकादि सम्बन्धी साधुक्रिया यह साधुधर्म की अभिव्यञ्जक है, प्रेरक एवं द्योतक है। अर्थात् साधुधर्म के उद्देश से साधुक्रिया का प्रारम्भ करने पर भी वहां कदाचित् आत्मा में तथाविध आन्तरिक क्षायोपशमिकादि परिणति रूप साधुधर्म यदि उत्पन्न न हुआ हो, तो भी सामायिक, महाव्रत, पञ्चाचार आदि की प्रवृत्ति के अभ्यास से वह प्रेरित होता हैं, उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार क्रिया प्रेरक हुई । एवं यदि अन्तरात्मा में साधु धर्म की परिणति हुई तो वह पुरुष सामायिकादि सम्बन्धी प्रवृत्ति के बिना रह नहीं सकता। इस नियम के अनुसार वैसी प्रवृत्ति देखने पर, आन्तरिक साधुधर्म की परिणति होने का ज्ञात होता है। इसलिए क्रिया उसकी द्योतक हुई । प्रेरकता - द्योतकता से सूचित होता है कि भावधर्म के अभिलाषी को क्रिया अत्यन्त अपेक्षित है
और इसमें पुनः पुनः प्रवृत्त होना चाहिए; अलबत्त उद्देश भावधर्म की प्राप्ति का रहना चाहिए। और जिसे सचमुच भावधर्म प्राप्त है वह वीतराग होने पूर्व इस सत् क्रिया को छोड कर असत् क्रिया में प्रवृत्त नहीं होगा। वीतराग होने पर भी सामायिक, महाव्रतादि तो रहते ही हैं।
(३) साधुधर्म का आत्मपरिणाम सर्वजीवहित के अमृतसमान आशय स्वरूप होता है। धर्म के मूल में जैसे सम्यग्दर्शन आवश्यक है वैसे मैत्री आदि भावना भी आवश्यक होती हैं। 'परहितचिन्ता मैत्री', - इसका स्वरूप यह है, शिवमस्तु सर्व जगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः । दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥ जिसके दिलमें मैत्री भावना नहीं, वहां भावधर्म रह नहीं सकता। अपेक्षा से कहिए तो मैत्री भावना ज्यों ज्यों हिंसादि की निवृत्ति द्वारा अधिकाधिक सक्रिय होती हैं त्यों त्यों धर्म का गुणस्थान बढ़ता रहता हैं; यावत् स्थूल-सूक्ष्म समस्त जीवों की हिंसा से एवं सर्वथा असत्यादि से प्रतिज्ञापूर्वक निवृत्ति की जाए ऐसा मैत्री भाव सक्रिय होता है, तब साधुधर्म सिद्ध होता है। अतः कहा कि आन्तरिक साधुधर्म समस्त जीवों के हित के
१५८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org