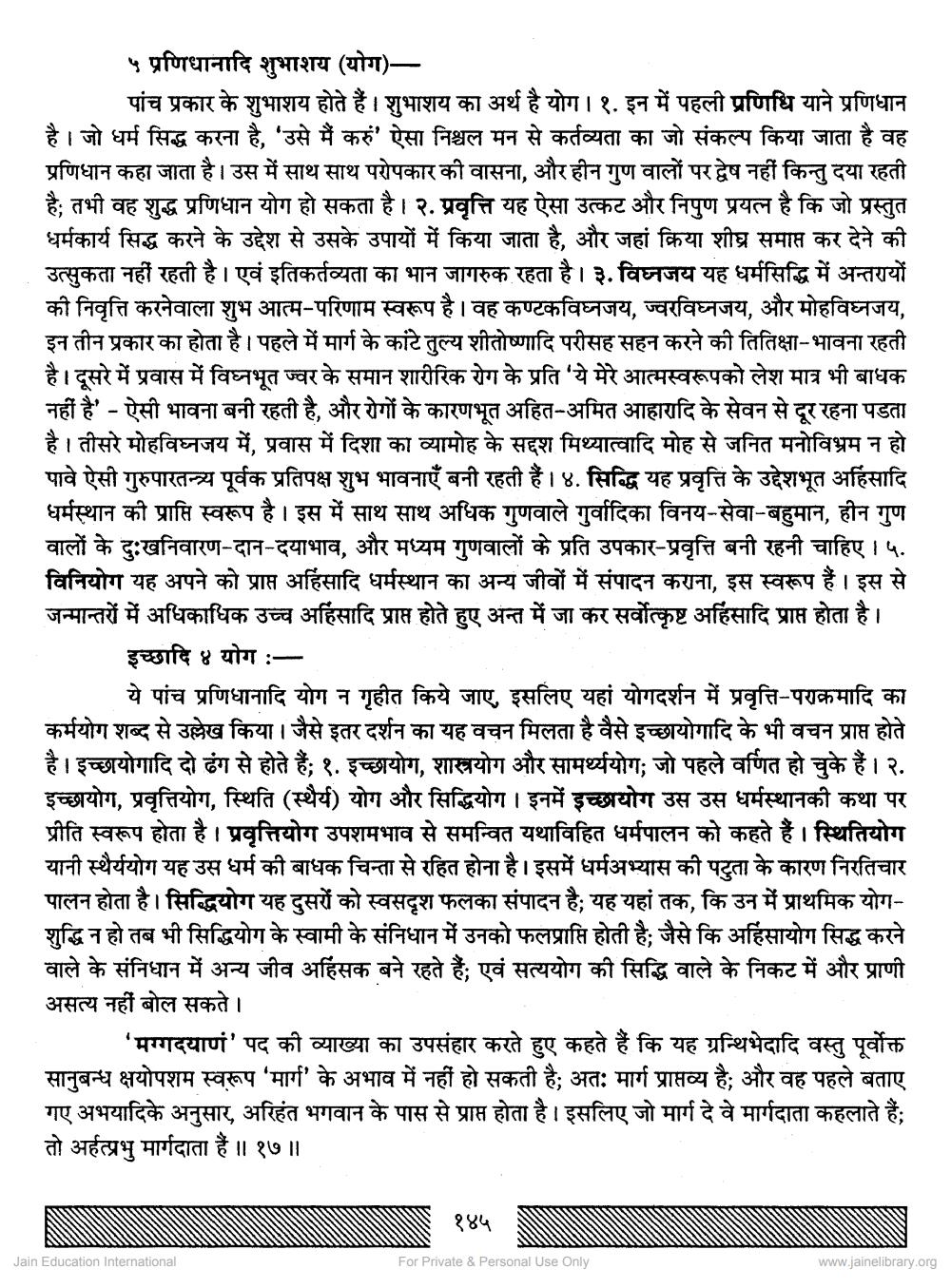________________
५ प्रणिधानादि शुभाशय (योग) -
पांच प्रकार के शुभाशय होते हैं। शुभाशय का अर्थ है योग । १. इन में पहली प्रणिधि याने प्रणिधान
I
है । जो धर्म सिद्ध करना है, 'उसे मैं करूं' ऐसा निश्चल मन से कर्तव्यता का जो संकल्प किया जाता है वह प्रणिधान कहा जाता है। उस में साथ साथ परोपकार की वासना, और हीन गुण वालों पर द्वेष नहीं किन्तु दया रहती है; तभी वह शुद्ध प्रणिधान योग हो सकता है । २. प्रवृत्ति यह ऐसा उत्कट और निपुण प्रयत्न है कि जो प्रस्तुत धर्मकार्य सिद्ध करने के उद्देश से उसके उपायों में किया जाता है, और जहां क्रिया शीघ्र समाप्त कर देने की उत्सुकता नहीं रहती है । एवं इतिकर्तव्यता का भान जागरुक रहता है । ३. विघ्नजय यह धर्मसिद्धि में अन्तरायों की निवृत्ति करनेवाला शुभ आत्म-परिणाम स्वरूप है। वह कण्टकविघ्नजय, ज्वरविघ्नजय, और मोहविघ्नजय,
तीन प्रकार का होता है। पहले में मार्ग के कांटे तुल्य शीतोष्णादि परीसह सहन करने की तितिक्षा -भावना रहती है। दूसरे में प्रवास में विघ्नभूत ज्वर के समान शारीरिक रोग के प्रति 'ये मेरे आत्मस्वरूपको लेश मात्र भी बाधक नहीं है' - ऐसी भावना बनी रहती है, और रोगों के कारणभूत अहित-अमित आहारादि के सेवन से दूर रहना पडता है । तीसरे मोहविघ्नजय में, प्रवास में दिशा का व्यामोह के सद्दश मिथ्यात्वादि मोह से जनित मनोविभ्रम न हो पावे ऐसी गुरुपारतन्त्र्य पूर्वक प्रतिपक्ष शुभ भावनाएँ बनी रहती हैं । ४. सिद्धि यह प्रवृत्ति के उद्देशभूत अहिंसादि धर्मस्थान की प्राप्ति स्वरूप है। इस में साथ साथ अधिक गुणवाले गुर्वादिका विनय-सेवा- बहुमान, हीन गुण वालों के दुःखनिवारण-दान- दयाभाव, और मध्यम गुणवालों के प्रति उपकार - प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए । ५. विनियोग यह अपने को प्राप्त अहिंसादि धर्मस्थान का अन्य जीवों में संपादन कराना, इस स्वरूप हैं। इससे जन्मान्तरों में अधिकाधिक उच्च अहिंसादि प्राप्त होते हुए अन्त में जा कर सर्वोत्कृष्ट अहिंसादि प्राप्त होता है ।
इच्छादि ४ योग --
1
ये पांच प्रणिधानादि योग न गृहीत किये जाए, इसलिए यहां योगदर्शन में प्रवृत्ति - पराक्रमादि का कर्मयोग शब्द से उल्लेख किया। जैसे इतर दर्शन का यह वचन मिलता है वैसे इच्छायोगादि के भी वचन प्राप्त होते है । इच्छायोगादि दो ढंग से होते हैं; १. इच्छायोग, शास्त्रयोग और सामर्थ्ययोग; जो पहले वर्णित हो चुके हैं । २. इच्छायोग, प्रवृत्तियोग, स्थिति ( स्थैर्य) योग और सिद्धियोग । इनमें इच्छायोग उस उस धर्मस्थानकी कथा पर प्रीति स्वरूप होता है । प्रवृत्तियोग उपशमभाव से समन्वित यथाविहित धर्मपालन को कहते हैं। स्थितियोग यानी स्थैर्ययोग यह उस धर्म की बाधक चिन्ता से रहित होना है। इसमें धर्मअभ्यास की पटुता के कारण निरतिचार पालन होता है। सिद्धियोग यह दुसरों को स्वसदृश फलका संपादन है; यह यहां तक कि उन में प्राथमिक योगशुद्धि न हो तब भी सिद्धियोग के स्वामी के संनिधान में उनको फलप्राप्ति होती है; जैसे कि अहिंसायोग सिद्ध करने वाले के संनिधान में अन्य जीव अहिंसक बने रहते हैं; एवं सत्ययोग की सिद्धि वाले के निकट में और प्राणी असत्य नहीं बोल सकते ।
'मग्गदयाणं' पद की व्याख्या का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि यह ग्रन्थिभेदादि वस्तु पूर्वोक्त सानुबन्ध क्षयोपशम स्वरूप 'मार्ग' के अभाव में नहीं हो सकती है; अतः मार्ग प्राप्तव्य है; और वह पहले बताए गए अभयादिके अनुसार, अरिहंत भगवान के पास से प्राप्त होता है। इसलिए जो मार्ग दे वे मार्गदाता कहलाते हैं; तो अर्हत्प्रभु मार्गदाता है ॥ १७ ॥
Jain Education International
१४५
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org