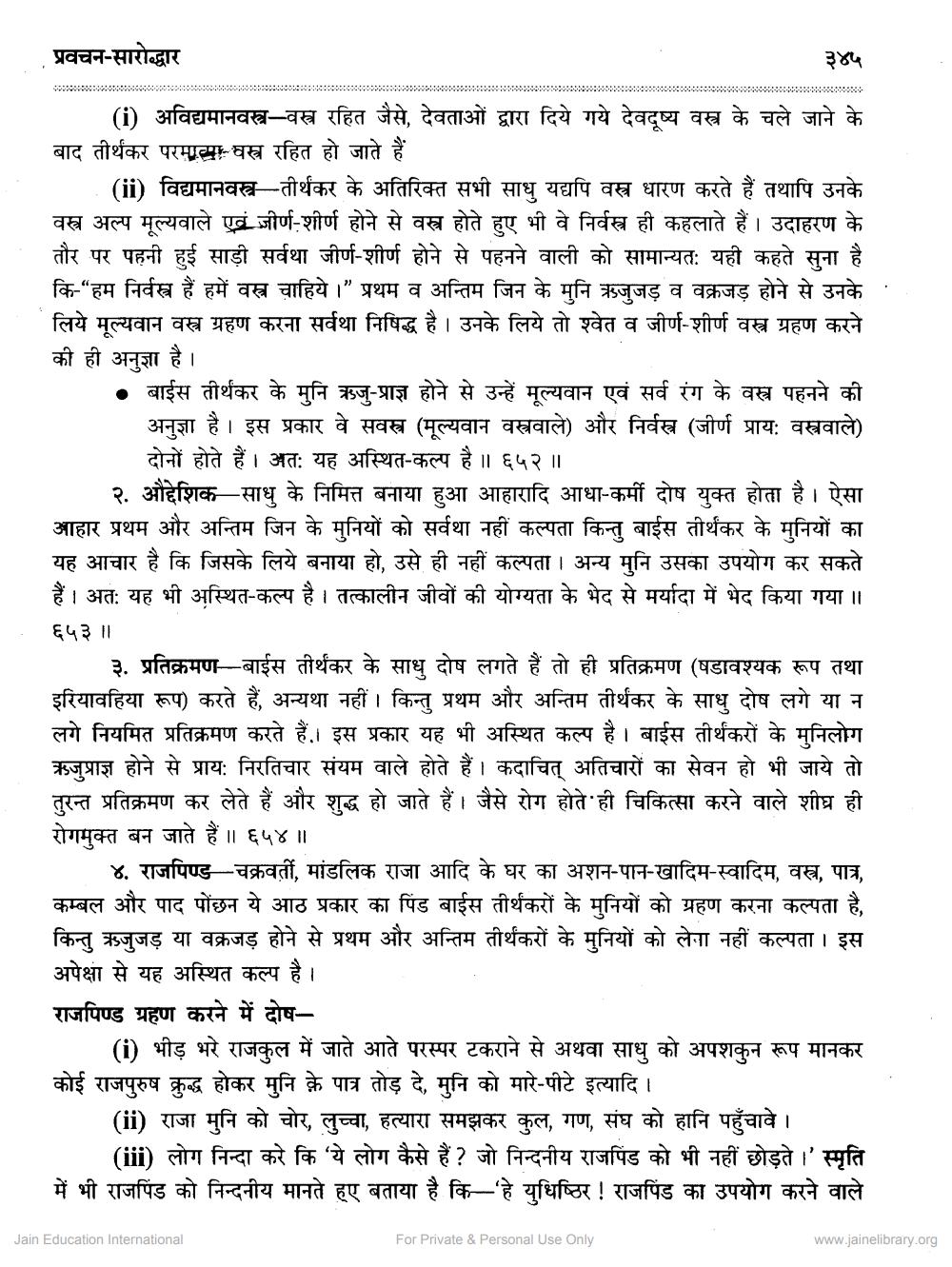________________
प्रवचन-सारोद्धार
३४५
(i) अविद्यमानवस्त्र-वस्त्र रहित जैसे, देवताओं द्वारा दिये गये देवदूष्य वस्त्र के चले जाने के बाद तीर्थंकर परमात्मा वस्त्र रहित हो जाते हैं
(ii) विद्यमानवस्त्र तीर्थंकर के अतिरिक्त सभी साधु यद्यपि वस्त्र धारण करते हैं तथापि उनके वस्त्र अल्प मूल्यवाले एवं जीर्ण-शीर्ण होने से वस्त्र होते हुए भी वे निर्वस्त्र ही कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर पहनी हुई साड़ी सर्वथा जीर्ण-शीर्ण होने से पहनने वाली को सामान्यत: यही कहते सुना है कि-"हम निर्वस्त्र हैं हमें वस्त्र चाहिये।" प्रथम व अन्तिम जिन के मुनि ऋजुजड़ व वक्रजड़ होने से उनके . लिये मूल्यवान वस्त्र ग्रहण करना सर्वथा निषिद्ध है। उनके लिये तो श्वेत व जीर्ण-शीर्ण वस्त्र ग्रहण करने की ही अनुज्ञा है।
• बाईस तीर्थंकर के मुनि ऋजु-प्राज्ञ होने से उन्हें मूल्यवान एवं सर्व रंग के वस्त्र पहनने की
अनुज्ञा है। इस प्रकार वे सवस्त्र (मूल्यवान वस्त्रवाले) और निर्वस्त्र (जीर्ण प्राय: वस्त्रवाले)
दोनों होते हैं। अत: यह अस्थित-कल्प है ॥ ६५२ ।।
२. औद्देशिक साधु के निमित्त बनाया हुआ आहारादि आधा-कर्मी दोष युक्त होता है। ऐसा आहार प्रथम और अन्तिम जिन के मुनियों को सर्वथा नहीं कल्पता किन्तु बाईस तीर्थंकर के मुनियों का यह आचार है कि जिसके लिये बनाया हो, उसे ही नहीं कल्पता। अन्य मुनि उसका उपयोग कर सकते हैं। अत: यह भी अस्थित-कल्प है। तत्कालीन जीवों की योग्यता के भेद से मर्यादा में भेद किया गया । ६५३ ॥
३. प्रतिक्रमण-बाईस तीर्थंकर के साधु दोष लगते हैं तो ही प्रतिक्रमण (षडावश्यक रूप तथा इरियावहिया रूप) करते हैं, अन्यथा नहीं। किन्तु प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के साधु दोष लगे या न लगे नियमित प्रतिक्रमण करते हैं.। इस प्रकार यह भी अस्थित कल्प है। बाईस तीर्थंकरों के मुनिलोग ऋजुप्राज्ञ होने से प्राय: निरतिचार संयम वाले होते हैं। कदाचित् अतिचारों का सेवन हो भी जाये तो तुरन्त प्रतिक्रमण कर लेते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। जैसे रोग होते ही चिकित्सा करने वाले शीघ्र ही रोगमुक्त बन जाते हैं ।। ६५४॥
४. राजपिण्ड-चक्रवर्ती, मांडलिक राजा आदि के घर का अशन-पान-खादिम-स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल और पाद पोंछन ये आठ प्रकार का पिंड बाईस तीर्थंकरों के मुनियों को ग्रहण करना कल्पता है, किन्तु ऋजुजड़ या वक्रजड़ होने से प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों के मुनियों को लेना नहीं कल्पता। इस अपेक्षा से यह अस्थित कल्प है। राजपिण्ड ग्रहण करने में दोष
(i) भीड़ भरे राजकुल में जाते आते परस्पर टकराने से अथवा साधु को अपशकुन रूप मानकर कोई राजपुरुष क्रुद्ध होकर मुनि के पात्र तोड़ दे, मुनि को मारे-पीटे इत्यादि ।
(ii) राजा मुनि को चोर, लुच्चा, हत्यारा समझकर कुल, गण, संघ को हानि पहुँचावे।
(iii) लोग निन्दा करे कि 'ये लोग कैसे हैं? जो निन्दनीय राजपिंड को भी नहीं छोड़ते।' स्मृति में भी राजपिंड को निन्दनीय मानते हुए बताया है कि-'हे युधिष्ठिर ! राजपिंड का उपयोग करने वाले
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org