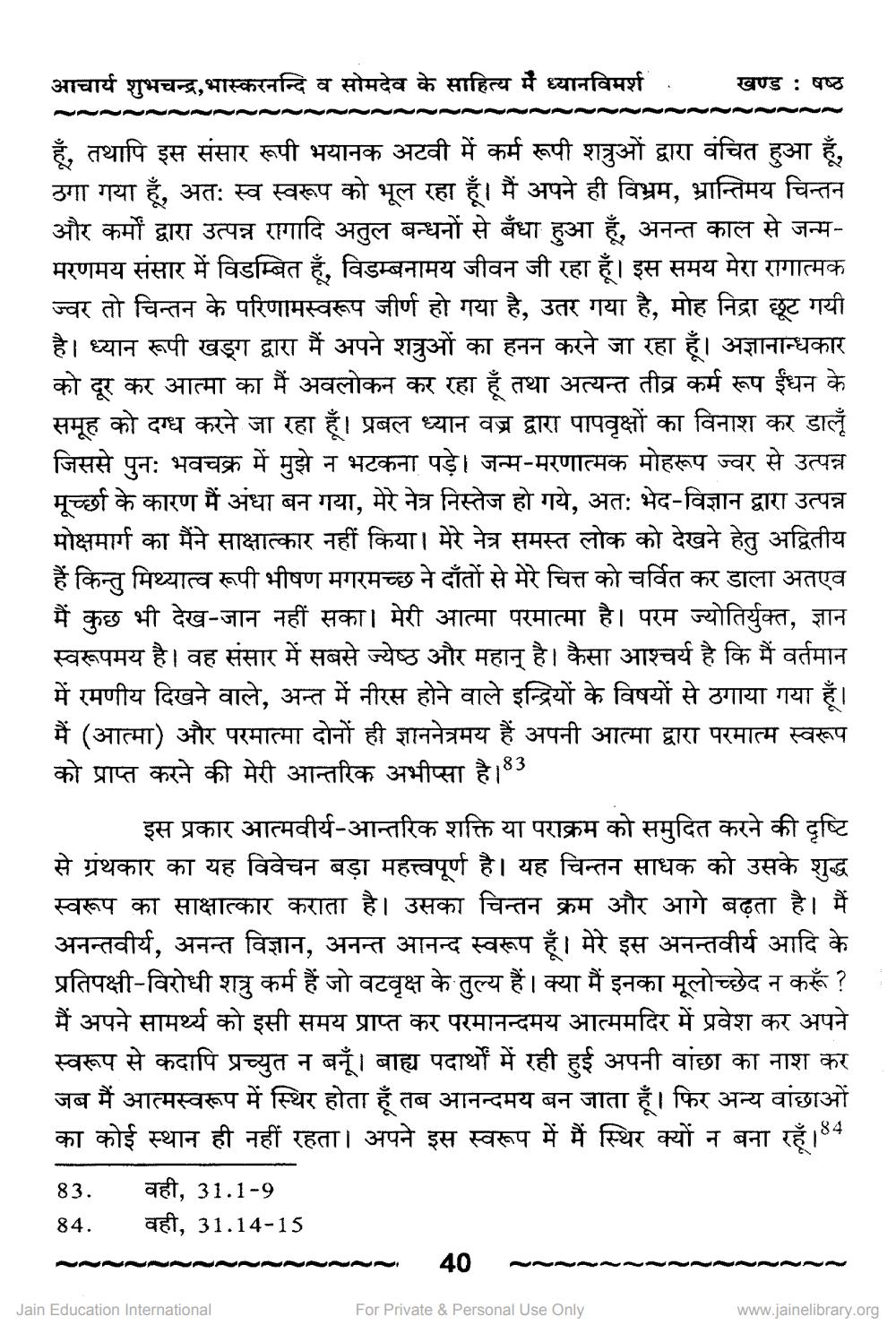________________
आचार्य शुभचन्द्र,भास्करनन्दि व सोमदेव के साहित्य में ध्यानविमर्श .
खण्ड : षष्ठ
हूँ, तथापि इस संसार रूपी भयानक अटवी में कर्म रूपी शत्रुओं द्वारा वंचित हुआ है, ठगा गया हूँ, अत: स्व स्वरूप को भूल रहा हूँ। मैं अपने ही विभ्रम, भ्रान्तिमय चिन्तन
और कर्मों द्वारा उत्पन्न रागादि अतुल बन्धनों से बँधा हुआ हूँ, अनन्त काल से जन्ममरणमय संसार में विडम्बित हूँ, विडम्बनामय जीवन जी रहा हूँ। इस समय मेरा रागात्मक ज्वर तो चिन्तन के परिणामस्वरूप जीर्ण हो गया है, उतर गया है, मोह निद्रा छूट गयी है। ध्यान रूपी खड्ग द्वारा मैं अपने शत्रुओं का हनन करने जा रहा हूँ। अज्ञानान्धकार को दूर कर आत्मा का मैं अवलोकन कर रहा हूँ तथा अत्यन्त तीव्र कर्म रूप ईंधन के समूह को दग्ध करने जा रहा हूँ। प्रबल ध्यान वज्र द्वारा पापवृक्षों का विनाश कर डालूँ जिससे पुन: भवचक्र में मुझे न भटकना पड़े। जन्म-मरणात्मक मोहरूप ज्वर से उत्पन्न मूर्छा के कारण मैं अंधा बन गया, मेरे नेत्र निस्तेज हो गये, अत: भेद-विज्ञान द्वारा उत्पन्न मोक्षमार्ग का मैंने साक्षात्कार नहीं किया। मेरे नेत्र समस्त लोक को देखने हेतु अद्वितीय हैं किन्तु मिथ्यात्व रूपी भीषण मगरमच्छ ने दाँतों से मेरे चित्त को चर्वित कर डाला अतएव मैं कुछ भी देख-जान नहीं सका। मेरी आत्मा परमात्मा है। परम ज्योतिर्युक्त, ज्ञान स्वरूपमय है। वह संसार में सबसे ज्येष्ठ और महान है। कैसा आश्चर्य है कि मैं वर्तमान में रमणीय दिखने वाले, अन्त में नीरस होने वाले इन्द्रियों के विषयों से ठगाया गया है। मैं (आत्मा) और परमात्मा दोनों ही ज्ञाननेत्रमय हैं अपनी आत्मा द्वारा परमात्म स्वरूप को प्राप्त करने की मेरी आन्तरिक अभीप्सा है।83
इस प्रकार आत्मवीर्य-आन्तरिक शक्ति या पराक्रम को समुदित करने की दृष्टि से ग्रंथकार का यह विवेचन बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यह चिन्तन साधक को उसके शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार कराता है। उसका चिन्तन क्रम और आगे बढ़ता है। मैं अनन्तवीर्य, अनन्त विज्ञान, अनन्त आनन्द स्वरूप हूँ। मेरे इस अनन्तवीर्य आदि के प्रतिपक्षी-विरोधी शत्रु कर्म हैं जो वटवृक्ष के तुल्य हैं। क्या मैं इनका मूलोच्छेद न करूँ ? मैं अपने सामर्थ्य को इसी समय प्राप्त कर परमानन्दमय आत्ममदिर में प्रवेश कर अपने स्वरूप से कदापि प्रच्युत न बनूँ। बाह्य पदार्थों में रही हुई अपनी वांछा का नाश कर जब मैं आत्मस्वरूप में स्थिर होता हूँ तब आनन्दमय बन जाता हूँ। फिर अन्य वांछाओं का कोई स्थान ही नहीं रहता। अपने इस स्वरूप में मैं स्थिर क्यों न बना रहँ।84 83. वही, 31.1-9 84. वही, 31.14-15 ~~~~~~~~~~~~~~~ 40 ~~~~~~~~~~~~~~~
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org