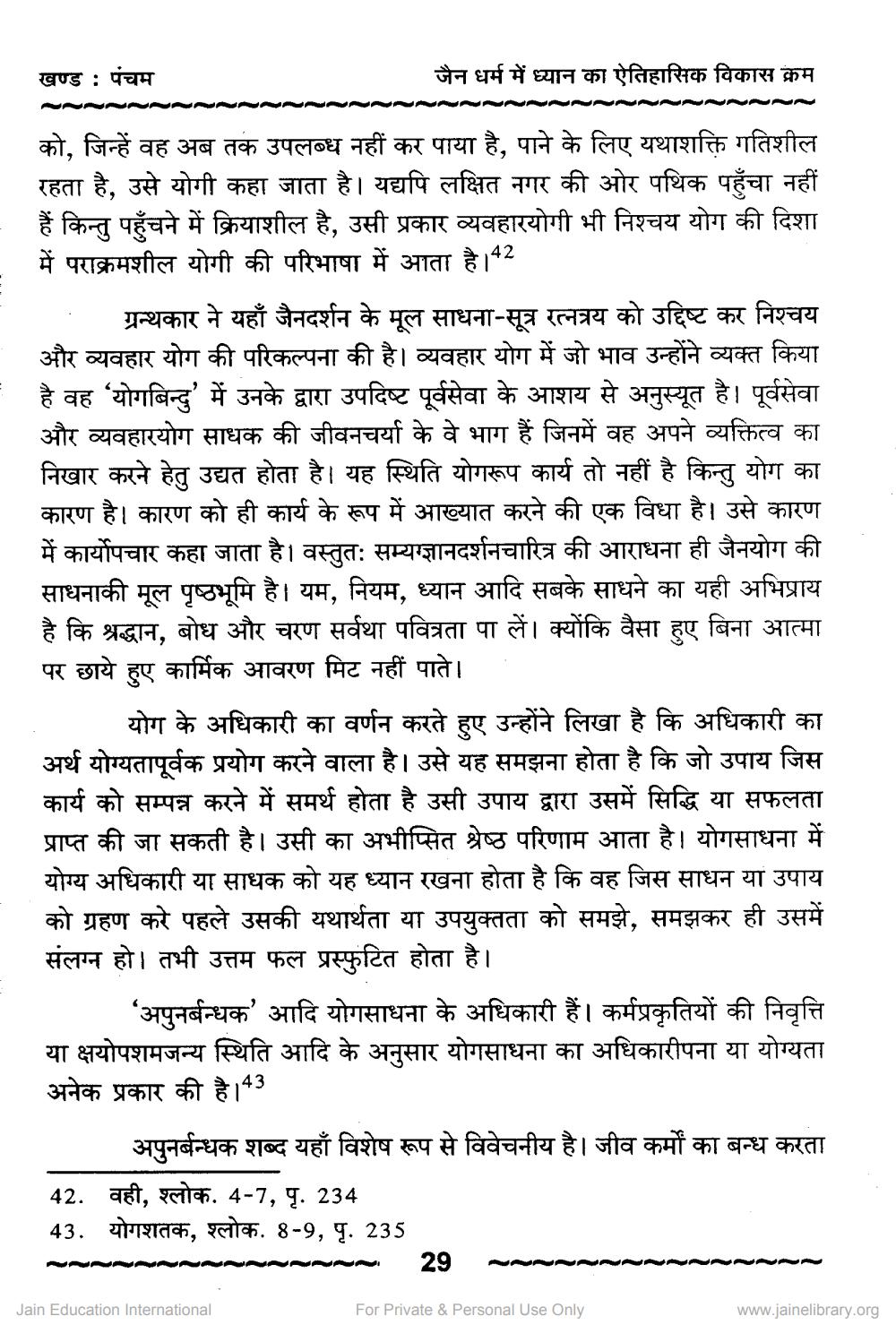________________
खण्ड : पंचम
जैन धर्म में ध्यान का ऐतिहासिक विकास क्रम
को, जिन्हें वह अब तक उपलब्ध नहीं कर पाया है, पाने के लिए यथाशक्ति गतिशील रहता है, उसे योगी कहा जाता है। यद्यपि लक्षित नगर की ओर पथिक पहुँचा नहीं हैं किन्तु पहुँचने में क्रियाशील है, उसी प्रकार व्यवहारयोगी भी निश्चय योग की दिशा में पराक्रमशील योगी की परिभाषा में आता है।42 _ ग्रन्थकार ने यहाँ जैनदर्शन के मूल साधना-सूत्र रत्नत्रय को उद्दिष्ट कर निश्चय
और व्यवहार योग की परिकल्पना की है। व्यवहार योग में जो भाव उन्होंने व्यक्त किया है वह 'योगबिन्दु' में उनके द्वारा उपदिष्ट पूर्वसेवा के आशय से अनुस्यूत है। पूर्वसेवा
और व्यवहारयोग साधक की जीवनचर्या के वे भाग हैं जिनमें वह अपने व्यक्तित्व का निखार करने हेतु उद्यत होता है। यह स्थिति योगरूप कार्य तो नहीं है किन्तु योग का कारण है। कारण को ही कार्य के रूप में आख्यात करने की एक विधा है। उसे कारण में कार्योपचार कहा जाता है। वस्तुत: सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्र की आराधना ही जैनयोग की साधनाकी मूल पृष्ठभूमि है। यम, नियम, ध्यान आदि सबके साधने का यही अभिप्राय है कि श्रद्धान, बोध और चरण सर्वथा पवित्रता पा लें। क्योंकि वैसा हुए बिना आत्मा पर छाये हुए कार्मिक आवरण मिट नहीं पाते।
योग के अधिकारी का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि अधिकारी का अर्थ योग्यतापूर्वक प्रयोग करने वाला है। उसे यह समझना होता है कि जो उपाय जिस कार्य को सम्पन्न करने में समर्थ होता है उसी उपाय द्वारा उसमें सिद्धि या सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसी का अभीप्सित श्रेष्ठ परिणाम आता है। योगसाधना में योग्य अधिकारी या साधक को यह ध्यान रखना होता है कि वह जिस साधन या उपाय को ग्रहण करे पहले उसकी यथार्थता या उपयुक्तता को समझे, समझकर ही उसमें संलग्न हो। तभी उत्तम फल प्रस्फुटित होता है।
'अपुनर्बन्धक' आदि योगसाधना के अधिकारी हैं। कर्मप्रकृतियों की निवृत्ति या क्षयोपशमजन्य स्थिति आदि के अनुसार योगसाधना का अधिकारीपना या योग्यता अनेक प्रकार की है।43
अपुनर्बन्धक शब्द यहाँ विशेष रूप से विवेचनीय है। जीव कर्मों का बन्ध करता 42. वही, श्लोक. 4-7, पृ. 234 43. योगशतक, श्लोक. 8-9, पृ. 235 cmmmmmmmmmmmmmmm 29 mmmmmmmmmmm~~~~
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org