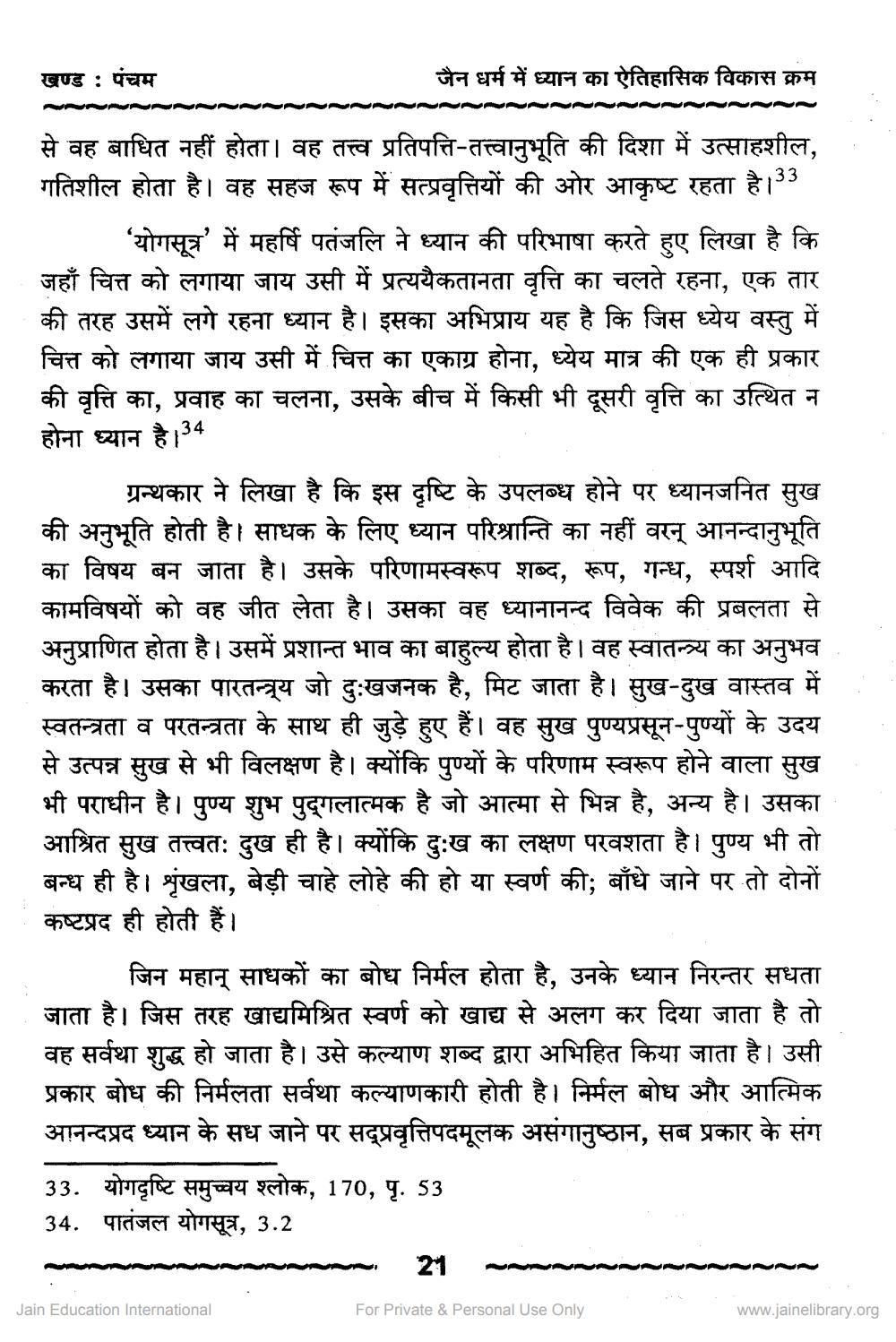________________
खण्ड : पंचम
जैन धर्म में ध्यान का ऐतिहासिक विकास क्रम
से वह बाधित नहीं होता । वह तत्त्व प्रतिपत्ति-तत्त्वानुभूति की दिशा में उत्साहशील, गतिशील होता है। वह सहज रूप में सत्प्रवृत्तियों की ओर आकृष्ट रहता है ।
33
'योगसूत्र' में महर्षि पतंजलि ने ध्यान की परिभाषा करते हुए लिखा है कि जहाँ चित्त को लगाया जाय उसी में प्रत्ययैकतानता वृत्ति का चलते रहना, एक तार की तरह उसमें लगे रहना ध्यान है । इसका अभिप्राय यह है कि जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाय उसी में चित्त का एकाग्र होना, ध्येय मात्र की एक ही प्रकार की वृत्ति का प्रवाह का चलना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का उत्थित न होना ध्यान है । 34
ग्रन्थकार ने लिखा है कि इस दृष्टि के उपलब्ध होने पर ध्यानजनित सुख की अनुभूति होती है। साधक के लिए ध्यान परिश्रान्ति का नहीं वरन् आनन्दानुभूति का विषय बन जाता है। उसके परिणामस्वरूप शब्द, रूप, गन्ध, स्पर्श आदि कामविषयों को वह जीत लेता है। उसका वह ध्यानानन्द विवेक की प्रबलता से अनुप्राणित होता है। उसमें प्रशान्त भाव का बाहुल्य होता है । वह स्वातन्त्र्य का अनुभव करता है। उसका पारतन्त्र्य जो दुःखजनक है, मिट जाता है। सुख-दुख वास्तव में स्वतन्त्रता व परतन्त्रता के साथ ही जुड़े हुए हैं। वह सुख पुण्यप्रसून - पुण्यों के उदय से उत्पन्न सुख से भी विलक्षण है। क्योंकि पुण्यों के परिणाम स्वरूप होने वाला सुख भी पराधीन है । पुण्य शुभ पुद्गलात्मक है जो आत्मा से भिन्न है, अन्य है। उसका आश्रित सुख तत्त्वतः दुख ही है। क्योंकि दुःख का लक्षण परवशता है। पुण्य भी तो बन्ध ही है। श्रृंखला, बेड़ी चाहे लोहे की हो या स्वर्ण की; बाँधे जाने पर तो दोनों कष्टप्रद ही होती हैं।
जिन महान् साधकों का बोध निर्मल होता है, उनके ध्यान निरन्तर सधता जाता है । जिस तरह खाद्यमिश्रित स्वर्ण को खाद्य से अलग कर दिया जाता है तो वह सर्वथा शुद्ध हो जाता है। उसे कल्याण शब्द द्वारा अभिहित किया जाता है । उसी प्रकार बोध की निर्मलता सर्वथा कल्याणकारी होती है। निर्मल बोध और आत्मिक आनन्दप्रद ध्यान के सध जाने पर सद्प्रवृत्तिपदमूलक असंगानुष्ठान, सब प्रकार के संग 33. योगदृष्टि समुच्चय श्लोक, 170, पृ. 53 34. पातंजल योगसूत्र, 3.2
Jain Education International
21
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org