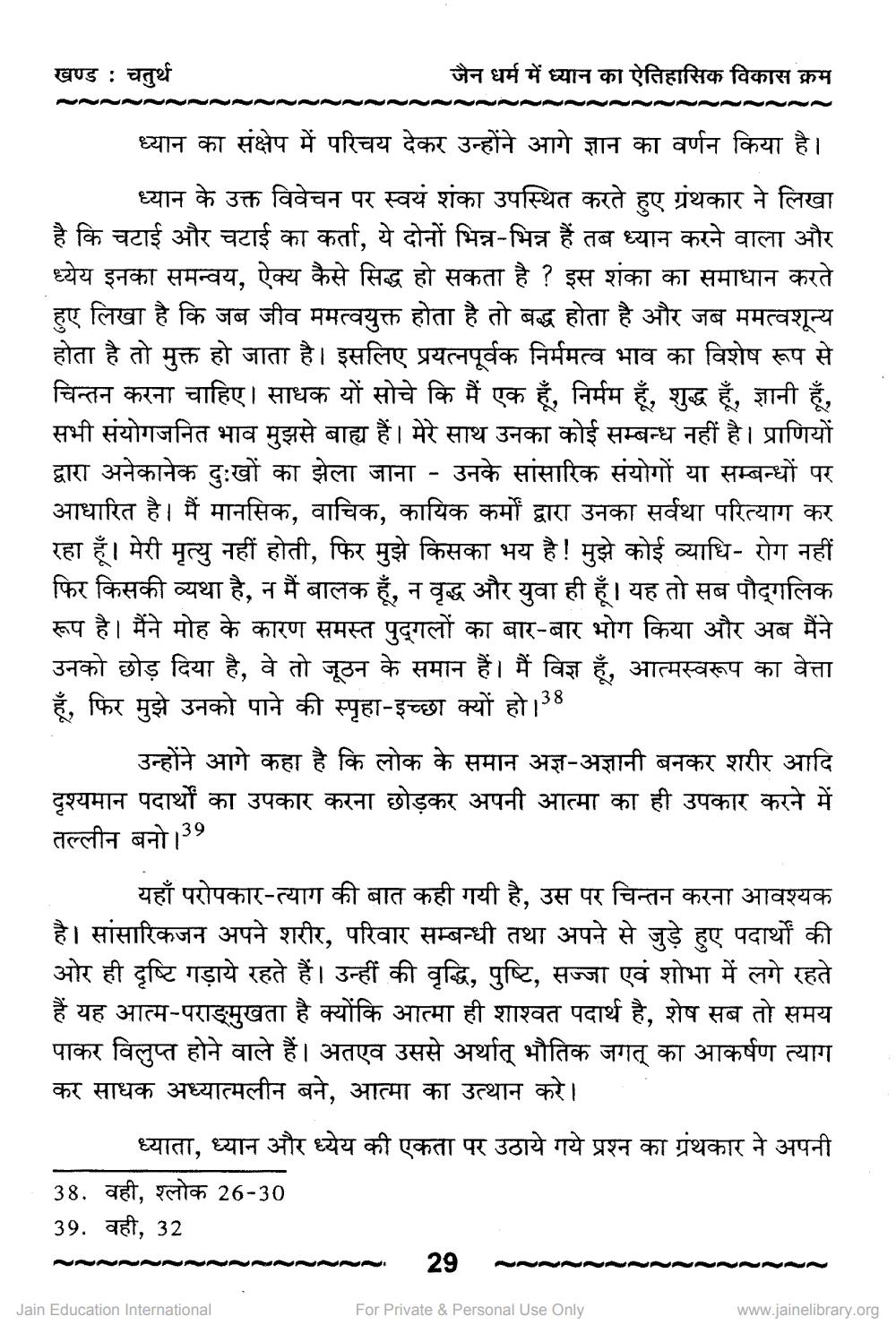________________
खण्ड : चतुर्थ
जैन धर्म में ध्यान का ऐतिहासिक विकास क्रम
ध्यान का संक्षेप में परिचय देकर उन्होंने आगे ज्ञान का वर्णन किया है।
ध्यान के उक्त विवेचन पर स्वयं शंका उपस्थित करते हुए ग्रंथकार ने लिखा है कि चटाई और चटाई का कर्ता, ये दोनों भिन्न-भिन्न हैं तब ध्यान करने वाला और ध्येय इनका समन्वय, ऐक्य कैसे सिद्ध हो सकता है ? इस शंका का समाधान करते हए लिखा है कि जब जीव ममत्वयुक्त होता है तो बद्ध होता है और जब ममत्वशून्य होता है तो मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक निर्ममत्व भाव का विशेष रूप से चिन्तन करना चाहिए। साधक यों सोचे कि मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, सभी संयोगजनित भाव मुझसे बाह्य हैं। मेरे साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। प्राणियों द्वारा अनेकानेक दु:खों का झेला जाना - उनके सांसारिक संयोगों या सम्बन्धों पर आधारित है। मैं मानसिक, वाचिक, कायिक कर्मों द्वारा उनका सर्वथा परित्याग कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु नहीं होती, फिर मुझे किसका भय है! मुझे कोई व्याधि- रोग नहीं फिर किसकी व्यथा है, न मैं बालक हूँ, न वृद्ध और युवा ही हूँ। यह तो सब पौद्गलिक रूप है। मैंने मोह के कारण समस्त पुद्गलों का बार-बार भोग किया और अब मैंने उनको छोड़ दिया है, वे तो जूठन के समान हैं। मैं विज्ञ हूँ, आत्मस्वरूप का वेत्ता हूँ, फिर मुझे उनको पाने की स्पृहा-इच्छा क्यों हो।38
उन्होंने आगे कहा है कि लोक के समान अज्ञ-अज्ञानी बनकर शरीर आदि दृश्यमान पदार्थों का उपकार करना छोड़कर अपनी आत्मा का ही उपकार करने में तल्लीन बनो।
यहाँ परोपकार-त्याग की बात कही गयी है, उस पर चिन्तन करना आवश्यक है। सांसारिकजन अपने शरीर, परिवार सम्बन्धी तथा अपने से जुड़े हुए पदार्थों की
ओर ही दृष्टि गड़ाये रहते हैं। उन्हीं की वृद्धि, पुष्टि, सज्जा एवं शोभा में लगे रहते हैं यह आत्म-पराङ्मुखता है क्योंकि आत्मा ही शाश्वत पदार्थ है, शेष सब तो समय पाकर विलुप्त होने वाले हैं। अतएव उससे अर्थात् भौतिक जगत् का आकर्षण त्याग कर साधक अध्यात्मलीन बने, आत्मा का उत्थान करे।
ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकता पर उठाये गये प्रश्न का ग्रंथकार ने अपनी 38. वही, श्लोक 26-30 39. वही, 32
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org