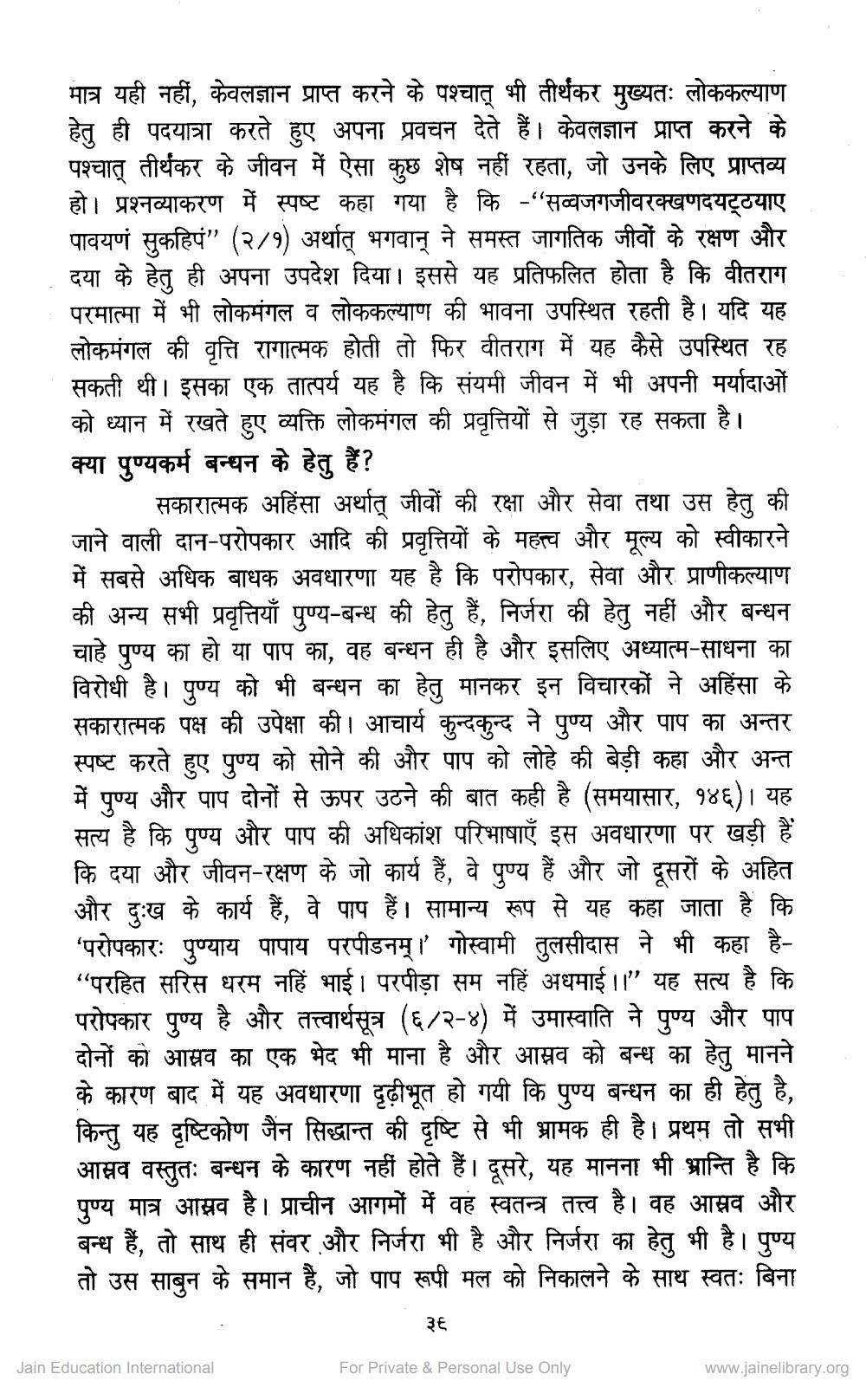________________
मात्र यही नहीं, केवलज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् भी तीर्थंकर मुख्यतः लोककल्याण हेतु ही पदयात्रा करते हुए अपना प्रवचन देते हैं। केवलज्ञान प्राप्त करने के पश्चात तीर्थकर के जीवन में ऐसा कुछ शेष नहीं रहता, जो उनके लिए प्राप्तव्य हो। प्रश्नव्याकरण में स्पष्ट कहा गया है कि - "सव्वजगजीवरक्खणदयट्टयाए पावयणं सुकहिपं" (२/१) अर्थात् भगवान ने समस्त जागतिक जीवों के रक्षण और दया के हेतु ही अपना उपदेश दिया। इससे यह प्रतिफलित होता है कि वीतराग परमात्मा में भी लोकमंगल व लोककल्याण की भावना उपस्थित रहती है। यदि यह लोकमंगल की वृत्ति रागात्मक होती तो फिर वीतराग में यह कैसे उपस्थित रह सकती थी। इसका एक तात्पर्य यह है कि संयमी जीवन में भी अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति लोकमंगल की प्रवृत्तियों से जुड़ा रह सकता है। क्या पुण्यकर्म बन्धन के हेतु हैं?
सकारात्मक अहिंसा अर्थात् जीवों की रक्षा और सेवा तथा उस हेतु की जाने वाली दान-परोपकार आदि की प्रवृत्तियों के महत्त्व और मूल्य को स्वीकारने में सबसे अधिक बाधक अवधारणा यह है कि परोपकार, सेवा और प्राणीकल्याण की अन्य सभी प्रवृत्तियाँ पुण्य-बन्ध की हेतु हैं, निर्जरा की हेतु नहीं और बन्धन चाहे पुण्य का हो या पाप का, वह बन्धन ही है और इसलिए अध्यात्म-साधना का विरोधी है। पुण्य को भी बन्धन का हेतु मानकर इन विचारकों ने अहिंसा के सकारात्मक पक्ष की उपेक्षा की। आचार्य कुन्दकुन्द ने पुण्य और पाप का अन्तर स्पष्ट करते हुए पुण्य को सोने की और पाप को लोहे की बेडी कहा और अन्त में पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठने की बात कही है (समयासार, १४६)। यह सत्य है कि पुण्य और पाप की अधिकांश परिभाषाएँ इस अवधारणा पर खड़ी हैं कि दया और जीवन-रक्षण के जो कार्य हैं, वे पुण्य हैं और जो दूसरों के अहित
और दुःख के कार्य हैं, वे पाप हैं। सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि 'परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।' गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है"परहित सरिस धरम नहिं भाई। परपीड़ा सम नहिं अधमाई ।।" यह सत्य है कि परोपकार पुण्य है और तत्त्वार्थसूत्र (६/२-४) में उमास्वाति ने पुण्य और पाप दोनों को आनव का एक भेद भी माना है और आसव को बन्ध का हेतु मानने के कारण बाद में यह अवधारणा दृढ़ीभूत हो गयी कि पुण्य बन्धन का ही हेतु है, किन्तु यह दृष्टिकोण जैन सिद्धान्त की दृष्टि से भी भ्रामक ही है। प्रथम तो सभी आनव वस्तुतः बन्धन के कारण नहीं होते हैं। दूसरे, यह मानना भी भ्रान्ति है कि पुण्य मात्र आम्रव है। प्राचीन आगमों में वह स्वतन्त्र तत्त्व है। वह आसव और बन्ध हैं, तो साथ ही संवर और निर्जरा भी है और निर्जरा का हेतु भी है। पुण्य तो उस साबुन के समान है, जो पाप रूपी मल को निकालने के साथ स्वतः बिना
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org