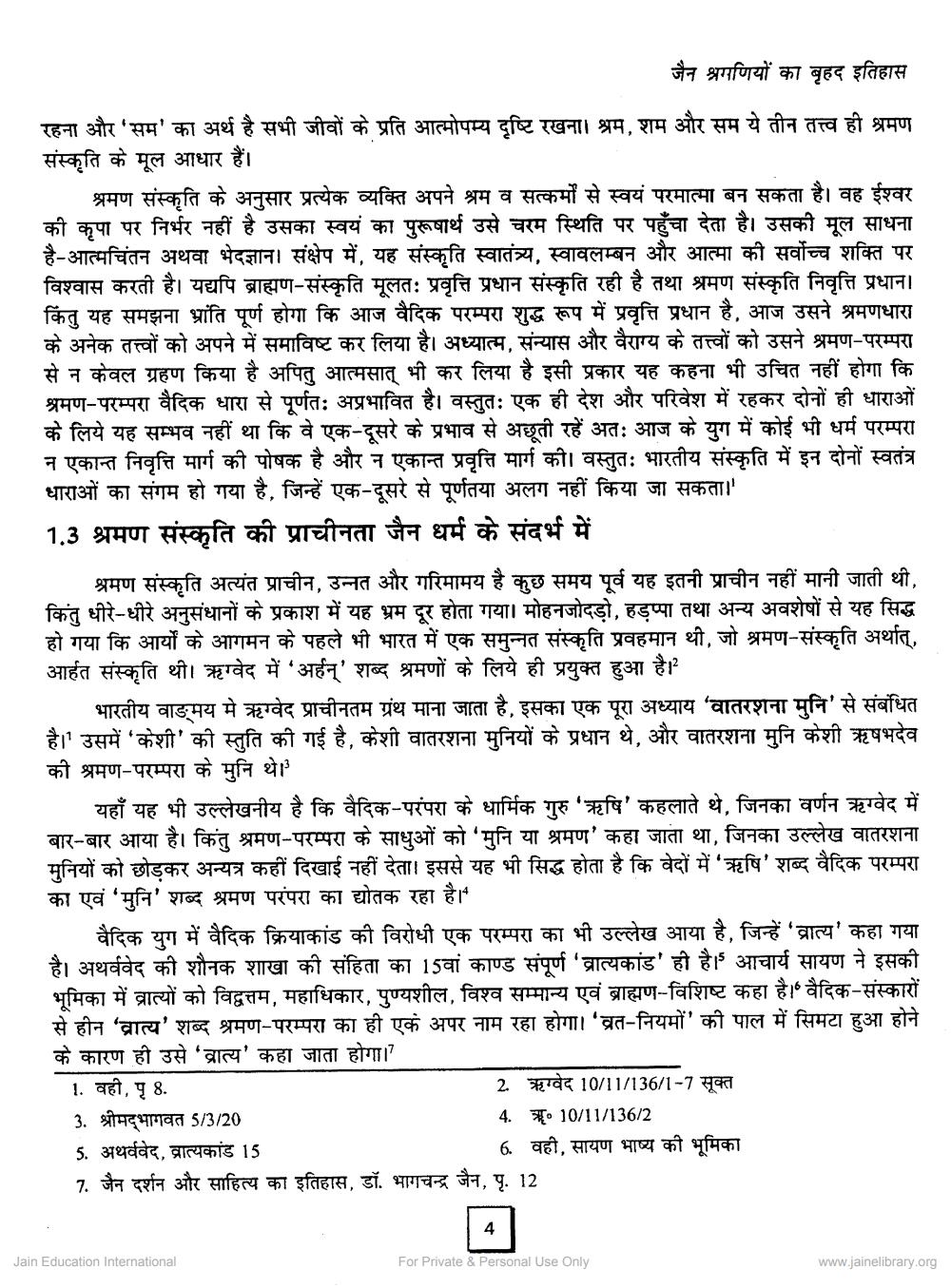________________
जैन श्रमणियों का बृहद इतिहास
रहना और 'सम' का अर्थ है सभी जीवों के प्रति आत्मोपम्य दृष्टि रखना। श्रम, शम और सम ये तीन तत्त्व ही श्रमण संस्कृति के मूल आधार हैं।
श्रमण संस्कृति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम व सत्कर्मों से स्वयं परमात्मा बन सकता है। वह ईश्वर की कृपा पर निर्भर नहीं है उसका स्वयं का पुरूषार्थ उसे चरम स्थिति पर पहुँचा देता है। उसकी मूल साधना है-आत्मचिंतन अथवा भेदज्ञान। संक्षेप में, यह संस्कृति स्वातंत्र्य, स्वावलम्बन और आत्मा की सर्वोच्च शक्ति पर विश्वास करती है। यद्यपि ब्राह्मण-संस्कृति मूलतः प्रवृत्ति प्रधान संस्कृति रही है तथा श्रमण संस्कृति निवृत्ति प्रधान। किंतु यह समझना भ्रांति पूर्ण होगा कि आज वैदिक परम्परा शुद्ध रूप में प्रवृत्ति प्रधान है, आज उसने श्रमणधारा के अनेक तत्त्वों को अपने में समाविष्ट कर लिया है। अध्यात्म, संन्यास और वैराग्य के तत्त्वों को उसने श्रमण-परम्परा से न केवल ग्रहण किया है अपितु आत्मसात् भी कर लिया है इसी प्रकार यह कहना भी उचित नहीं होगा कि श्रमण-परम्परा वैदिक धारा से पूर्णतः अप्रभावित है। वस्तुतः एक ही देश और परिवेश में रहकर दोनों ही धाराओं के लिये यह सम्भव नहीं था कि वे एक-दूसरे के प्रभाव से अछूती रहें अत: आज के युग में कोई भी धर्म परम्परा न एकान्त निवृत्ति मार्ग की पोषक है और न एकान्त प्रवृत्ति मार्ग की। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में इन दोनों स्वतंत्र धाराओं का संगम हो गया है, जिन्हें एक-दूसरे से पूर्णतया अलग नहीं किया जा सकता।' 1.3 श्रमण संस्कृति की प्राचीनता जैन धर्म के संदर्भ में
श्रमण संस्कृति अत्यंत प्राचीन, उन्नत और गरिमामय है कुछ समय पूर्व यह इतनी प्राचीन नहीं मानी जाती थी, किंतु धीरे-धीरे अनुसंधानों के प्रकाश में यह भ्रम दूर होता गया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा अन्य अवशेषों से यह सिद्ध हो गया कि आर्यों के आगमन के पहले भी भारत में एक समुन्नत संस्कृति प्रवहमान थी, जो श्रमण-संस्कृति अर्थात्, आर्हत संस्कृति थी। ऋग्वेद में 'अर्हन्' शब्द श्रमणों के लिये ही प्रयुक्त हुआ है।
भारतीय वाङ्मय मे ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, इसका एक पूरा अध्याय 'वातरशना मुनि' से संबंधित है। उसमें 'केशी' की स्तति की गई है, केशी वातरशना मुनियों के प्रधान थे, और वातरशना मुनि केशी ऋषभदेव की श्रमण-परम्परा के मुनि थे।'
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वैदिक-परंपरा के धार्मिक गुरु 'ऋषि' कहलाते थे, जिनका वर्णन ऋग्वेद में बार-बार आया है। किंतु श्रमण-परम्परा के साधुओं को 'मुनि या श्रमण' कहा जाता था, जिनका उल्लेख वातरशना मुनियों को छोड़कर अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता। इससे यह भी सिद्ध होता है कि वेदों में 'ऋषि' शब्द वैदिक परम्परा का एवं 'मुनि' शब्द श्रमण परंपरा का द्योतक रहा है।'
वैदिक युग में वैदिक क्रियाकांड की विरोधी एक परम्परा का भी उल्लेख आया है, जिन्हें 'व्रात्य' कहा गया है। अथर्ववेद की शौनक शाखा की संहिता का 15वां काण्ड संपूर्ण 'व्रात्यकांड' ही है। आचार्य सायण ने इसकी भूमिका में व्रात्यों को विद्वत्तम, महाधिकार, पुण्यशील, विश्व सम्मान्य एवं ब्राह्मण-विशिष्ट कहा है। वैदिक-संस्कारों से हीन 'व्रात्य' शब्द श्रमण-परम्परा का ही एक अपर नाम रहा होगा। 'व्रत-नियमों' की पाल में सिमटा हआ होने के कारण ही उसे 'व्रात्य' कहा जाता होगा।' 1. वही, पृ8.
2. ऋग्वेद 10/11/136/1-7 सूक्त 3. श्रीमद्भागवत 5/3/20
4. ऋ. 10/11/136/2 5. अथर्ववेद, व्रात्यकांड 15
6. वही, सायण भाष्य की भूमिका 7. जैन दर्शन और साहित्य का इतिहास, डॉ. भागचन्द्र जैन, पृ. 12
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org