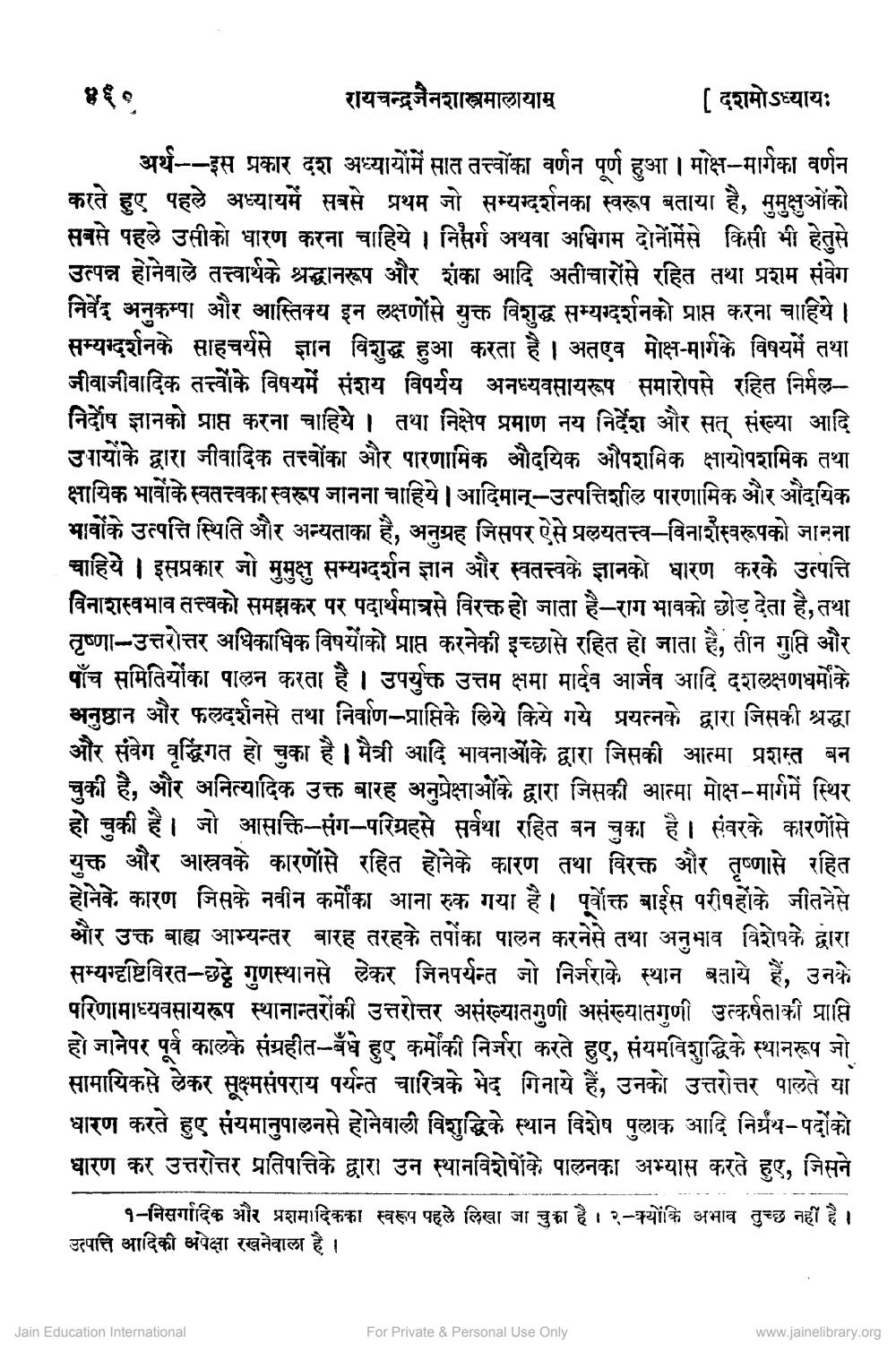________________
१६९.
रायचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम् [ दशमोऽध्यायः अर्थ--इस प्रकार दश अध्यायोंमें सात तत्त्वोंका वर्णन पूर्ण हुआ। माक्ष-मार्गका वर्णन करते हुए पहले अध्यायमें सबसे प्रथम जो सम्यग्दर्शनका स्वरूप बताया है, मुमुक्षुओंको सबसे पहले उसीको धारण करना चाहिये । निसर्ग अथवा अधिगम दोनों से किसी भी हेतुसे उत्पन्न होनेवाले तत्त्वार्थके श्रद्धानरूप और शंका आदि अतीचारोंसे रहित तथा प्रशम संवेग निर्वेद अनुकम्पा और आस्तिक्य इन लक्षणोंसे युक्त विशुद्ध सम्यग्दर्शनको प्राप्त करना चाहिये । सम्यग्दर्शनके साहचर्य से ज्ञान विशुद्ध हुआ करता है । अतएव मोक्ष-मार्गके विषयमें तथा जीवानीवादिक तत्त्वोंके विषयमें संशय विपर्यय अनध्यवसायरूप समारोपप्से रहित निर्मलनिर्दोष ज्ञानको प्राप्त करना चाहिये। तथा निक्षेप प्रमाण नय निर्देश और सत् संख्या आदि उपायोंके द्वारा जीवादिक तत्त्वोंका और पारणामिक औदयिक औपशमिक क्षायोपशमिक तथा क्षायिक भावोंके स्वतत्त्वका स्वरूप जानना चाहिये।आदिमान-उत्पत्तिशील पारणामिक और औदायक भावोंके उत्पत्ति स्थिति और अन्यताका है, अनुग्रह जिसपर ऐसे प्रलयतत्त्व-विनाशैस्वरूपको जानना चाहिये । इसप्रकार जो मुमुक्षु सम्यग्दर्शन ज्ञान और स्वतत्त्वके ज्ञानको धारण करके उत्पत्ति विनाशस्वभाव तत्त्वको समझकर पर पदार्थमात्रसे विरक्त हो जाता है-राग भावको छोड देता है, तथा तृष्णा-उत्तरोत्तर अधिकाधिक विषयोंको प्राप्त करनेकी इच्छासे रहित हो जाता है, तीन गुप्ति और पाँच समितियोंका पालन करता है । उपर्युक्त उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि दशलक्षणधर्मोके अनुष्ठान और फलदर्शनसे तथा निर्वाण-प्राप्तिके लिये किये गये प्रयत्नके द्वारा जिसकी श्रद्धा और संवेग वृद्धिंगत हो चुका है। मैत्री आदि भावनाओंके द्वारा जिसकी आत्मा प्रशस्त बन चुकी है, और अनित्यादिक उक्त बारह अनुप्रेक्षाओंके द्वारा जिसकी आत्मा मोक्ष-मार्गमें स्थिर हो चुकी है। जो आसक्ति-संग-परिग्रहसे सर्वथा रहित बन चुका है। संवरके कारणोंसे युक्त और आस्रवके कारणोंसे रहित होनेके कारण तथा विरक्त और तृष्णासे रहित होनेके कारण जिसके नवीन कर्मोंका आना रुक गया है। पूर्वोक्त बाईस परीपहोंके जीतनेसे और उक्त बाह्य आभ्यन्तर बारह तरहके तपोंका पालन करनेसे तथा अनुभाव विशेषके द्वारा सम्यग्दृष्टिविरत-छठे गुणस्थानसे लेकर जिनपर्यन्त जो निर्जराके स्थान बताये हैं, उनके परिणामाध्यवसायरूप स्थानान्तरोंकी उत्तरोत्तर असंख्यातगणी असंख्यातगणी उत्कर्षताकी प्राप्ति हो जानेपर पूर्व कालके संग्रहीत-बँधे हुए कर्मोकी निर्जरा करते हुए, संयमविशुद्धिके स्थानरूप जो सामायिकसे लेकर सूक्ष्मसंपराय पर्यन्त चारित्रके भेद गिनाये हैं, उनको उत्तरोत्तर पालते या धारण करते हुए संयमानुपालनसे होनेवाली विशुद्धिके स्थान विशेष पुलाक आदि निग्रंथ-पदोंको धारण कर उत्तरोत्तर प्रतिपत्तिके द्वारा उन स्थानविशेषोंके पालनका अभ्यास करते हुए, जिसने
१-निसर्गादिक और प्रशमादिकका स्वरूप पहले लिखा जा चुका है । २-क्योंकि अभाव तुच्छ नहीं है। उत्पत्ति आदिकी अपेक्षा रखनेवाला है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org