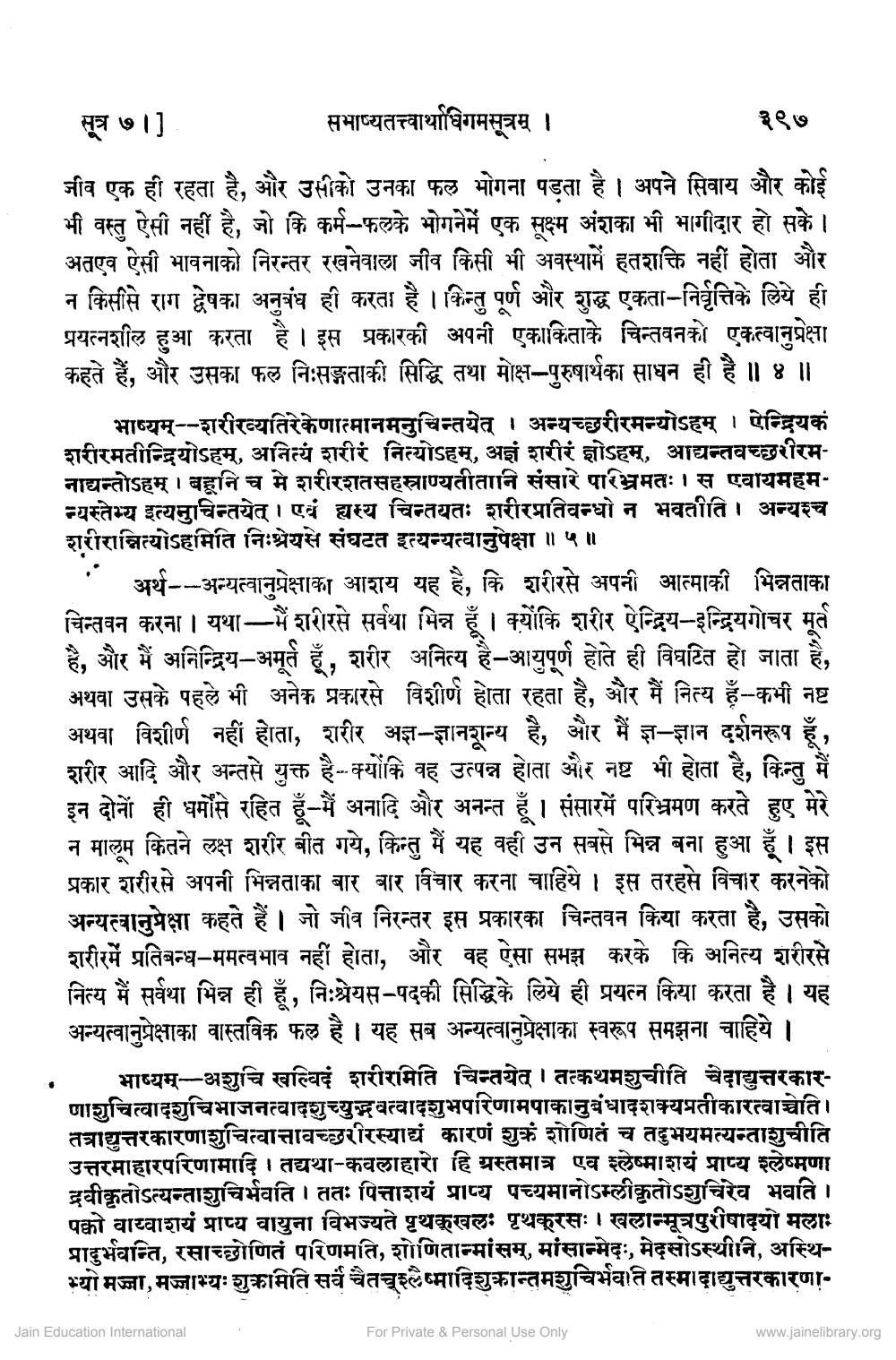________________
३९७
सूत्र ७।]
सभाप्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् । जीव एक ही रहता है, और उसीको उनका फल भोगना पड़ता है। अपने सिवाय और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो कि कर्म-फलके भोगनेमें एक सूक्ष्म अंशका भी भागीदार हो सके। अतएव ऐसी भावनाको निरन्तर रखनेवाला जीव किसी भी अवस्थामें हतशक्ति नहीं होता और न किसीसे राग द्वेषका अनुबंध ही करता है । किन्तु पूर्ण और शुद्ध एकता-निर्वृत्तिके लिये ही प्रयत्नशील हुआ करता है । इस प्रकारकी अपनी एकाकिताके चिन्तवनको एकत्वानुप्रेक्षा कहते हैं, और उसका फल निःसङ्गताकी सिद्धि तथा मोक्ष-पुरुषार्थका साधन ही है ॥ ४ ॥
भाष्यम्--शरीरव्यतिरेकेणात्मानमनुचिन्तयेत् । अन्यच्छरीरमन्योऽहम् । ऐन्द्रियक शरीरमतीन्द्रियोऽहम्, अनित्यं शरीरं नित्योऽहम्, अझं शरीरं ज्ञोऽहम्, आद्यन्तवच्छरीरमनाद्यन्तोऽहम् । बहूनि च मे शरीरशतसहस्राण्यतीतानि संसारे परिभ्रमतः । स एवायमहमन्यस्तेभ्य इत्यनुचिन्तयेत् । एवं ह्यस्य चिन्तयतः शरीरप्रतिवन्धो न भवतीति। अन्यश्च शरीरान्नित्योऽहमिति निःश्रेयसे संघटत इत्यन्यत्वानुपेक्षा ॥ ५॥
- अर्थ--अन्यत्वानुप्रेक्षाका आशय यह है, कि शरीरसे अपनी आत्माकी भिन्नताका चिन्तवन करना । यथा-मैं शरीरसे सर्वथा भिन्न हूँ । क्योंकि शरीर ऐन्द्रिय-इन्द्रियगोचर मूर्त है, और मैं अनिन्द्रिय-अमूर्त हूँ, शरीर अनित्य है-आयुपूर्ण होते ही विघटित हो जाता है, अथवा उसके पहले भी अनेक प्रकारसे विशीर्ण होता रहता है, और मैं नित्य हँ-कभी नष्ट अथवा विशीर्ण नहीं होता, शरीर अज्ञ-ज्ञानशून्य है, और मैं ज्ञ-ज्ञान दर्शनरूप हूँ, शरीर आदि और अन्तसे युक्त है क्योंकि वह उत्पन्न होता और नष्ट भी होता है, किन्तु मैं इन दोनों ही धर्मोंसे रहित हूँ-मैं अनादि और अनन्त हूँ । संसारमें परिभ्रमण करते हुए मेरे न मालूम कितने लक्ष शरीर बीत गये, किन्तु मैं यह वही उन सबसे भिन्न बना हुआ हूँ । इस प्रकार शरीरसे अपनी भिन्नताका बार बार विचार करना चाहिये । इस तरहसे विचार करनेको अन्यत्वानुप्रेक्षा कहते हैं । जो जीव निरन्तर इस प्रकारका चिन्तवन किया करता है, उसको शरीरमें प्रतिबन्ध-ममत्वभाव नहीं होता, और वह ऐसा समझ करके कि अनित्य शरीरसे नित्य मैं सर्वथा भिन्न ही हूँ, निःश्रेयस-पदकी सिद्धिके लिये ही प्रयत्न किया करता है । यह अन्यत्वानुप्रेक्षाका वास्तविक फल है । यह सब अन्यत्वानुप्रेक्षाका स्वरूप समझना चाहिये ।
भाष्यम्-अशुचि खल्विदं शरीरमिति चिन्तयेत् । तत्कथमशुचीति चेदाद्युत्तरकारणाशुचित्वादशुचिभाजनत्वादशुच्युद्भवत्वादशुभपरिणामपाकानुबंधादशक्यप्रतीकारत्वाच्चेति। तत्राद्युत्तरकारणाशुचित्वात्तावच्छरीरस्याचं कारणं शुक्र शोणितं च तदुभयमत्यन्ताशुचीति उत्तरमाहारपरिणामादि । तद्यथा-कवलाहारो हि ग्रस्तमात्र एव श्लेष्माशयं प्राप्य श्लेष्मणा द्रवीकृतोऽत्यन्ताशुचिर्भवति । ततः पित्ताशयं प्राप्य पच्यमानोऽम्लीकृतोऽशुचिरेव भवति । पक्को वाय्वाशयं प्राप्य वायुना विभज्यते पृथक्खलः पृथकूरसः । खलान्मूत्रपुरीषादयो मला: प्रादुर्भवन्ति, रसाच्छोणितं परिणमति, शोणितान्मांसम्, मांसान्मेदः, मेदसोऽस्थीनि, अस्थिभ्यो मज्जा, मज्जाभ्यः शुक्रमिति सर्व चैतच्श्लेष्मादिशुक्रान्तमशुचिर्भवति तस्मादायुत्तरकारणा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org