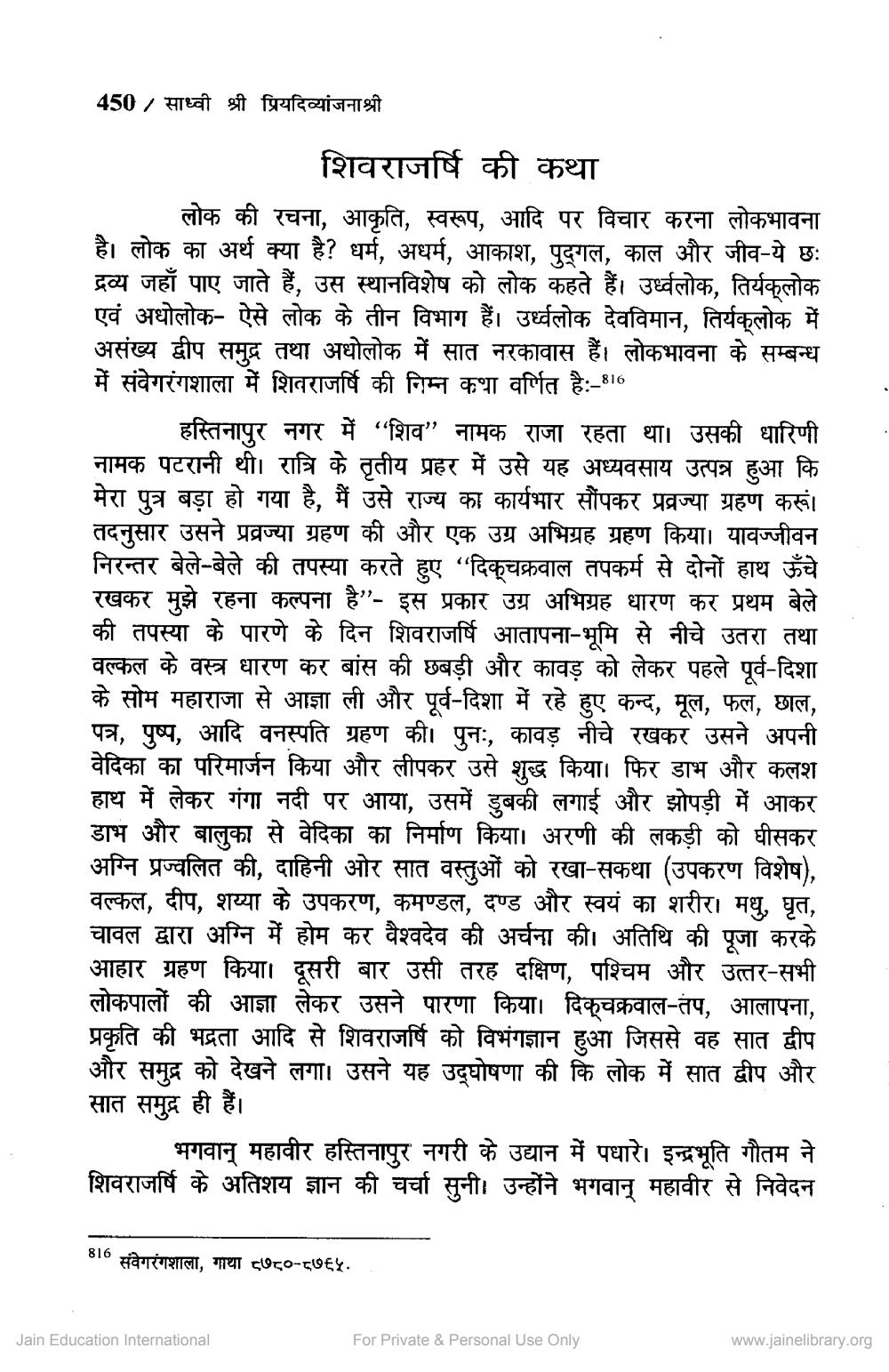________________
450 / साध्वी श्री प्रियदिव्यांजनाश्री
शिवराजर्षि की कथा
लोक की रचना, आकृति, स्वरूप, आदि पर विचार करना लोकभावना है। लोक का अर्थ क्या है? धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, काल और जीव- ये छः द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं, उस स्थानविशेष को लोक कहते हैं। उर्ध्वलोक, तिर्यक्लोक एवं अधोलोक - ऐसे लोक के तीन विभाग हैं। उर्ध्वलोक देवविमान, तिर्यक्लोक में असंख्य द्वीप समुद्र तथा अधोलोक में सात नरकावास हैं। लोकभावना के सम्बन्ध में संवेगरंगशाला में शिवराजर्षि की निम्न कथा वर्णित है:- 816
हस्तिनापुर नगर में "शिव" नामक राजा रहता था। उसकी धारिणी नामक पटरानी थी। रात्रि के तृतीय प्रहर में उसे यह अध्यवसाय उत्पन्न हुआ कि मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, मैं उसे राज्य का कार्यभार सौंपकर प्रव्रज्या ग्रहण करूं । तदनुसार उसने प्रव्रज्या ग्रहण की और एक उग्र अभिग्रह ग्रहण किया । यावज्जीवन निरन्तर बेले- बेले की तपस्या करते हुए “दिक्चक्रवाल तपकर्म से दोनों हाथ ऊँचे रखकर मुझे रहना कल्पना है”- इस प्रकार उग्र अभिग्रह धारण कर प्रथम बेले की तपस्या के पारणे के दिन शिवराजर्षि आतापना - भूमि से नीचे उतरा तथा वल्कल के वस्त्र धारण कर बांस की छबड़ी और कावड़ को लेकर पहले पूर्व-दिशा के सोम महाराजा से आज्ञा ली और पूर्व दिशा में रहे हुए कन्द, मूल, फल, छाल, पत्र, पुष्प, आदि वनस्पति ग्रहण की। पुनः कावड़ नीचे रखकर उसने अपनी वेदिका का परिमार्जन किया और लीपकर उसे शुद्ध किया। फिर डाभ और कलश हाथ में लेकर गंगा नदी पर आया, उसमें डुबकी लगाई और झोपड़ी में आकर डाभ और बालुका से वेदिका का निर्माण किया । अरणी की लकड़ी को घीसकर अग्नि प्रज्वलित की, दाहिनी ओर सात वस्तुओं को रखा - सकथा ( उपकरण विशेष ), वल्कल, दीप, शय्या के उपकरण, कमण्डल, दण्ड और स्वयं का शरीर । मधु, घृत, चावल द्वारा अग्नि में होम कर वैश्वदेव की अर्चना की। अतिथि की पूजा करके आहार ग्रहण किया। दूसरी बार उसी तरह दक्षिण, पश्चिम और उत्तर - सभी लोकपालों की आज्ञा लेकर उसने पारणा किया। दिक्चक्रवाल-तप, आलापना, प्रकृति की भद्रता आदि से शिवराजर्षि को विभंगज्ञान हुआ जिससे वह सात द्वीप और समुद्र को देखने लगा। उसने यह उद्घोषणा की कि लोक में सात द्वीप और सात समुद्र ही हैं।
भगवान् महावीर हस्तिनापुर नगरी के उद्यान में पधारे। इन्द्रभूति गौतम ने शिवराजर्षि के अतिशय ज्ञान की चर्चा सुनी। उन्होंने भगवान् महावीर से निवेदन
816
संवेगरंगशाला, गाथा ८७८०-८७६५.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org