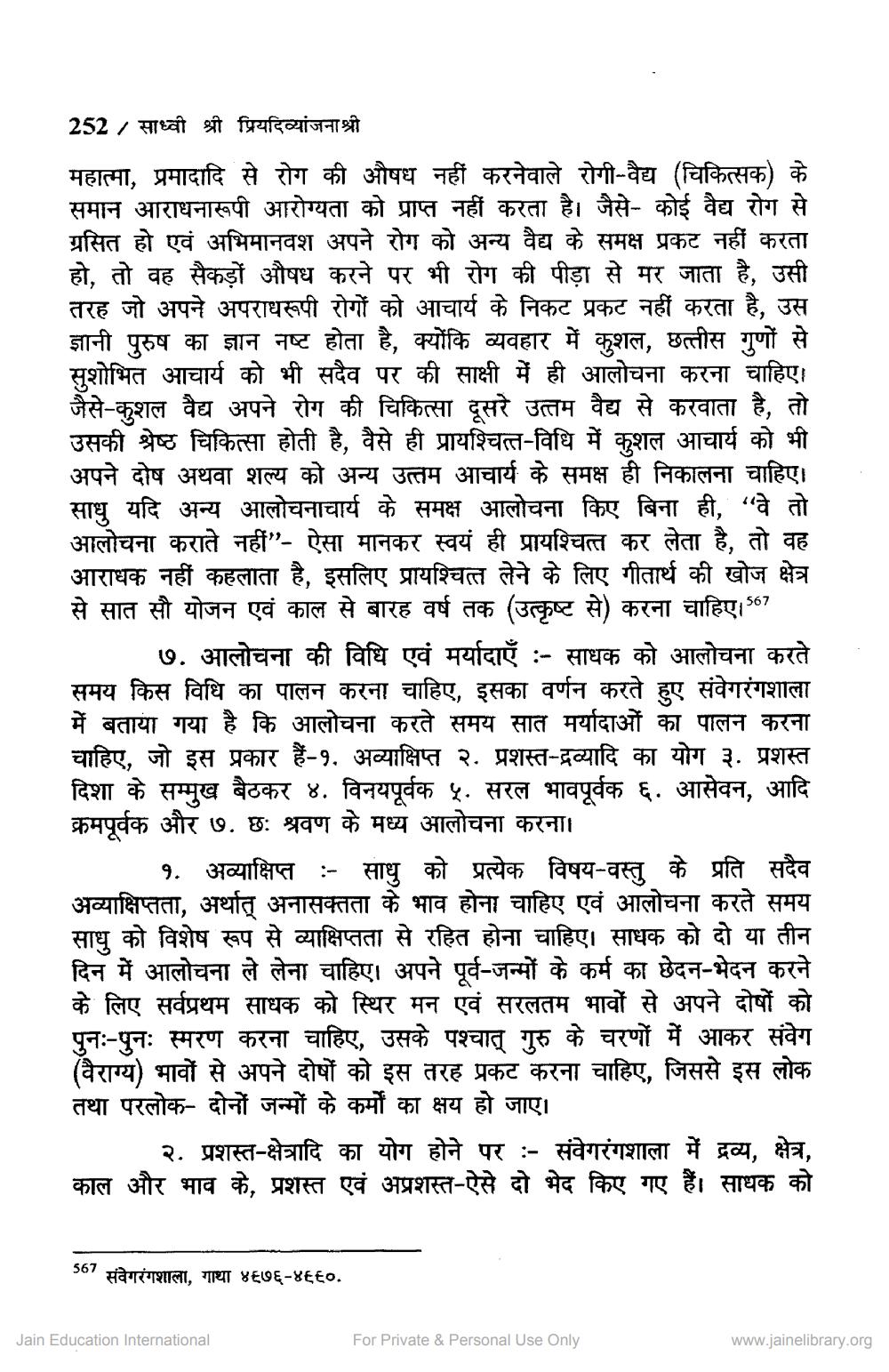________________
252 / साध्वी श्री प्रियदिव्यांजनाश्री महात्मा, प्रमादादि से रोग की औषध नहीं करनेवाले रोगी-वैद्य (चिकित्सक) के समान आराधनारूपी आरोग्यता को प्राप्त नहीं करता है। जैसे- कोई वैद्य रोग से ग्रसित हो एवं अभिमानवश अपने रोग को अन्य वैद्य के समक्ष प्रकट नहीं करता हो, तो वह सैकड़ों औषध करने पर भी रोग की पीड़ा से मर जाता है, उसी तरह जो अपने अपराधरूपी रोगों को आचार्य के निकट प्रकट नहीं करता है, उस ज्ञानी पुरुष का ज्ञान नष्ट होता है, क्योंकि व्यवहार में कुशल, छत्तीस गुणों से सुशोभित आचार्य को भी सदैव पर की साक्षी में ही आलोचना करना चाहिए। जैसे-कुशल वैद्य अपने रोग की चिकित्सा दूसरे उत्तम वैद्य से करवाता है, तो उसकी श्रेष्ठ चिकित्सा होती है, वैसे ही प्रायश्चित्त-विधि में कुशल आचार्य को भी अपने दोष अथवा शल्य को अन्य उत्तम आचार्य के समक्ष ही निकालना चाहिए। साधु यदि अन्य आलोचनाचार्य के समक्ष आलोचना किए बिना ही, "वे तो आलोचना कराते नहीं"- ऐसा मानकर स्वयं ही प्रायश्चित्त कर लेता है, तो वह आराधक नहीं कहलाता है, इसलिए प्रायश्चित्त लेने के लिए गीतार्थ की खोज क्षेत्र से सात सौ योजन एवं काल से बारह वर्ष तक (उत्कृष्ट से) करना चाहिए।67
७. आलोचना की विधि एवं मर्यादाएँ :- साधक को आलोचना करते समय किस विधि का पालन करना चाहिए, इसका वर्णन करते हुए संवेगरंगशाला में बताया गया है कि आलोचना करते समय सात मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, जो इस प्रकार हैं-१. अव्याक्षिप्त २. प्रशस्त-द्रव्यादि का योग ३. प्रशस्त दिशा के सम्मुख बैठकर ४. विनयपूर्वक ५. सरल भावपूर्वक ६. आसेवन, आदि क्रमपूर्वक और ७. छ: श्रवण के मध्य आलोचना करना।
१. अव्याक्षिप्त :- साधु को प्रत्येक विषय-वस्तु के प्रति सदैव अव्याक्षिप्तता, अर्थात् अनासक्तता के भाव होना चाहिए एवं आलोचना करते समय साधु को विशेष रूप से व्याक्षिप्तता से रहित होना चाहिए। साधक को दो या तीन दिन में आलोचना ले लेना चाहिए। अपने पूर्व-जन्मों के कर्म का छेदन-भेदन करने के लिए सर्वप्रथम साधक को स्थिर मन एवं सरलतम भावों से अपने दोषों को पुनः-पुनः स्मरण करना चाहिए, उसके पश्चात् गुरु के चरणों में आकर संवेग (वैराग्य) भावों से अपने दोषों को इस तरह प्रकट करना चाहिए, जिससे इस लोक तथा परलोक- दोनों जन्मों के कर्मों का क्षय हो जाए।
२. प्रशस्त-क्षेत्रादि का योग होने पर :- संवेगरंगशाला में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के, प्रशस्त एवं अप्रशस्त-ऐसे दो भेद किए गए हैं। साधक को
567 संवेगरंगशाला, गाथा ४६७६-४६६०.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org