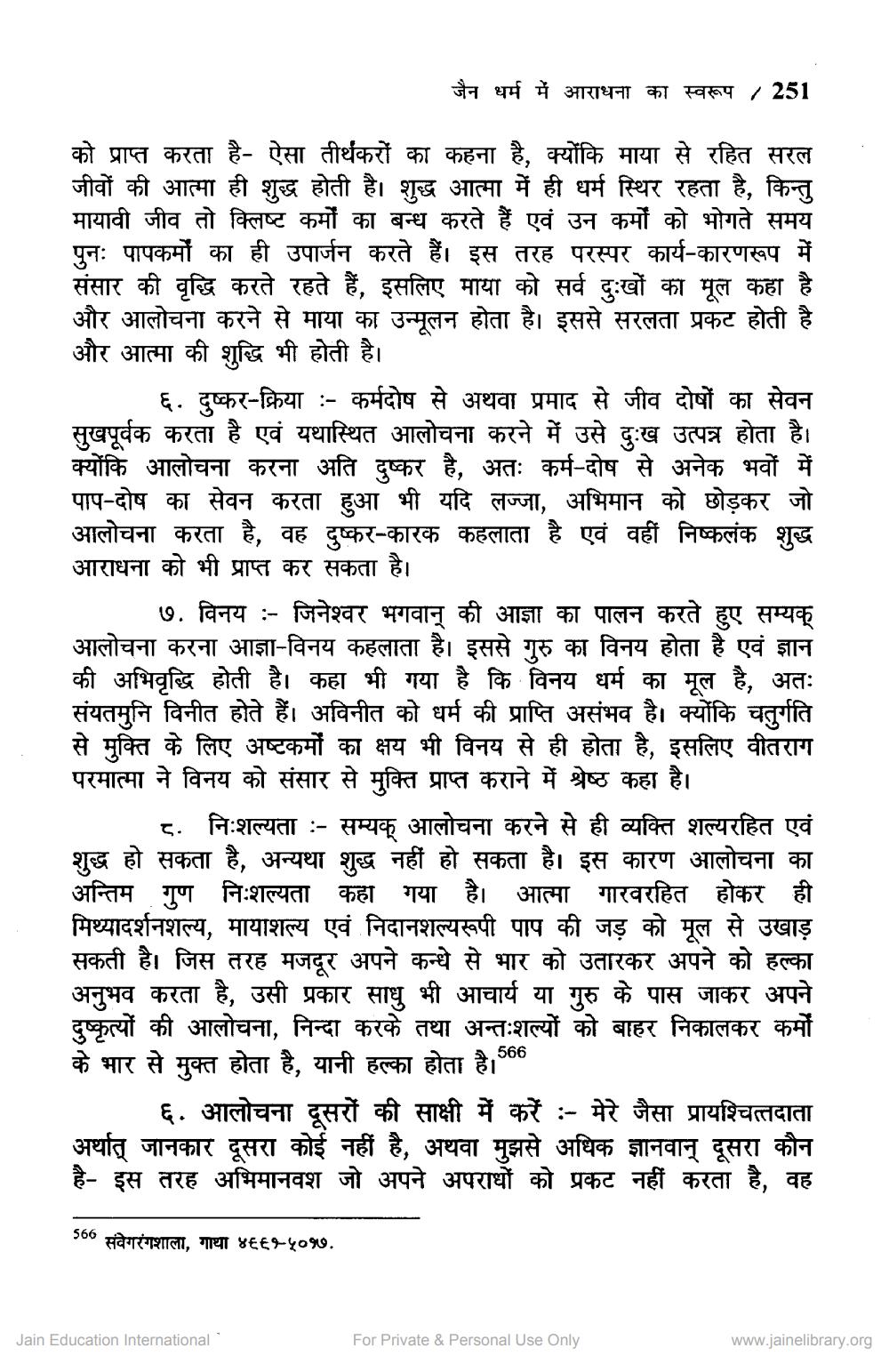________________
जैन धर्म में आराधना का स्वरूप / 251
को प्राप्त करता है- ऐसा तीर्थंकरों का कहना है, क्योंकि माया से रहित सरल जीवों की आत्मा ही शुद्ध होती है। शुद्ध आत्मा में ही धर्म स्थिर रहता है, किन्तु मायावी जीव तो क्लिष्ट कमों का बन्ध करते हैं एवं उन कर्मों को भोगते समय पुनः पापकर्मों का ही उपार्जन करते हैं। इस तरह परस्पर कार्य-कारणरूप में संसार की वृद्धि करते रहते हैं, इसलिए माया को सर्व दुःखों का मूल कहा है और आलोचना करने से माया का उन्मूलन होता है। इससे सरलता प्रकट होती है और आत्मा की शुद्धि भी होती है।
६. दुष्कर-क्रिया :- कर्मदोष से अथवा प्रमाद से जीव दोषों का सेवन सुखपूर्वक करता है एवं यथास्थित आलोचना करने में उसे दुःख उत्पन्न होता है। क्योंकि आलोचना करना अति दुष्कर है, अतः कर्म-दोष से अनेक भवों में पाप-दोष का सेवन करता हुआ भी यदि लज्जा, अभिमान को छोड़कर जो आलोचना करता है, वह दुष्कर-कारक कहलाता है एवं वहीं निष्कलंक शुद्ध आराधना को भी प्राप्त कर सकता है।
७. विनय :- जिनेश्वर भगवान् की आज्ञा का पालन करते हुए सम्यक् आलोचना करना आज्ञा-विनय कहलाता है। इससे गुरु का विनय होता है एवं ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। कहा भी गया है कि विनय धर्म का मूल है, अतः संयतमुनि विनीत होते हैं। अविनीत को धर्म की प्राप्ति असंभव है। क्योंकि चतुर्गति से मुक्ति के लिए अष्टकमों का क्षय भी विनय से ही होता है, इसलिए वीतराग परमात्मा ने विनय को संसार से मुक्ति प्राप्त कराने में श्रेष्ठ कहा है।
८. निःशल्यता :- सम्यक् आलोचना करने से ही व्यक्ति शल्यरहित एवं शुद्ध हो सकता है, अन्यथा शुद्ध नहीं हो सकता है। इस कारण आलोचना का अन्तिम गुण निःशल्यता कहा गया है। आत्मा गारवरहित होकर ही मिथ्यादर्शनशल्य, मायाशल्य एवं निदानशल्यरूपी पाप की जड़ को मूल से उखाड़ सकती है। जिस तरह मजदूर अपने कन्धे से भार को उतारकर अपने को हल्का अनुभव करता है, उसी प्रकार साधु भी आचार्य या गुरु के पास जाकर अपने दुष्कृत्यों की आलोचना, निन्दा करके तथा अन्तःशल्यों को बाहर निकालकर कों के भार से मुक्त होता है, यानी हल्का होता है।566
६. आलोचना दूसरों की साक्षी में करें :- मेरे जैसा प्रायश्चित्तदाता अर्थात् जानकार दूसरा कोई नहीं है, अथवा मुझसे अधिक ज्ञानवान् दूसरा कौन है- इस तरह अभिमानवश जो अपने अपराधों को प्रकट नहीं करता है, वह
२०० संवेगरंगशाला, गाथा ४६६१-५०१७.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org