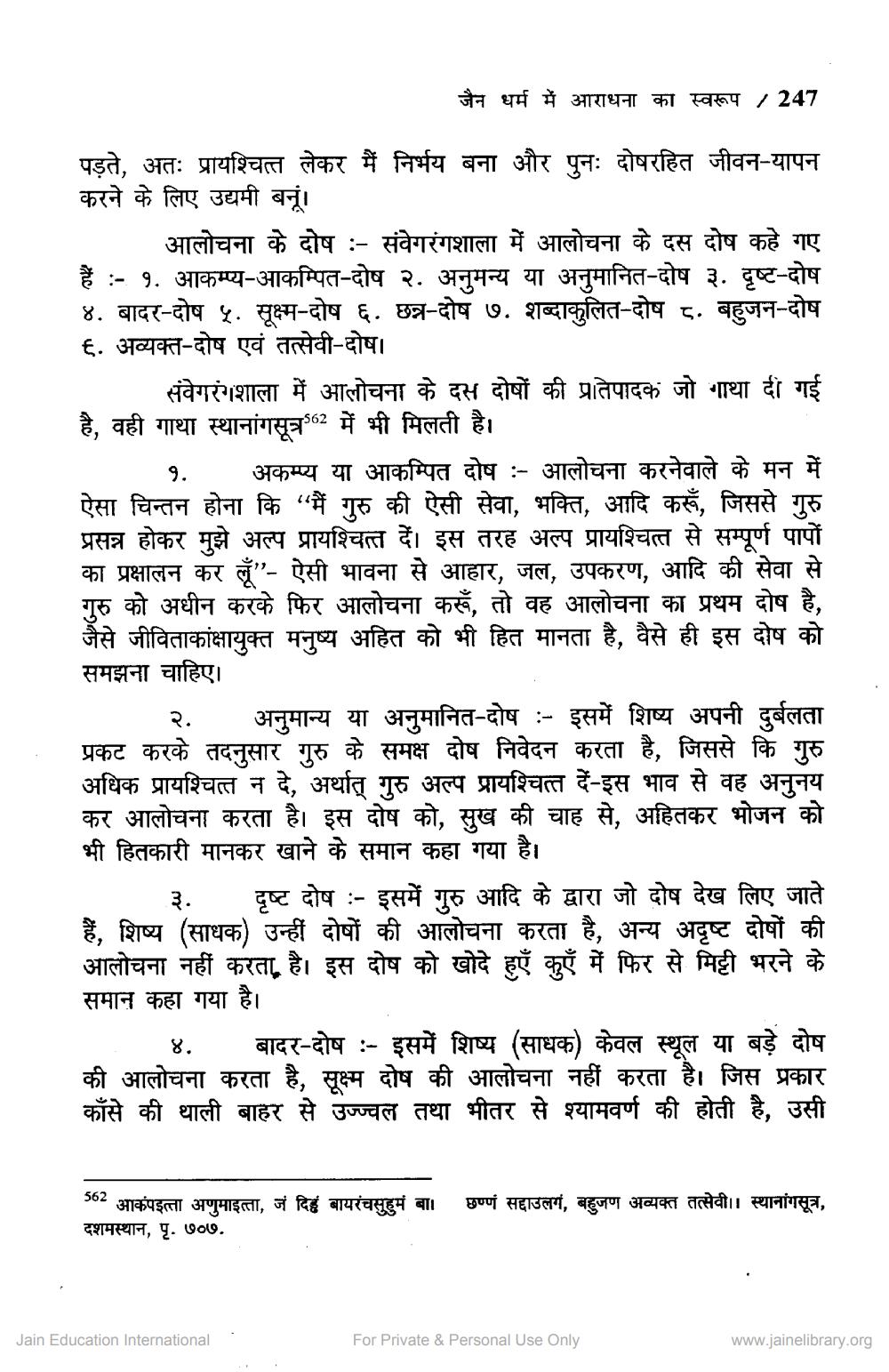________________
जैन धर्म में आराधना का स्वरूप / 247
पड़ते, अतः प्रायश्चित्त लेकर मैं निर्भय बना और पुनः दोषरहित जीवन-यापन करने के लिए उद्यमी बनूं।
आलोचना के दोष :- संवेगरंगशाला में आलोचना के दस दोष कहे गए हैं :- १. आकम्प्य-आकम्पित - दोष २. अनुमन्य या अनुमानित - दोष ३. दृष्ट-दोष ४. बादर - दोष ५. सूक्ष्म-दोष ६ छन्न-दोष ७. शब्दाकुलित - दोष ८. बहुजन - दोष ६. अव्यक्त - दोष एवं तत्सेवी - दोष ।
संवेगरंगशाला में आलोचना के दस दोषों की प्रतिपादक जो गाथा दी गई है, वही गाथा स्थानांगसूत्र 2 में भी मिलती है।
१. अकम्प्य या आकम्पित दोष :- आलोचना करनेवाले के मन में ऐसा चिन्तन होना कि “मैं गुरु की ऐसी सेवा, भक्ति, आदि करूँ, जिससे गुरु प्रसन्न होकर मुझे अल्प प्रायश्चित्त दें। इस तरह अल्प प्रायश्चित्त से सम्पूर्ण पापों का प्रक्षालन कर लूँ”- ऐसी भावना से आहार, जल, उपकरण, आदि की सेवा से गुरु को अधीन करके फिर आलोचना करूँ, तो वह आलोचना का प्रथम दोष है, जैसे जीविताकांक्षायुक्त मनुष्य अहित को भी हित मानता है, वैसे ही इस दोष को समझना चाहिए।
२. अनुमान्य या अनुमानित - दोष :- इसमें शिष्य अपनी दुर्बलता प्रकट करके तदनुसार गुरु के समक्ष दोष निवेदन करता है, जिससे कि गुरु अधिक प्रायश्चित्त न दे, अर्थात् गुरु अल्प प्रायश्चित्त दें - इस भाव से वह अनुनय कर आलोचना करता है। इस दोष को, सुख की चाह से, अहितकर भोजन को भी हितकारी मानकर खाने के समान कहा गया है।
३. दृष्ट दोष :इसमें गुरु आदि के द्वारा जो दोष देख लिए जाते हैं, शिष्य (साधक) उन्हीं दोषों की आलोचना करता है, अन्य अदृष्ट दोषों की आलोचना नहीं करता है। इस दोष को खोदे हुएँ कुएँ में फिर से मिट्टी भरने के समान कहा गया है।
४. बादर - दोष :- इसमें शिष्य ( साधक) केवल स्थूल या बड़े दोष की आलोचना करता है, सूक्ष्म दोष की आलोचना नहीं करता है। जिस प्रकार काँसे की थाली बाहर से उज्ज्वल तथा भीतर से श्यामवर्ण की होती है, उसी
562 आकंपइत्ता अणुमाइत्ता, जं दिडुं बायरंचसुहुमं बा। दशमस्थान, पृ. ७०७.
Jain Education International
छष्णं सद्दाउलगं, बहुजण अव्यक्त तत्सेवी । । स्थानांगसूत्र,
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org