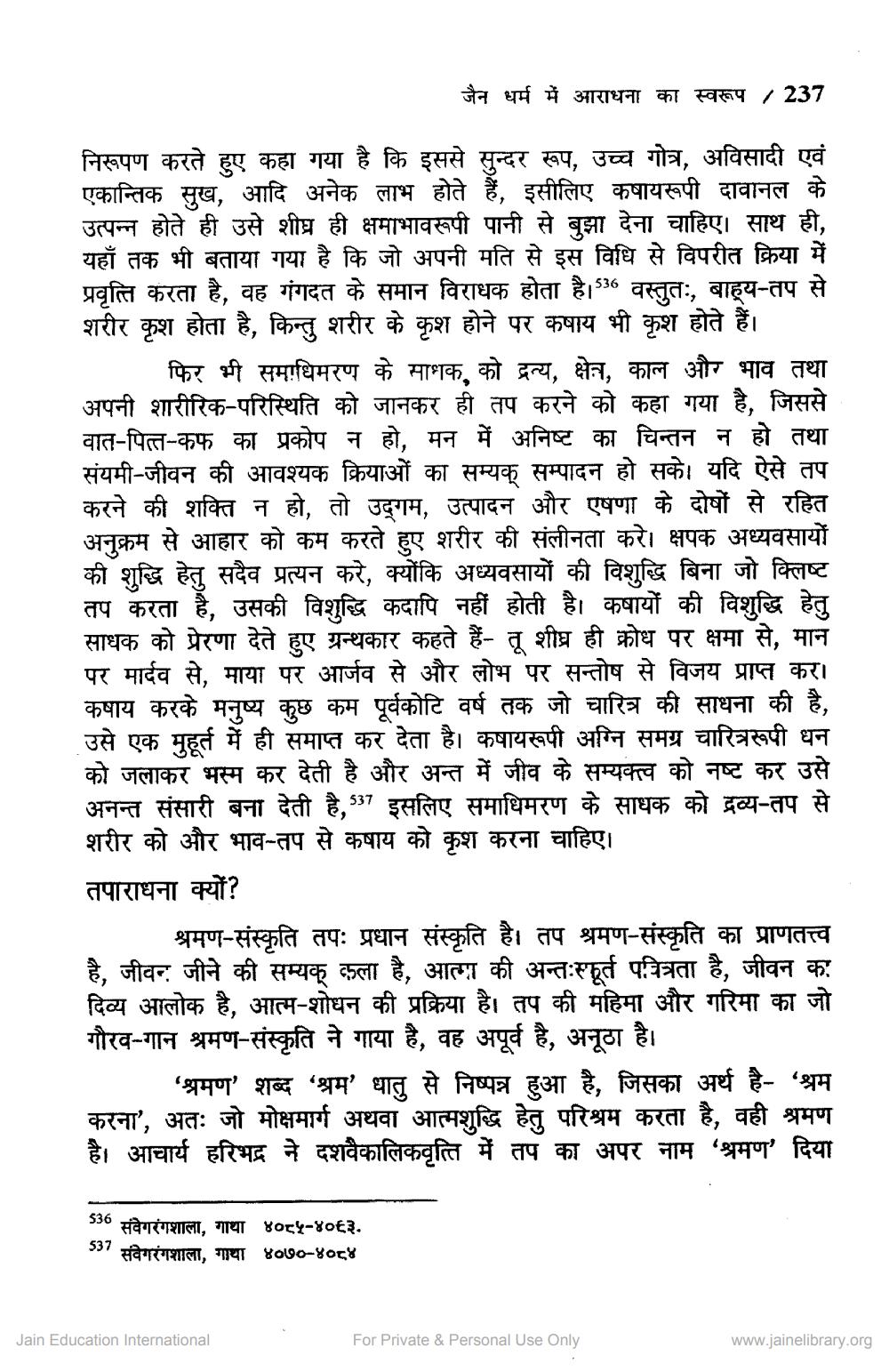________________
जैन धर्म में आराधना का स्वरूप / 237
निरूपण करते हुए कहा गया है कि इससे सुन्दर रूप, उच्च गोत्र, अविसादी एवं एकान्तिक सुख, आदि अनेक लाभ होते हैं, इसीलिए कषायरूपी दावानल के उत्पन्न होते ही उसे शीघ्र ही क्षमाभावरूपी पानी से बुझा देना चाहिए। साथ ही, यहाँ तक भी बताया गया है कि जो अपनी मति से इस विधि से विपरीत क्रिया में प्रवृत्ति करता है, वह गंगदत के समान विराधक होता है। 536 वस्तुतः, बाहूय-तप से शरीर कृश होता है, किन्तु शरीर के कृश होने पर कषाय भी कृश होते हैं।
फिर भी समाधिमरण के साधक, को द्रन्य, क्षेत्र, काल और भाव तथा अपनी शारीरिक परिस्थिति को जानकर ही तप करने को कहा गया है, जिससे वात-पित्त-कफ का प्रकोप न हो, मन में अनिष्ट का चिन्तन न हो तथा संयमी - जीवन की आवश्यक क्रियाओं का सम्यक् सम्पादन हो सके। यदि ऐसे तप करने की शक्ति न हो, तो उद्गम, उत्पादन और एषणा के दोषों से रहित अनुक्रम से आहार को कम करते हुए शरीर की संलीनता करे । क्षपक अध्यवसायों की शुद्धि हेतु सदैव प्रत्यन करे, क्योंकि अध्यवसायों की विशुद्धि बिना जो क्लिष्ट तप करता है, उसकी विशुद्धि कदापि नहीं होती है। कषायों की विशुद्धि हेतु साधक को प्रेरणा देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं- तू शीघ्र ही क्रोध पर क्षमा से, मान पर मार्दव से, माया पर आर्जव से और लोभ पर सन्तोष से विजय प्राप्त कर । कषाय करके मनुष्य कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष तक जो चारित्र की साधना की है, . उसे एक मुहूर्त में ही समाप्त कर देता है। कषायरूपी अग्नि समग्र चारित्ररूपी धन को जलाकर भस्म कर देती है और अन्त में जीव के सम्यक्त्व को नष्ट कर उसे अनन्त संसारी बना देती है, 537 इसलिए समाधिमरण के साधक को द्रव्य-तप से शरीर को और भाव - तप से कषाय को कृश करना चाहिए।
तपाराधना क्यों?
श्रमण-संस्कृति तपः प्रधान संस्कृति है । तप श्रमण संस्कृति का प्राणतत्त्व है, जीवन जीने की सम्यक् कला है, आत्मा की अन्तःस्फूर्त पवित्रता है, जीवन का दिव्य आलोक है, आत्म-शोधन की प्रक्रिया है । तप की महिमा और गरिमा का जो गौरव गान श्रमण- -संस्कृति ने गाया है, वह अपूर्व है, अनूठा है।
'श्रमण' शब्द 'श्रम' धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है- 'श्रम करना', अतः जो मोक्षमार्ग अथवा आत्मशुद्धि हेतु परिश्रम करता है, वही श्रमण है। आचार्य हरिभद्र ने दशवैकालिकवृत्ति में तप का अपर नाम 'श्रमण' दिया
536 संवेगरंगशाला, गाथा ४०८५ - ४०६३.
537
संवेगरंगशाला, गाथा ४०७०-४०८४
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org