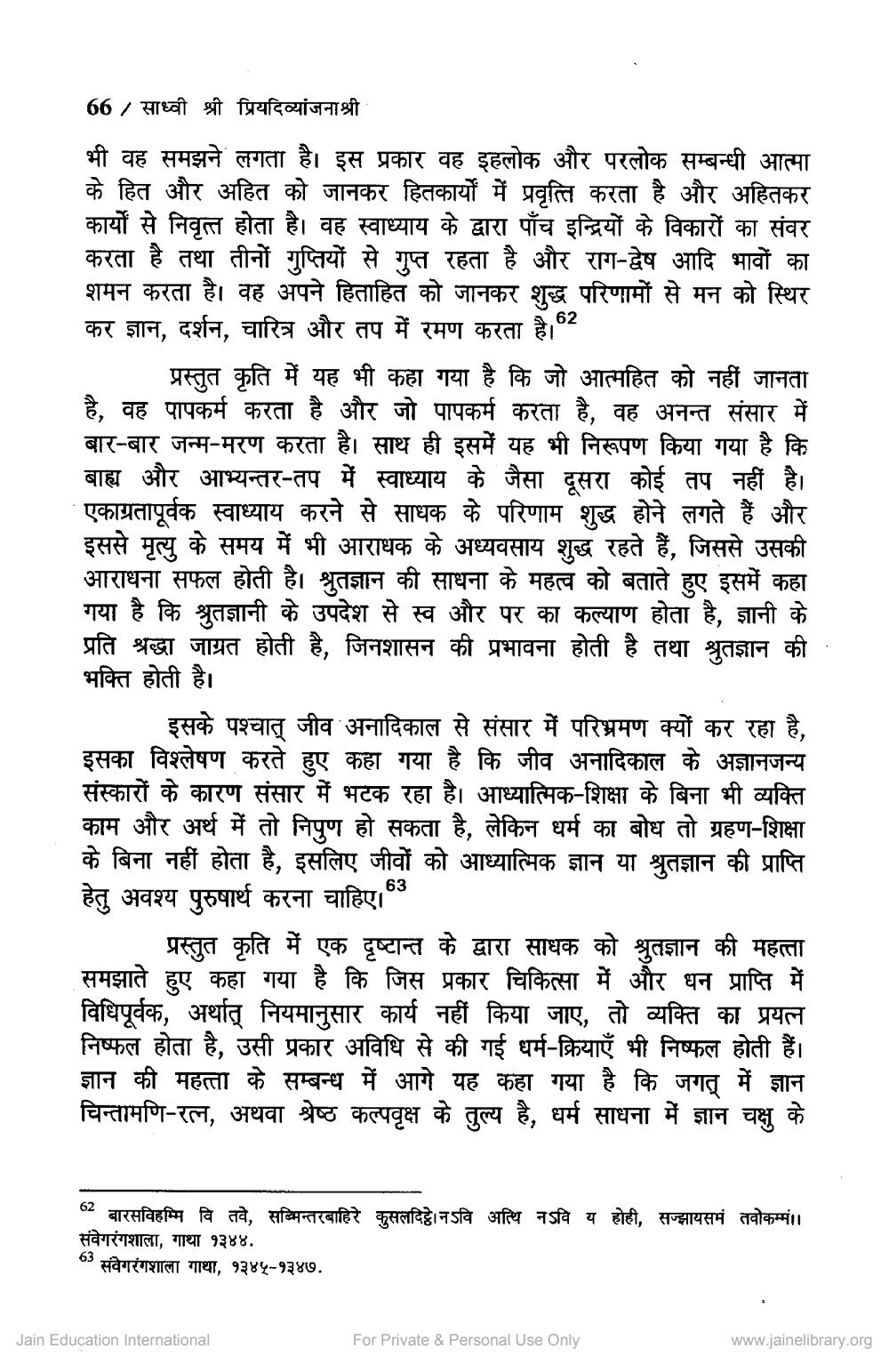________________
66 / साध्वी श्री प्रियदिव्यांजना श्री
भी वह समझने लगता है। इस प्रकार वह इहलोक और परलोक सम्बन्धी आत्मा के हित और अहित को जानकर हितकार्यों में प्रवृत्ति करता है और अहितकर कार्यों से निवृत्त होता है। वह स्वाध्याय के द्वारा पाँच इन्द्रियों के विकारों का संवर करता है तथा तीनों गुप्तियों से गुप्त रहता है और राग-द्वेष आदि भावों का शमन करता है। वह अपने हिताहित को जानकर शुद्ध परिणामों से मन को स्थिर कर ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में रमण करता है। 62
प्रस्तुत कृति में यह भी कहा गया है कि जो आत्महित को नहीं जानता है, वह पापकर्म करता है और जो पापकर्म करता है, वह अनन्त संसार में बार-बार जन्म-मरण करता है। साथ ही इसमें यह भी निरूपण किया गया है कि बाह्य और आभ्यन्तर- तप में स्वाध्याय के जैसा दूसरा कोई तप नहीं है । एकाग्रतापूर्वक स्वाध्याय करने से साधक के परिणाम शुद्ध होने लगते हैं और इससे मृत्यु के समय में भी आराधक के अध्यवसाय शुद्ध रहते हैं, जिससे उसकी आराधना सफल होती है। श्रुतज्ञान की साधना के महत्व को बताते हुए इसमें कहा गया है कि श्रुतज्ञानी के उपदेश से स्व और पर का कल्याण होता है, ज्ञानी के प्रति श्रद्धा जाग्रत होती है, जिनशासन की प्रभावना होती है तथा श्रुतज्ञान की भक्ति होती है।
इसके पश्चात् जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है, इसका विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि जीव अनादिकाल के अज्ञानजन्य संस्कारों के कारण संसार में भटक रहा है। आध्यात्मिक शिक्षा के बिना भी व्यक्ति काम और अर्थ में तो निपुण हो सकता है, लेकिन धर्म का बोध तो ग्रहण-शिक्षा के बिना नहीं होता है, इसलिए जीवों को आध्यात्मिक ज्ञान या श्रुतज्ञान की प्राप्ति हेतु अवश्य पुरुषार्थ करना चाहिए ।
63
प्रस्तुत कृति में एक दृष्टान्त के द्वारा साधक को श्रुतज्ञान की महत्ता समझाते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार चिकित्सा में और धन प्राप्ति में विधिपूर्वक, अर्थात् नियमानुसार कार्य नहीं किया जाए, तो व्यक्ति का प्रयत्न निष्फल होता है, उसी प्रकार अविधि से की गई धर्म - क्रियाएँ भी निष्फल होती हैं। ज्ञान की महत्ता के सम्बन्ध में आगे यह कहा गया है कि जगत् में ज्ञान चिन्तामणि- रत्न, अथवा श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के तुल्य है, धर्म साधना में ज्ञान चक्षु के
62 बारसविहम्मि वि तवे, सब्मिन्तरबाहिरे कुसलदिट्ठे । नऽवि अस्थि नऽवि य होही, सज्झायसमं तवोकम्मं ।। संवेगरंगशाला, गाथा १३४४.
63 संवेगरंगशाला गाथा, १३४५-१३४७.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org