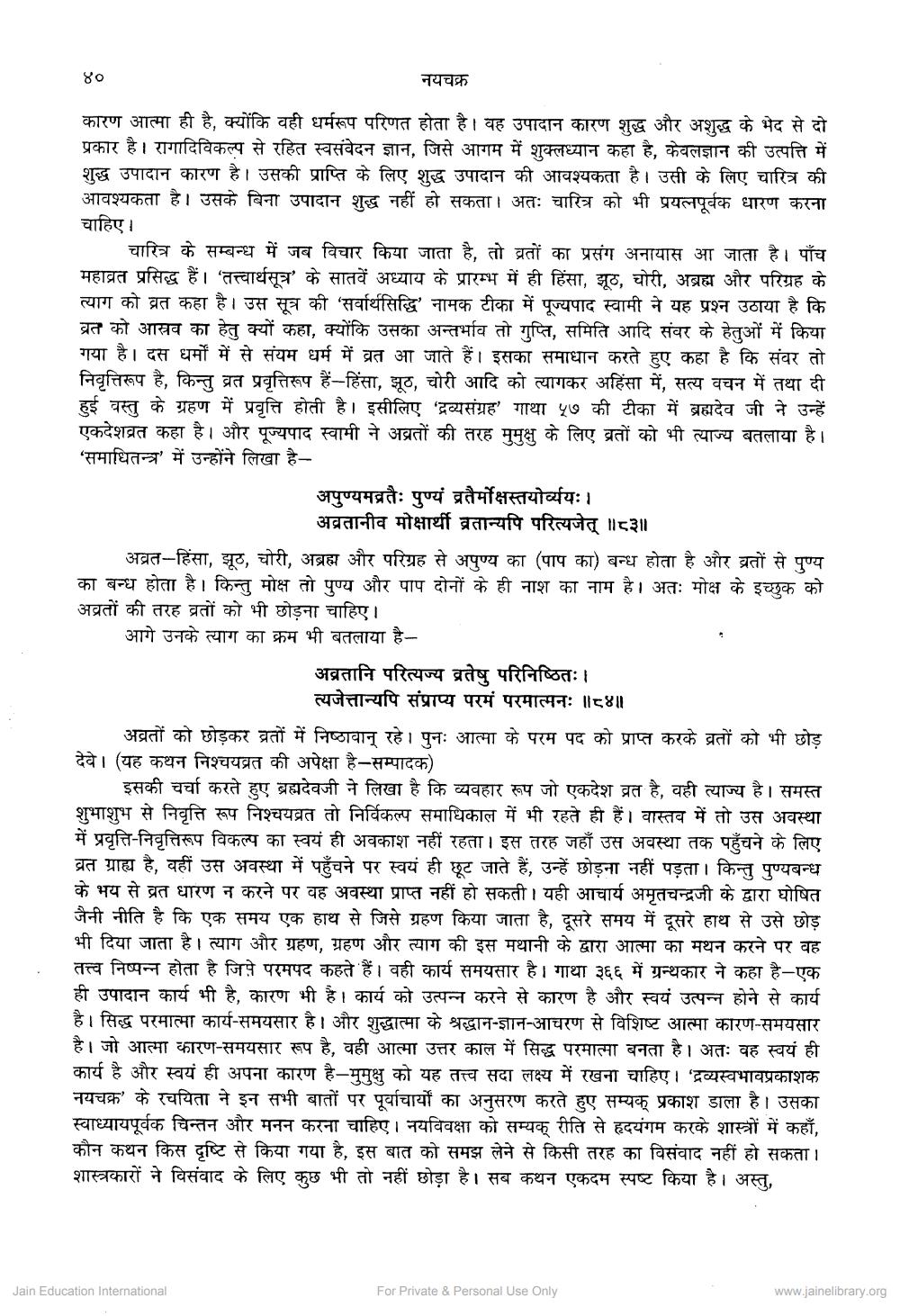________________
४०
नयचक्र
कारण आत्मा ही है, क्योंकि वही धर्मरूप परिणत होता है। वह उपादान कारण शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार है। रागादिविकल्प से रहित स्वसंवेदन ज्ञान, जिसे आगम में शुक्लध्यान कहा है, केवलज्ञान की उत्पत्ति में शुद्ध उपादान कारण है। उसकी प्राप्ति के लिए शुद्ध उपादान की आवश्यकता है। उसी के लिए चारित्र की आवश्यकता है। उसके बिना उपादान शुद्ध नहीं हो सकता। अतः चारित्र को भी प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए।
चारित्र के सम्बन्ध में जब विचार किया जाता है, तो व्रतों का प्रसंग अनायास आ जाता है। पाँच महाव्रत प्रसिद्ध हैं। 'तत्त्वार्थसूत्र' के सातवें अध्याय के प्रारम्भ में ही हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह के त्याग को व्रत कहा है। उस सूत्र की 'सर्वार्थसिद्धि' नामक टीका में पूज्यपाद स्वामी ने यह प्रश्न उठाया है कि व्रत को आस्रव का हेतु क्यों कहा, क्योंकि उसका अन्तर्भाव तो गुप्ति, समिति आदि संवर के हेतुओं में किया गया है। दस धर्मों में से संयम धर्म में व्रत आ जाते हैं। इसका समाधान करते हुए कहा है कि संवर तो निवृत्तिरूप है, किन्तु व्रत प्रवृत्तिरूप हैं-हिंसा, झूठ, चोरी आदि को त्यागकर अहिंसा में, सत्य वचन में तथा दी हुई वस्तु के ग्रहण में प्रवृत्ति होती है। इसीलिए 'द्रव्यसंग्रह' गाथा ५७ की टीका में ब्रह्मदेव जी ने उन्हें एकदेशव्रत कहा है। और पूज्यपाद स्वामी ने अव्रतों की तरह मुमुक्षु के लिए व्रतों को भी त्याज्य बतलाया है। 'समाधितन्त्र' में उन्होंने लिखा है
अपुण्यमव्रतैः पुण्यं व्रतैर्मोक्षस्तयोर्व्ययः। अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि परित्यजेत् ॥५३॥
अव्रत-हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह से अपुण्य का (पाप का) बन्ध होता है और व्रतों से पुण्य का बन्ध होता है। किन्तु मोक्ष तो पुण्य और पाप दोनों के ही नाश का नाम है। अतः मोक्ष के इच्छुक को अव्रतों की तरह व्रतों को भी छोड़ना चाहिए। आगे उनके त्याग का क्रम भी बतलाया है
अव्रतानि परित्यज्य व्रतेष परिनिष्ठितः।
त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य परमं परमात्मनः ॥४॥ अव्रतों को छोड़कर व्रतों में निष्ठावान रहे। पुनः आत्मा के परम पद को प्राप्त करके व्रतों को भी छोड़ देवे। (यह कथन निश्चयव्रत की अपेक्षा है-सम्पादक)
इसकी चर्चा करते हुए ब्रह्मदेवजी ने लिखा है कि व्यवहार रूप जो एकदेश व्रत है, वही त्याज्य है। समस्त शुभाशुभ से निवृत्ति रूप निश्चयव्रत तो निर्विकल्प समाधिकाल में भी रहते ही हैं। वास्तव में तो उस अवस्था
त्तिरूप विकल्प का स्वयं ही अवकाश नहीं रहता। इस तरह जहाँ उस अवस्था तक पहुँचने के लिए व्रत ग्राह्य है, वहीं उस अवस्था में पहुँचने पर स्वयं ही छूट जाते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता। किन्तु पुण्यबन्ध के भय से व्रत धारण न करने पर वह अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। यही आचार्य अमृतचन्द्रजी के द्वारा घोषित जैनी नीति है कि एक समय एक हाथ से जिसे ग्रहण किया जाता है, दूसरे समय में दूसरे हाथ से उसे छोड़ भी दिया जाता है। त्याग और ग्रहण, ग्रहण और त्याग की इस मथानी के द्वारा आत्मा का मथन करने पर वह तत्त्व निष्पन्न होता है जिसे परमपद कहते हैं। वही कार्य समयसार है। गाथा ३६६ में ग्रन्थकार ने कहा है-एक ही उपादान कार्य भी है, कारण भी है। कार्य को उत्पन्न करने से कारण है और स्वयं उत्पन्न होने से कार्य है। सिद्ध परमात्मा कार्य-समयसार है। और शुद्धात्मा के श्रद्धान-ज्ञान-आचरण से विशिष्ट आत्मा कारण-समयसार है। जो आत्मा कारण-समयसार रूप है, वही आत्मा उत्तर काल में सिद्ध परमात्मा बनता है। अतः वह स्वयं ही कार्य है और स्वयं ही अपना कारण है-मुमुक्षु को यह तत्त्व सदा लक्ष्य में रखना चाहिए। 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' के रचयिता ने इन सभी बातों पर पूर्वाचार्यों का अनुसरण करते हुए सम्यक् प्रकाश डाला है। उसका स्वाध्यायपूर्वक चिन्तन और मनन करना चाहिए। नयविवक्षा को सम्यक् रीति से हृदयंगम करके शास्त्रों में कहाँ, कौन कथन किस दृष्टि से किया गया है, इस बात को समझ लेने से किसी तरह का विसंवाद नहीं हो सकता। शास्त्रकारों ने विसंवाद के लिए कुछ भी तो नहीं छोड़ा है। सब कथन एकदम स्पष्ट किया है। अस्तु,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org