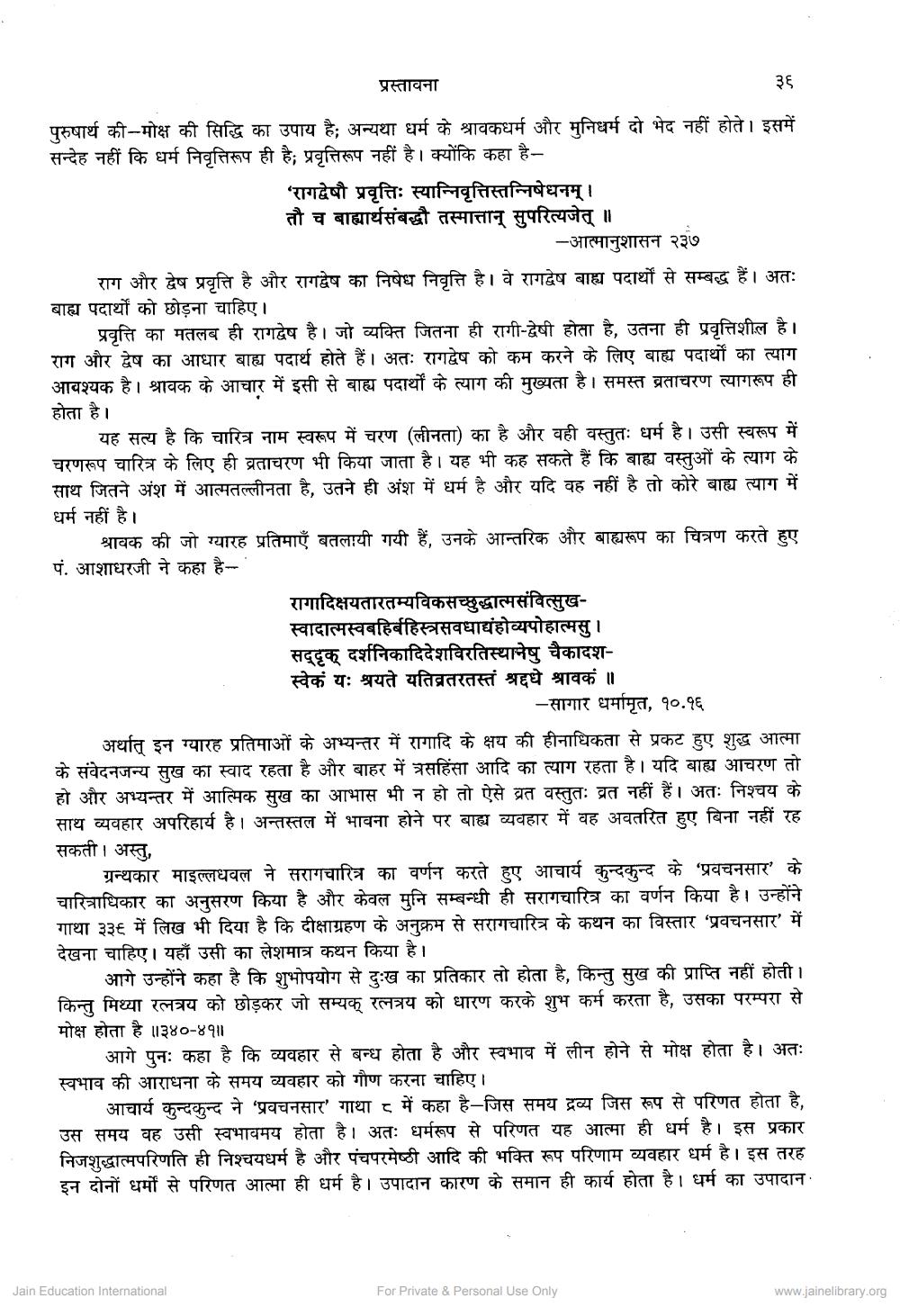________________
प्रस्तावना
३६
पुरुषार्थ की-मोक्ष की सिद्धि का उपाय है; अन्यथा धर्म के श्रावकधर्म और मुनिधर्म दो भेद नहीं होते। इसमें सन्देह नहीं कि धर्म निवृत्तिरूप ही है; प्रवृत्तिरूप नहीं है। क्योंकि कहा है
'रागद्वेषौ प्रवृत्तिः स्यान्निवृत्तिस्तन्निषेधनम्। तौ च बाह्यार्थसंबद्धौ तस्मात्तान् सुपरित्यजेत् ॥
-आत्मानुशासन २३७ राग और द्वेष प्रवृत्ति है और रागद्वेष का निषेध निवृत्ति है। वे रागद्वेष बाह्य पदार्थों से सम्बद्ध हैं। अतः बाह्य पदार्थों को छोड़ना चाहिए।
प्रवृत्ति का मतलब ही रागद्वेष है। जो व्यक्ति जितना ही रागी-द्वेषी होता है, उतना ही प्रवृत्तिशील है। राग और द्वेष का आधार बाह्य पदार्थ होते हैं। अतः रागद्वेष को कम करने के लिए बाह्य पदार्थों का त्याग आवश्यक है। श्रावक के आचार में इसी से बाह्य पदार्थों के त्याग की मुख्यता है। समस्त व्रताचरण त्यागरूप ही होता है।
यह सत्य है कि चारित्र नाम स्वरूप में चरण (लीनता) का है और वही वस्तुतः धर्म है। उसी स्वरूप में चरणरूप चारित्र के लिए ही व्रताचरण भी किया जाता है। यह भी कह सकते हैं कि बाह्य वस्तुओं के त्याग के साथ जितने अंश में आत्मतल्लीनता है, उतने ही अंश में धर्म है और यदि वह नहीं है तो कोरे बाह्य त्याग में धर्म नहीं है।
श्रावक की जो ग्यारह प्रतिमाएँ बतलायी गयी हैं, उनके आन्तरिक और बाह्यरूप का चित्रण करते हए पं. आशाधरजी ने कहा है
रागादिक्षयतारतम्यविकसच्छुद्धात्मसंवित्सुखस्वादात्मस्वबहिर्बहिस्त्रसवधायहोव्यपोहात्मसु । सदुदक दर्शनिकादिदेशविरतिस्थानेष चैकादशस्वेकं यः श्रयते यतिव्रतरतस्तं श्रद्दधे श्रावकं ॥
-सागार धर्मामृत, १०.१६ अर्थात इन ग्यारह प्रतिमाओं के अभ्यन्तर में रागादि के क्षय की हीनाधिकता से प्रकट हए शद्ध आत्मा के संवेदनजन्य सुख का स्वाद रहता है और बाहर में त्रसहिंसा आदि का त्याग रहता है। यदि बाह्य आचरण तो हो और अभ्यन्तर में आत्मिक सुख का आभास भी न हो तो ऐसे व्रत वस्तुतः व्रत नहीं हैं। अतः निश्चय के साथ व्यवहार अपरिहार्य है। अन्तस्तल में भावना होने पर बाह्य व्यवहार में वह अवतरित हुए बिना नहीं रह सकती। अस्तु,
ग्रन्थकार माइल्लधवल ने सरागचारित्र का वर्णन करते हुए आचार्य कुन्दकुन्द के 'प्रवचनसार' के चारित्राधिकार का अनुसरण किया है और केवल मुनि सम्बन्धी ही सरागचारित्र का वर्णन किया है। उन्होंने गाथा ३३६ में लिख भी दिया है कि दीक्षाग्रहण के अनुक्रम से सरागचारित्र के कथन का विस्तार 'प्रवचनसार' में देखना चाहिए। यहाँ उसी का लेशमात्र कथन किया है।।
आगे उन्होंने कहा है कि शुभोपयोग से दुःख का प्रतिकार तो होता है, किन्तु सुख की प्राप्ति नहीं होती। किन्तु मिथ्या रत्नत्रय को छोड़कर जो सम्यक् रत्नत्रय को धारण करके शुभ कर्म करता है, उसका परम्परा से मोक्ष होता है ॥३४०-४१॥
आगे पुनः कहा है कि व्यवहार से बन्ध होता है और स्वभाव में लीन होने से मोक्ष होता है। अतः स्वभाव की आराधना के समय व्यवहार को गौण करना चाहिए।
आचार्य कुन्दकुन्द ने 'प्रवचनसार' गाथा ८ में कहा है-जिस समय द्रव्य जिस रूप से परिणत होता है, उस समय वह उसी स्वभावमय होता है। अतः धर्मरूप से परिणत यह आत्मा ही धर्म है। इस प्रकार निजशुद्धात्मपरिणति ही निश्चयधर्म है और पंचपरमेष्ठी आदि की भक्ति रूप परिणाम व्यवहार धर्म है। इस तरह इन दोनों धर्मों से परिणत आत्मा ही धर्म है। उपादान कारण के समान ही कार्य होता है। धर्म का उपादान
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org