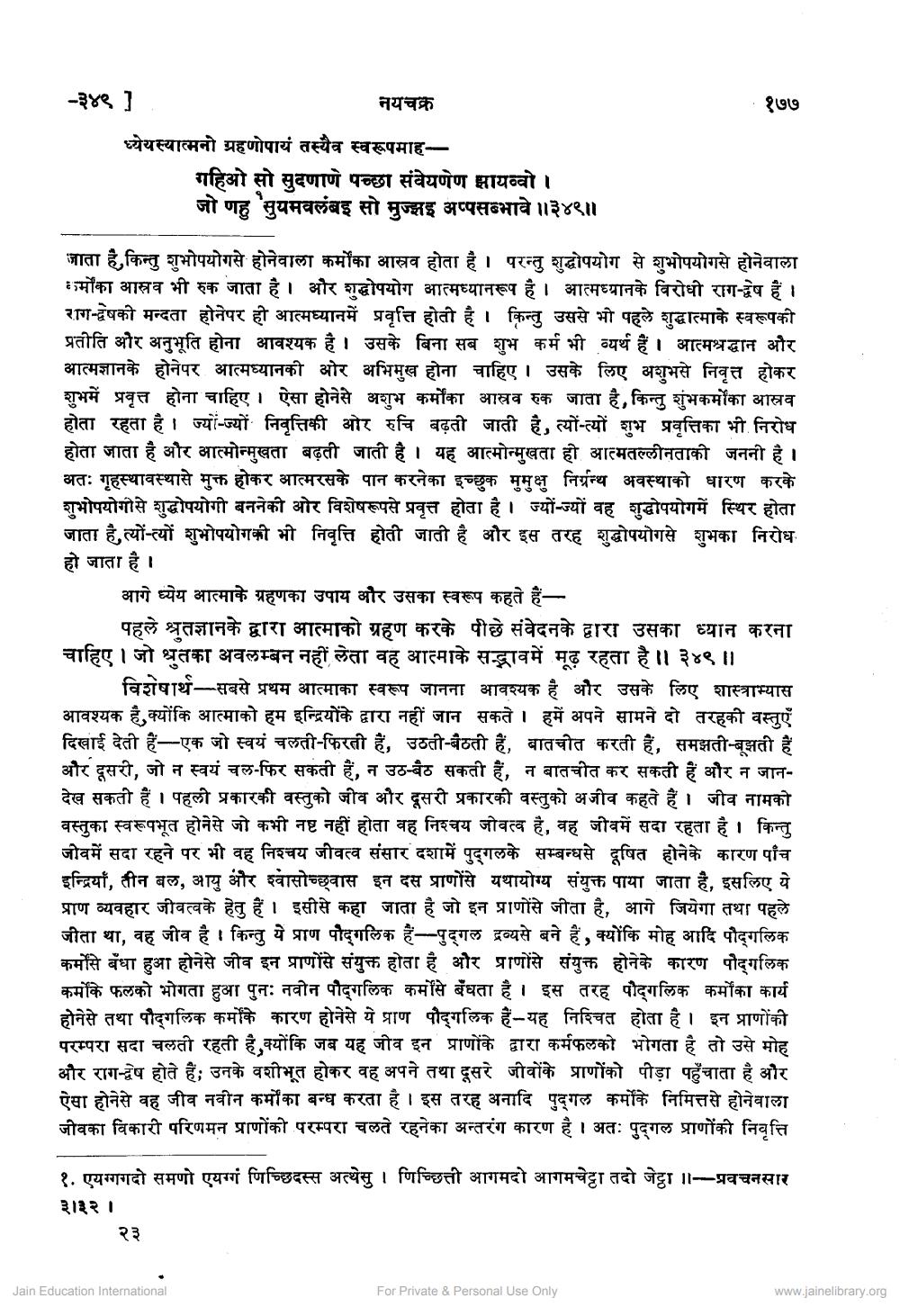________________
-३४९ ] .
नयचक्र
.१७७
ध्येयस्यात्मनो ग्रहणोपायं तस्यैव स्वरूपमाह
गहिओ सो सुदणाणे पच्छा संवेयणेण झायव्वो। जो णहु 'सुयमवलंबइ सो मुज्झइ अप्पसब्भावे ॥३४९॥
जाता है, किन्तु शुभोपयोगसे होनेवाला कर्मोंका आस्रव होता है। परन्तु शुद्धोपयोग से शुभोपयोगसे होनेवाला कर्मोंका आस्रव भी रुक जाता है। और शुद्धोपयोग आत्मध्यानरूप है। आत्मध्यानके विरोधी राग-द्वेष हैं । राग-द्वेषको मन्दता होनेपर हो आत्मध्यानमें प्रवृत्ति होती है। किन्तु उससे भी पहले शुद्धात्माके स्वरूपकी प्रतीति और अनुभूति होना आवश्यक है। उसके बिना सब शुभ कर्म भी व्यर्थ हैं। आत्मश्रद्धान और आत्मज्ञानके होनेपर आत्मध्यानकी ओर अभिमुख होना चाहिए। उसके लिए अशुभसे निवृत्त होकर शुभमें प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा होनेसे अशुभ कर्मोका आस्रव रुक जाता है, किन्तु शुभकर्मोका आस्रव होता रहता है। ज्यों-ज्यों निवृत्तिकी ओर रुचि बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों शुभ प्रवृत्तिका भी निरोध होता जाता है और आत्मोन्मुखता बढ़ती जाती है। यह आत्मोन्मुखता ही आत्मतल्लीनताकी जननी है । अतः गृहस्थावस्थासे मुक्त होकर आत्मरसके पान करनेका इच्छुक मुमुक्षु निर्ग्रन्थ अवस्थाको धारण करके शुभोपयोगीसे शुद्धोपयोगी बननेकी ओर विशेषरूपसे प्रवृत्त होता है। ज्यों-ज्यों वह शुद्धोपयोगमें स्थिर होता जाता है,त्यों-त्यों शुभोपयोगकी भी निवृत्ति होती जाती है और इस तरह शुद्धोपयोगसे शुभका निरोध हो जाता है।
आगे ध्येय आत्माके ग्रहणका उपाय और उसका स्वरूप कहते हैं
पहले श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माको ग्रहण करके पीछे संवेदनके द्वारा उसका ध्यान करना चाहिए । जो श्रुतका अवलम्बन नहीं लेता वह आत्माके सद्भावमें मूढ रहता है ।। ३४९ ॥
विशेषार्थ-सबसे प्रथम आत्माका स्वरूप जानना आवश्यक है और उसके लिए शास्त्राभ्यास आवश्यक है, क्योंकि आत्माको हम इन्द्रियोंके द्वारा नहीं जान सकते । हमें अपने सामने दो तरहकी वस्तुएँ दिखाई देती हैं-एक जो स्वयं चलती-फिरती हैं, उठती-बैठती हैं, बातचीत करती हैं, समझती-बूझती हैं और दूसरी, जो न स्वयं चल-फिर सकती हैं, न उठ-बैठ सकती हैं, न बातचीत कर सकती हैं और न जानदेख सकती हैं । पहली प्रकारकी वस्तुको जीव और दूसरी प्रकारको वस्तुको अजीव कहते हैं। जीव नामको वस्तुका स्वरूपभूत होनेसे जो कभी नष्ट नहीं होता वह निश्चय जोवत्व है, वह जीवमें सदा रहता है। किन्तु जीवमें सदा रहने पर भी वह निश्चय जीवत्व संसार दशामें पुद्गलके सम्बन्धसे दूषित होनेके कारण पाँच इन्द्रियाँ, तीन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास इन दस प्राणोंसे यथायोग्य संयुक्त पाया जाता है, इसलिए ये प्राण व्यवहार जीवत्वके हेतु हैं । इसीसे कहा जाता है जो इन प्राणोंसे जीता है, आगे जियेगा तथा पहले जीता था, वह जीव है। किन्तु ये प्राण पोद्गलिक हैं-पुद्गल द्रव्यसे बने हैं, क्योंकि मोह आदि पौद्गलिक कर्मोसे बंधा हुआ होनेसे जीव इन प्राणोंसे संयुक्त होता है और प्राणोंसे संयुक्त होनेके कारण पौद्गलिक कर्मोके फलको भोगता हुआ पुनः नवीन पौद्गलिक कर्मोसे बंधता है। इस तरह पौद्गलिक कर्मोका कार्य होनेसे तथा पौदगलिक कर्मोंके कारण होनेसे ये प्राण पौद्गलिक हैं-यह निश्चित होता है। इन प्राणोंकी परम्परा सदा चलती रहती है,क्योंकि जब यह जीव इन प्राणोंके द्वारा कर्मफलको भोगता है तो उसे मोह और राग-द्वेष होते हैं। उनके वशीभूत होकर वह अपने तथा दूसरे जीवोंके प्राणोंको पीड़ा पहुँचाता है और ऐसा होनेसे वह जीव नवीन कर्मों का बन्ध करता है । इस तरह अनादि पुद्गल कर्मोके निमित्तसे होनेवाला जीवका विकारी परिणमन प्राणोंको परम्परा चलते रहनेका अन्तरंग कारण है। अतः पुद्गल प्राणोंकी निवत्ति
१. एयग्गगदो समणो एयग्गं णिच्छिदस्स अत्थेसु । णिच्छित्ती आगमदो आगमचेट्टा तदो जेट्ठा ॥-प्रवचनसार ३।३२।
२३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org