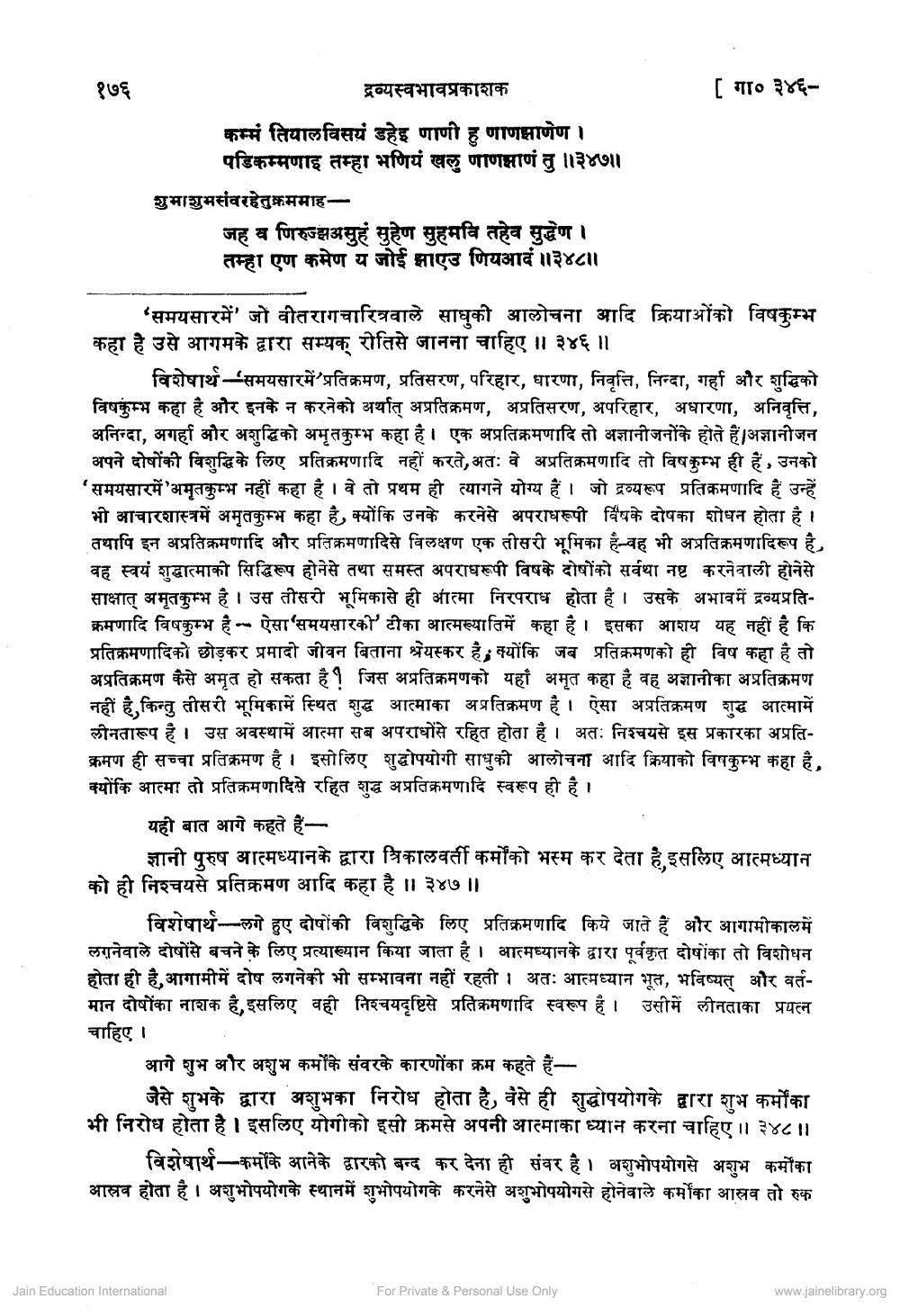________________
१७६
द्रव्यस्वभावप्रकाशक
कम्मं तियालविस डहेइ णाणी ह णाणझाणेण । पडिकम्मणाइ तम्हा भणियं खलु णाणझाणं तु ॥३४७॥ शुभाशुभसंवर हेतु क्रममाह-
जह व णिरुज्झअसुहं सुहेण सुहमवि तहेव सुद्धेण । तम्हा एण कमेण य जोई झाएउ णियआदं ॥ ३४८ ॥
'समयसारमें' जो वीतरागचारित्रवाले साधुकी आलोचना आदि क्रियाओंको विषकुम्भ कहा है उसे आगम द्वारा सम्यक् रोतिसे जानना चाहिए || ३४६ ॥
[ गा० ३४६
विशेषार्थ समयसार में 'प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा गर्हा और शुद्धिको विषकुम्भ कहा है और इनके न करनेको अर्थात् अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिन्दा, अगर्हा और अशुद्धिको अमृतकुम्भ कहा है। एक अप्रतिक्रमणादि तो अज्ञानीजनोंके होते हैं। अज्ञानीजन अपने दोषोंकी विशुद्धि के लिए प्रतिक्रमणादि नहीं करते, अतः वे अप्रतिक्रमणादि तो विषकुम्भ ही हैं, उनको 'समयसारमें 'अमृतकुम्भ नहीं कहा है । वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य हैं । जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि हैं उन्हें भी आचारशास्त्र में अमृतकुम्भ कहा है, क्योंकि उनके करनेसे अपराधरूपी विषके दोषका शोधन होता है । तथापि इन अप्रतिक्रमणादि और प्रतिक्रमणादिसे विलक्षण एक तीसरी भूमिका है वह भी अप्रतिक्रमणादिरूप है, वह स्वयं शुद्धात्माको सिद्धिरूप होनेसे तथा समस्त अपराधरूपी विषके दोषोंको सर्वथा नष्ट करनेवाली होने से साक्षात् अमृतकुम्भ है । उस तीसरी भूमिकासे ही आत्मा निरपराध होता है । उसके अभाव में द्रव्यप्रतिक्रमणादि विषकुम्भ है ऐसा 'समयसार की' टीका आत्मख्यातिमें कहा है । इसका आशय यह नहीं है कि प्रतिक्रमणादिको छोड़कर प्रमादी जीवन बिताना श्रेयस्कर है; क्योंकि जब प्रतिक्रमणको ही विष कहा है तो अप्रतिक्रमण कैसे अमृत हो सकता है ? जिस अप्रतिक्रमणको यहाँ अमृत कहा है वह अज्ञानीका अप्रतिक्रमण नहीं है, किन्तु तीसरी भूमिका में स्थित शुद्ध आत्माका अप्रतिक्रमण है । ऐसा अप्रतिक्रमण शुद्ध आत्मा लीनतारूप है । उस अवस्थामें आत्मा सब अपराधोंसे रहित होता है । अतः निश्चयसे इस प्रकारका अप्रतिक्रमण ही सच्चा प्रतिक्रमण है । इसीलिए शुद्धोपयोगी साधुकी आलोचना आदि क्रियाको विषकुम्भ कहा है, क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादिसे रहित शुद्ध अप्रतिक्रमणादि स्वरूप ही है ।
--
यही बात आगे कहते हैं
ज्ञानी पुरुष आत्मध्यानके द्वारा त्रिकालवर्ती कर्मोंको भस्म कर देता है, इसलिए आत्मध्यान को ही निश्चय प्रतिक्रमण आदि कहा है ।। ३४७ ॥
विशेषार्थ - लगे हुए दोषोंकी विशुद्धिके लिए प्रतिक्रमणादि किये जाते हैं और आगामीकालमें लग़नेवाले दोषोंसे बचने के लिए प्रत्याख्यान किया जाता है । आत्मध्यानके द्वारा पूर्वकृत दोषोंका तो विशोधन होता ही है, आगामी में दोष लगनेकी भी सम्भावना नहीं रहती । अतः आत्मध्यान भूत, भविष्यत् और वर्तमान दोषों का नाशक है, इसलिए वही निश्चयदृष्टिसे प्रतिक्रमणादि स्वरूप है । उसी में लीनताका प्रयत्न चाहिए ।
आगे शुभ और अशुभ कर्मोंके संवरके कारणोंका क्रम कहते हैं
जैसे शुभके द्वारा अशुभका निरोध होता है, वैसे ही शुद्धोपयोग के द्वारा शुभ कर्मोंका भी निरोध होता है । इसलिए योगीको इसी क्रमसे अपनी आत्माका ध्यान करना चाहिए ॥ ३४८ ॥
विशेषार्थ - कर्मोंके आनेके द्वारको बन्द कर देना ही संवर है। अशुभोपयोगसे अशुभ कर्मोका आस्रव होता है । अशुभोपयोगके स्थान में शुभोपयोगके करनेसे अशुभोपयोगसे होनेवाले कर्मोंका आस्रव तो रुक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org