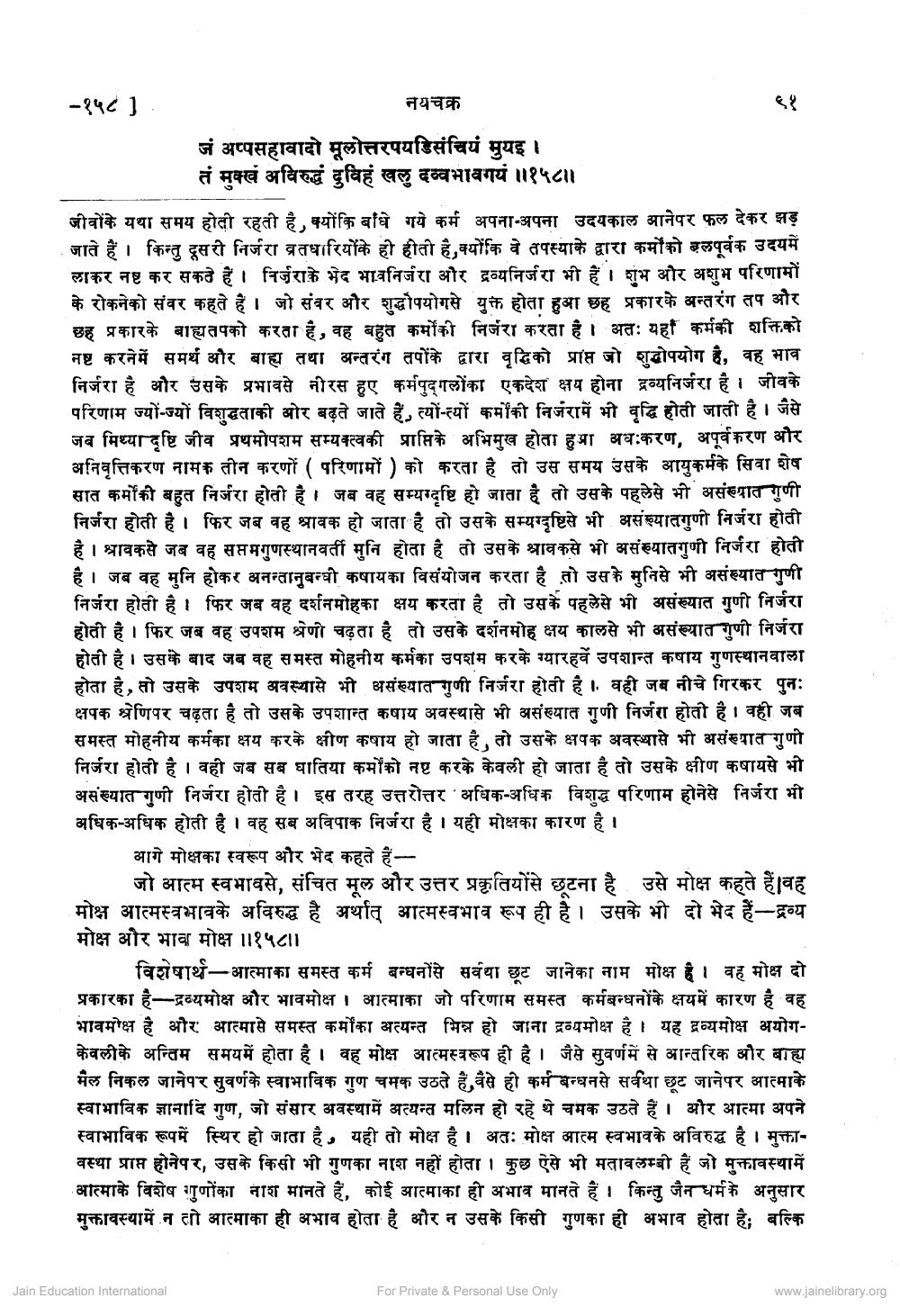________________
-१५८ ]
नयचक्र
९१
जं अप्पसहावादो मूलोत्तरपयडिसंचियं मुयइ । तं मुक्खं अविरुद्धं दुविहं खलु दव्वभावगयं ॥१५८॥
जीवोंके यथा समय होती रहती है, क्योंकि बांधे गये कर्म अपना-अपना उदयकाल आनेपर फल देकर झड़ जाते हैं। किन्तु दूसरी निर्जरा व्रतधारियोंके ही होती है,क्योंकि वे तपस्याके द्वारा कर्मोको बलपूर्वक उदयमें लाकर नष्ट कर सकते हैं। निर्जराके भेद भावनिर्जरा और द्रव्यनिर्जरा भी हैं। शुभ और अशुभ परिणामों के रोकनेको संवर कहते हैं । जो संवर और शुद्धोपयोगसे युक्त होता हुआ छह प्रकारके अन्तरंग तप और छह प्रकारके बाह्यतपको करता है, वह बहुत कर्मोकी निर्जरा करता है। अतः यहाँ कर्मकी शक्तिको नष्ट करने में समर्थ और बाह्य तथा अन्तरंग तपोंके द्वारा वृद्धिको प्राप्त जो शुद्धोपयोग है, वह भाव निर्जरा है और उसके प्रभावसे नीरस हए कर्मपदगलोंका एकदेश क्षय होना द्रव्यनिर्जरा है। जीवके परिणाम ज्यों-ज्यों विशुद्धताकी ओर बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों कर्मोंकी निर्जरामें भी वृद्धि होती जाती है । जैसे जब मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्तिके अभिमुख होता हा अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामक तीन करणों ( परिणामों ) को करता है तो उस समय उसके आयुकर्मके सिवा शेष सात कर्मों की बहुत निर्जरा होती है। जब वह सम्यग्दष्टि हो जाता है तो उसके पहलेसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। फिर जब वह श्रावक हो जाता है तो उसके सम्यग्दृष्टिसे भी असंख्यातगुणी निर्जरा होती है । श्रावकसे जब वह सप्तमगुणस्थानवर्ती मुनि होता है तो उसके श्रावकसे भी असंख्यातगुणी निर्जरा होती है। जब वह मुनि होकर अनन्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन करता है तो उसके मुनिसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। फिर जब वह दर्शनमोहका क्षय करता है तो उसके पहलेसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है । फिर जब वह उपशम श्रेणी चढ़ता है तो उसके दर्शनमोह क्षय कालसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है । उसके बाद जब वह समस्त मोहनीय कर्मका उपशम करके ग्यारहवें उपशान्त कषाय गुणस्थानवाला होता है, तो उसके उपशम अवस्थासे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। वही जब नीचे गिरकर पुनः क्षपक श्रेणिपर चढ़ता है तो उसके उपशान्त कषाय अवस्थासे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। वही जब समस्त मोहनीय कर्मका क्षय करके क्षीण कषाय हो जाता है, तो उसके क्षपक अवस्थासे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है । वही जब सब घातिया कोको नष्ट करके केवली हो जाता है तो उसके क्षीण कषायसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इस तरह उत्तरोत्तर अधिक-अधिक विशद्ध परिणाम होनेसे निर्जरा भी अधिक-अधिक होती है। वह सब अविपाक निर्जरा है । यही मोक्षका कारण है।
आगे मोक्षका स्वरूप और भेद कहते हैं
जो आत्म स्वभावसे, संचित मूल और उत्तर प्रकृतियोंसे छुटना है उसे मोक्ष कहते हैं।वह मोक्ष आत्मस्वभावके अविरुद्ध है अर्थात् आत्मस्वभाव रूप ही है। उसके भी दो भेद हैं-द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष ॥१५८|
विशेषार्थ-आत्माका समस्त कर्म बन्धनोंसे सर्वथा छूट जानेका नाम मोक्ष है। वह मोक्ष दो प्रकारका है-द्रव्यमोक्ष और भावमोक्ष । आत्माका जो परिणाम समस्त कर्मबन्धनोंके क्षयमें कारण है वह भावमोक्ष है और आत्मासे समस्त कर्मों का अत्यन्त भिन्न हो जाना द्रव्यमोक्ष है। यह द्रव्यमोक्ष अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें होता है। वह मोक्ष आत्मस्वरूप ही है। जैसे सुवर्णमें से आन्तरिक और बाह्य मैल निकल जानेपर सुवर्णके स्वाभाविक गुण चमक उठते हैं, वैसे ही कर्मबन्धनसे सर्वथा छुट जानेपर आत्माके स्वाभाविक ज्ञानादि गुण, जो संसार अवस्थामें अत्यन्त मलिन हो रहे थे चमक उठते हैं। और आत्मा अपने स्वाभाविक रूपमें स्थिर हो जाता है, यही तो मोक्ष है। अतः मोक्ष आत्म स्वभावके अविरुद्ध है । मुक्तावस्था प्राप्त होनेपर, उसके किसी भी गुणका नाश नहीं होता। कुछ ऐसे भी मतावलम्बी हैं जो मुक्तावस्था में आत्माके विशेष गुणोंका नाश मानते हैं, कोई आत्माका ही अभाव मानते हैं। किन्तु जैन धर्मके अनुसार मुक्तावस्थामें न तो आत्माका ही अभाव होता है और न उसके किसी गुणका ही अभाव होता है, बल्कि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org