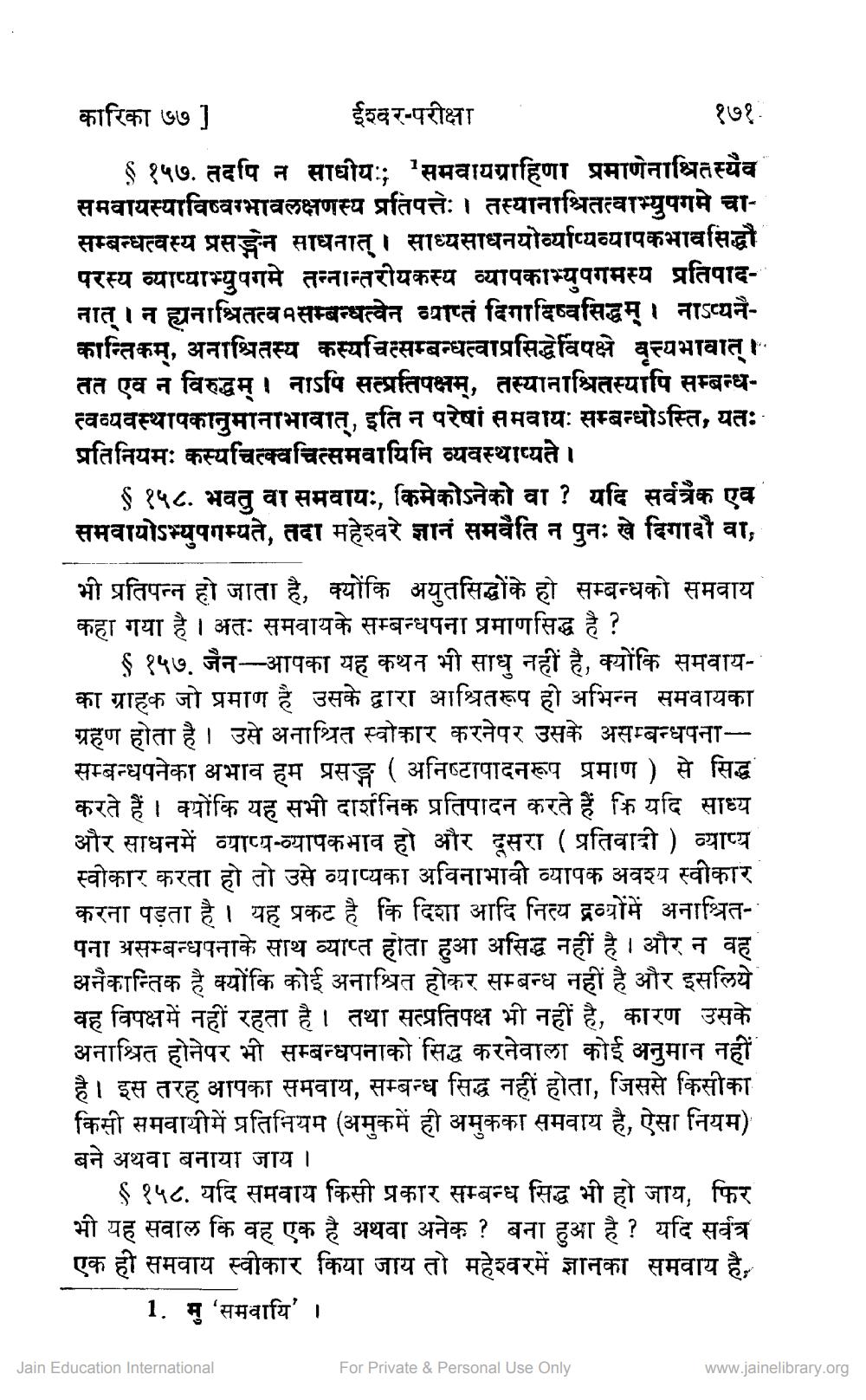________________
कारिका ७७] ईश्वर-परीक्षा
१७१. $ १५७. तदपि न साधीयः; 'समवायग्राहिणा प्रमाणेनाश्रितस्यैव समवायस्याविष्वग्भावलक्षणस्य प्रतिपत्तेः। तस्यानाश्रितत्वाभ्युपगमे चासम्बन्धत्वस्य प्रसङ्न साधनात्। साध्यसाधनयोाप्यव्यापकभावसिद्धौ परस्य व्याप्याभ्युपगमे तन्नान्तरीयकस्य व्यापकाभ्युपगमस्य प्रतिपादनात् । न ह्यनाश्रितत्वमसम्बन्धत्वेन व्याप्तं दिगादिष्वसिद्धम् । नाऽप्यनैकान्तिकम्, अनाश्रितस्य कस्यचित्सम्बन्धत्वाप्रसिद्धविपक्षे वृत्त्यभावात्। तत एव न विरुद्धम । नाऽपि सत्प्रतिपक्षम, तस्यानाश्रितस्यापि सम्बन्धत्वव्यवस्थापकानुमानाभावात्, इति न परेषां समवायः सम्बन्धोऽस्ति, यतः प्रतिनियमः कस्यचित्क्वचित्समवायिनि व्यवस्थाप्यते।
$ १५८. भवतु वा समवायः, किमेकोऽनेको वा ? यदि सर्वत्रैक एव समवायोऽभ्युपगम्यते, तदा महेश्वरे ज्ञानं समवेति न पुनः खे दिगादी वा,
भी प्रतिपन्न हो जाता है, क्योंकि अयुतसिद्धोंके हो सम्बन्धको समवाय कहा गया है । अतः समवायके सम्बन्धपना प्रमाण सिद्ध है ?
१५७. जैन-आपका यह कथन भी साधु नहीं है, क्योंकि समवायका ग्राहक जो प्रमाण है उसके द्वारा आश्रितरूप हो अभिन्न समवायका ग्रहण होता है। उसे अनाथित स्वोकार करनेपर उसके असम्बन्धपनासम्बन्धपनेका अभाव हम प्रसङ्ग ( अनिष्टापादनरूप प्रमाण ) से सिद्ध करते हैं। क्योंकि यह सभी दार्शनिक प्रतिपादन करते हैं कि यदि साध्य और साधनमें व्याप्य-व्यापकभाव हो और दूसरा ( प्रतिवादी ) व्याप्य स्वीकार करता हो तो उसे व्याप्यका अविनाभावी व्यापक अवश्य स्वीकार करना पड़ता है। यह प्रकट है कि दिशा आदि नित्य द्रव्योंमें अनाश्रितपना असम्बन्धपनाके साथ व्याप्त होता हुआ असिद्ध नहीं है । और न वह अनेकान्तिक है क्योंकि कोई अनाश्रित होकर सम्बन्ध नहीं है और इसलिये वह विपक्ष में नहीं रहता है। तथा सत्प्रतिपक्ष भी नहीं है, कारण उसके अनाश्रित होनेपर भी सम्बन्धपनाको सिद्ध करनेवाला कोई अनुमान नहीं है। इस तरह आपका समवाय, सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता, जिससे किसीका किसी समवायीमें प्रतिनियम (अमुकमें ही अमुकका समवाय है, ऐसा नियम) बने अथवा बनाया जाय।।
$ १५८. यदि समवाय किसी प्रकार सम्बन्ध सिद्ध भी हो जाय, फिर भी यह सवाल कि वह एक है अथवा अनेक ? बना हुआ है ? यदि सर्वत्र एक ही समवाय स्वीकार किया जाय तो महेश्वरमें ज्ञानका समवाय है,
1. मु 'समवायि' ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org