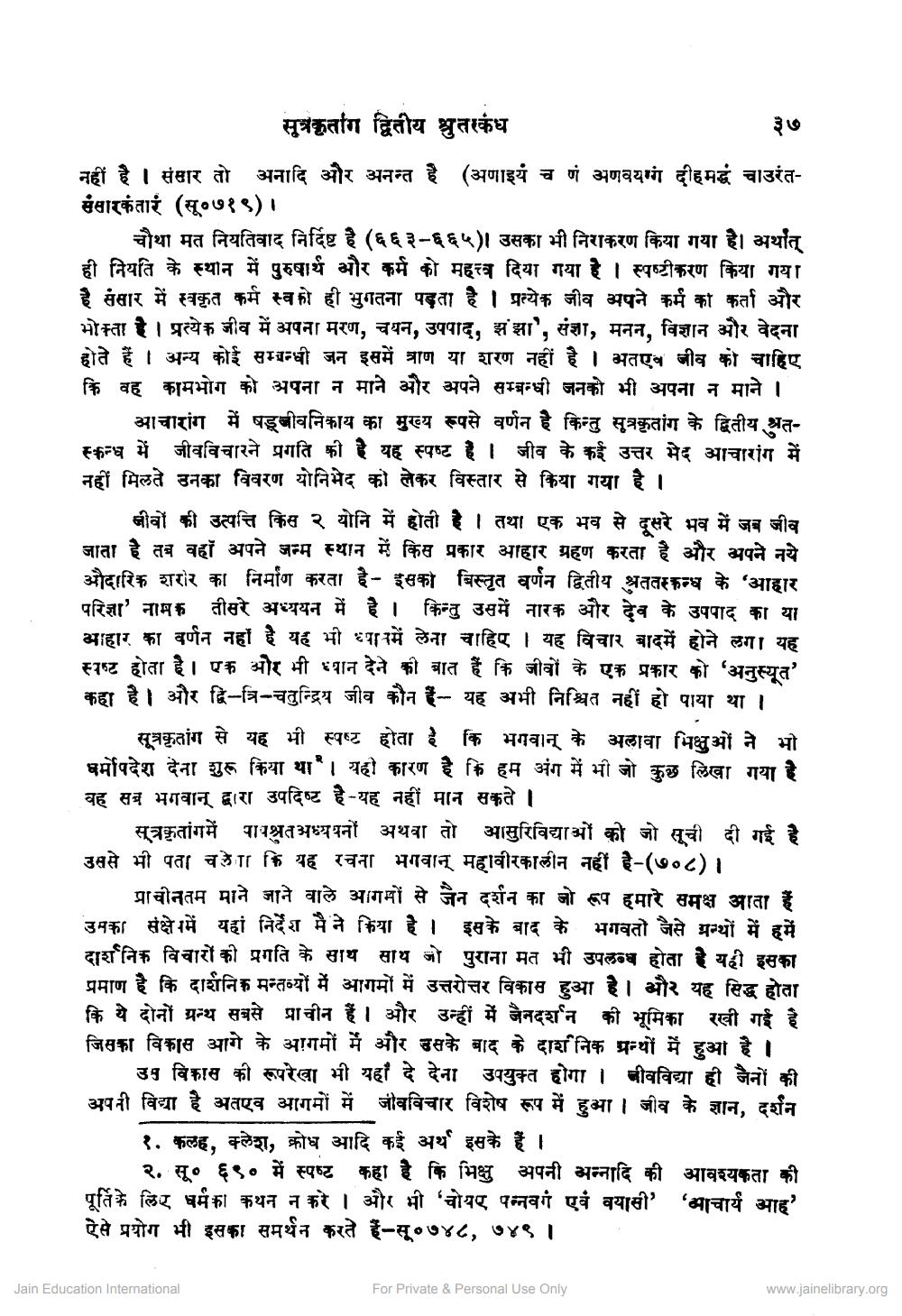________________
सूत्रकृतांग द्वितीय श्रुतस्कंध नहीं है । संसार तो अनादि और अनन्त है (अणाइयं च णं अणवयाग दीहमद्धं चाउरतसंसारकंतारं (सू०७१९)।
चौथा मत नियतिवाद निर्दिष्ट है (६६३-६६५)। उसका भी निराकरण किया गया है। अर्थात् ही नियति के स्थान में पुरुषार्थ और कर्म को महत्त्व दिया गया है । स्पष्टीकरण किया गया है संसार में स्वकृत कर्म स्वको ही भुगतना पड़ता है । प्रत्येक जीव अपने कर्म का कर्ता और भोक्ता है। प्रत्येक जीव में अपना मरण, चयन, उपपाद, झंझा', संज्ञा, मनन, विज्ञान और वेदना होते हैं । अन्य कोई सम्बन्धी जन इसमें त्राण या शरण नहीं है । अतएव जीव को चाहिए कि वह कामभोग को अपना न माने और अपने सम्बन्धी जनको भी अपना न माने ।
आचारांग में षड्जीवनिकाय का मुख्य रूपसे वर्णन है किन्तु सूत्रकृतांग के द्वितीय श्रतस्कन्ध में जीवविचारने प्रगति की है यह स्पष्ट है । जीव के कई उत्तर भेद आचारांग में नहीं मिलते उनका विवरण योनिभेद को लेकर विस्तार से किया गया है ।
जीवों की उत्पत्ति किस २ योनि में होती है । तथा एक भव से दूसरे भव में जब जीव जाता है तब वहाँ अपने जन्म स्थान में किस प्रकार आहार ग्रहण करता है और अपने नये
औदारिक शरीर का निर्माण करता है- इसको बिस्तृत वर्णन द्वितीय श्रुततस्कन्ध के 'आहार परिज्ञा' नामक तीसरे अध्ययन में है। किन्तु उसमें नारक और देव के उपपाद का या आहार का वर्णन नहीं है यह भी ध्यानमें लेना चाहिए । यह विचार बादमें होने लगा यह स्पष्ट होता है। एक और भी ध्यान देने की बात हैं कि जीवों के एक प्रकार को 'अनुस्यूत' कहा है। और द्वि-त्रि-चतुन्द्रिय जीव कौन है- यह अभी निश्चित नहीं हो पाया था ।
सूत्रकृतांग से यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान् के अलावा भिक्षुओं ने भो धर्मोपदेश देना शुरू किया था। यही कारण है कि हम अंग में भी जो कुछ लिखा गया है वह सब भगवान् द्वारा उपदिष्ट है-यह नहीं मान सकते ।
सूत्रकृतांगमें पापश्रुतअध्ययनों अथवा तो आसुरिविद्याओं को जो सूची दी गई है उससे भी पता चलेगा कि यह रचना भगवान् महावीरकालीन नहीं है-(७०८)।
प्राचीनतम माने जाने वाले आगमों से जैन दर्शन का जो रूप हमारे समक्ष आता है उमका संक्षेपमें यहां निर्देश मै ने किया है । इसके बाद के भगवतो जैसे ग्रन्थों में हमें दार्शनिक विचारों की प्रगति के साथ साथ जो पुराना मत भी उपलब्ध होता है यही इसका प्रमाण है कि दार्शनिक मन्तव्यों में आगमों में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। और यह सिद्ध होता कि ये दोनों ग्रन्थ सबसे प्राचीन हैं। और उन्हीं में जैनदर्शन की भूमिका रखी गई है जिसका विकास आगे के आगमों में और उसके बाद के दार्शनिक प्रन्थों में हुआ है।
उस विकास की रूपरेखा भी यहाँ दे देना उपयुक्त होगा। नीवविद्या ही जैनों की अपनी विद्या है अतएव आगमों में जीवविचार विशेष रूप में हुआ। जीव के ज्ञान, दर्शन
१. कलह, क्लेश, क्रोध आदि कई अर्थ इसके हैं।
२. सू० ६९० में स्पष्ट कहा है कि भिक्षु अपनी अन्नादि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए धर्मका कथन न करे । और भी 'चोयए पन्नवगं एवं वयासी' 'आचार्य आहे' ऐसे प्रयोग भी इसका समर्थन करते हैं-सू०७४८, ७४९ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org