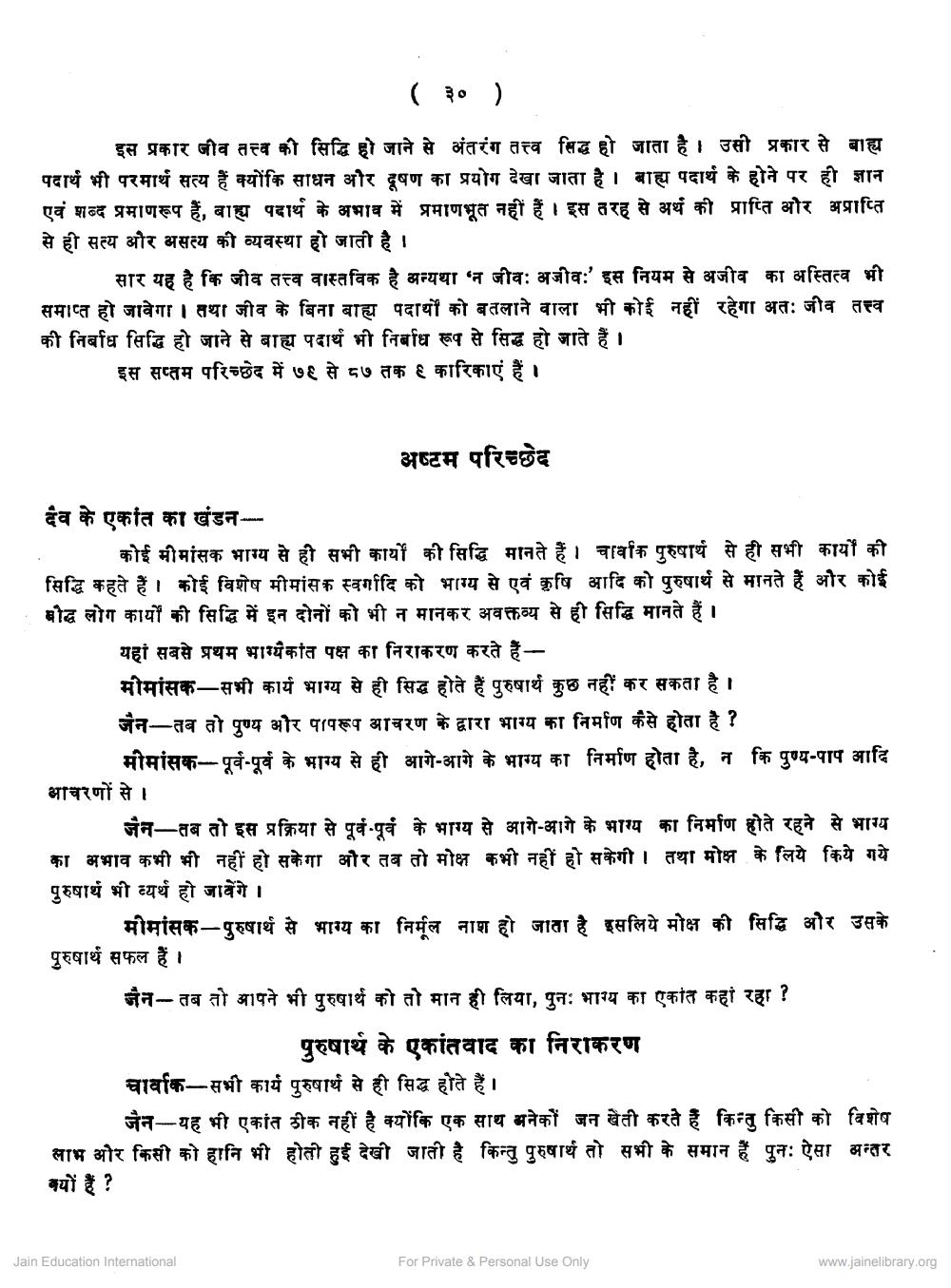________________
इस प्रकार जीव तत्त्व की सिद्धि हो जाने से अंतरंग तत्त्व सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से बाह्य पदार्थ भी परमार्थ सत्य हैं क्योंकि साधन और दूषण का प्रयोग देखा जाता है। बाह्य पदार्थ के होने पर ही ज्ञान एवं शब्द प्रमाणरूप हैं, बाह्य पदार्थ के अभाव में प्रमाणभूत नहीं हैं । इस तरह से अर्थ की प्राप्ति और अप्राप्ति से ही सत्य और असत्य की व्यवस्था हो जाती है ।
सार यह है कि जीव तत्त्व वास्तविक है अन्यथा 'न जीवः अजीवः' इस नियम से अजीव का अस्तित्व भी समाप्त हो जावेगा। तथा जीव के बिना बाह्य पदार्थों को बतलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा अतः जीव तत्त्व की निर्बाध सिद्धि हो जाने से बाह्य पदार्थ भी निर्बाध रूप से सिद्ध हो जाते हैं ।
इस सप्तम परिच्छेद में ७९ से ८७ तक कारिकाएं हैं।
अष्टम परिच्छेद
देव के एकांत का खंडन--
कोई मीमांसक भाग्य से ही सभी कार्यों की सिद्धि मानते हैं। चार्वाक पुरुषार्थ से ही सभी कार्यों की सिद्धि कहते हैं। कोई विशेष मीमांसक स्वर्गादि को भाग्य से एवं कृषि आदि को पुरुषार्थ से मानते हैं और कोई - बौद्ध लोग कार्यों की सिद्धि में इन दोनों को भी न मानकर अवक्तव्य से ही सिद्धि मानते हैं।
यहां सबसे प्रथम भाग्यकांत पक्ष का निराकरण करते हैंमीमांसक-सभी कार्य भाग्य से ही सिद्ध होते हैं पुरुषार्थ कुछ नहीं कर सकता है। जैन-तब तो पुण्य और पापरूप आचरण के द्वारा भाग्य का निर्माण कैसे होता है ?
मीमांसक-पूर्व-पूर्व के भाग्य से ही आगे-आगे के भाग्य का निर्माण होता है, न कि पुण्य-पाप आदि आचरणों से ।
जैन-तब तो इस प्रक्रिया से पूर्व-पूर्व के भाग्य से आगे-आगे के भाग्य का निर्माण होते रहने से भाग्य का अभाव कभी भी नहीं हो सकेगा और तब तो मोक्ष कभी नहीं हो सकेगी। तथा मोक्ष के लिये किये गये पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जावेंगे।
मीमांसक-पुरुषार्थ से भाग्य का निर्मूल नाश हो जाता है इसलिये मोक्ष की सिद्धि और उसके पुरुषार्थ सफल हैं। जैन- तब तो आपने भी पुरुषार्थ को तो मान ही लिया, पुनः भाग्य का एकांत कहां रहा ?
पुरुषार्थ के एकांतवाद का निराकरण चार्वाक-सभी कार्य पुरुषार्थ से ही सिद्ध होते हैं।
जैन-यह भी एकांत ठीक नहीं है क्योंकि एक साथ अनेकों जन खेती करते हैं किन्तु किसी को विशेष लाभ और किसी को हानि भी होती हुई देखी जाती है किन्तु पुरुषार्थ तो सभी के समान हैं पुनः ऐसा अन्तर क्यों हैं ?
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org