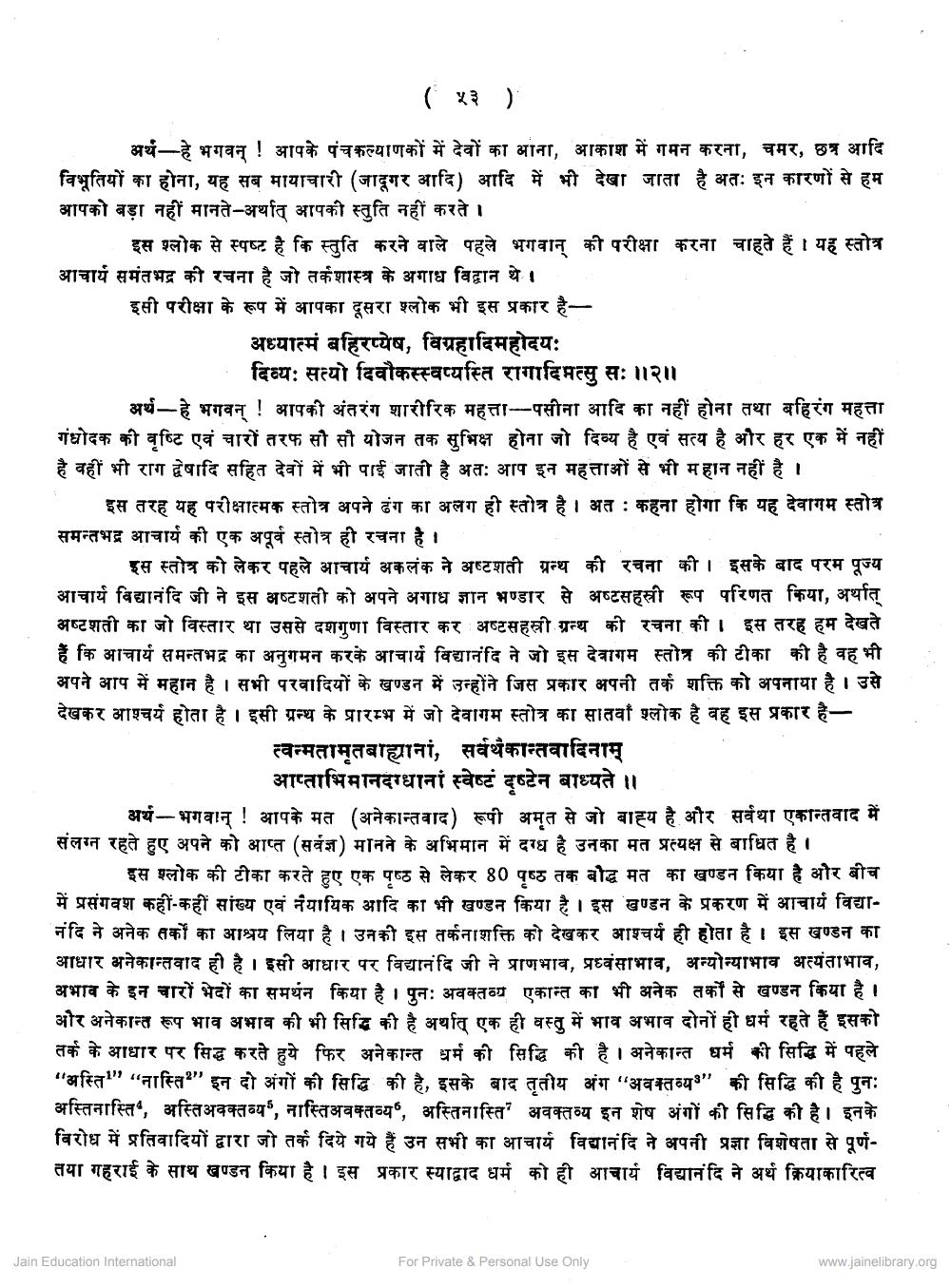________________
( ५३ )
अर्थ - हे भगवन् ! आपके पंचकल्याणकों में देवों का आना, आकाश में गमन करना, चमर, छत्र आदि विभूतियों का होना, यह सब मायाचारी ( जादूगर आदि ) आदि में भी देखा जाता है अतः इन कारणों से हम आपको बड़ा नहीं मानते - अर्थात् आपकी स्तुति नहीं करते ।
इस श्लोक से स्पष्ट है कि स्तुति करने वाले पहले भगवान् की परीक्षा करना चाहते हैं । यह स्तोत्र आचार्य समंतभद्र की रचना है जो तर्कशास्त्र के अगाध विद्वान थे ।
इसी परीक्षा के
रूप में आपका दूसरा श्लोक भी इस प्रकार है
अध्यात्मं बहिरव्येष, विग्रहादिमहोदयः
for: सत्यो दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ॥ २ ॥
अर्थ - हे भगवन् ! आपकी अंतरंग शारीरिक महत्ता - पसीना आदि का नहीं होना तथा बहिरंग महत्ता गंधोदक की वृष्टि एवं चारों तरफ सौ सौ योजन तक सुभिक्ष होना जो दिव्य है एवं सत्य है और हर एक में नहीं है वहीं भी राग द्वेषादि सहित देवों में भी पाई जाती है अतः आप इन महत्ताओं से भी महान नहीं है ।
इस तरह यह परीक्षात्मक स्तोत्र अपने ढंग का अलग ही स्तोत्र है । अत: कहना होगा कि यह देवागम स्तोत्र समन्तभद्र आचार्य की एक अपूर्व स्तोत्र ही रचना है ।
इस स्तोत्र को लेकर पहले आचार्य अकलंक ने अष्टशती ग्रन्थ की रचना की। इसके बाद परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी ने इस अष्टशती को अपने अगाध ज्ञान भण्डार से अष्टसहस्री रूप परिणत किया, अर्थात् अष्टशती का जो विस्तार था उससे दशगुणा विस्तार कर अष्टसहस्री ग्रन्थ की रचना की। इस तरह हम देखते हैं कि आचार्य समन्तभद्र का अनुगमन करके आचार्य विद्यानंदि ने जो इस देवागम स्तोत्र की टीका की है वह भी अपने आप में महान है । सभी परवादियों के खण्डन में उन्होंने जिस प्रकार अपनी तर्क शक्ति को अपनाया है । उसे देखकर आश्चर्य होता है । इसी ग्रन्थ के प्रारम्भ में जो देवागम स्तोत्र का सातवाँ श्लोक है वह इस प्रकार हैत्वन्मतामृतबाह्यानां सर्वथैकान्तवादिनाम् आप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते ॥
अर्थ - भगवान् ! आपके मत ( अनेकान्तवाद) रूपी अमृत से जो बाह्य है और सर्वथा एकान्तवाद में संलग्न रहते हुए अपने को आप्त (सर्वज्ञ) मानने के अभिमान में दग्ध है उनका मत प्रत्यक्ष से बाधित है ।
Jain Education International
इस श्लोक की टीका करते हुए एक पृष्ठ से लेकर 80 पृष्ठ तक बौद्ध मत का खण्डन किया है और बीच में प्रसंगवश कहीं-कहीं सांख्य एवं नैयायिक आदि का भी खण्डन किया । इस खण्डन के प्रकरण में आचार्य विद्याfara का आश्रय लिया है। उनकी इस तर्कनाशक्ति को देखकर आश्चर्य ही होता है । इस खण्डन का आधार अनेकान्तवाद ही है। इसी आधार पर विद्यानंद जी ने प्राणभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव अत्यंताभाव, अभाव के इन चारों भेदों का समर्थन किया है । पुनः अवक्तव्य एकान्त का भी अनेक तर्कों से खण्डन किया है । और अनेकान्त रूप भाव अभाव की भी सिद्धि की है अर्थात् एक ही वस्तु में भाव अभाव दोनों ही धर्म रहते हैं इसको तर्क के आधार पर सिद्ध करते हुये फिर अनेकान्त धर्म की सिद्धि की है । अनेकान्त धर्म की सिद्धि में पहले "अस्ति" "नास्ति" इन दो अंगों की सिद्धि की है, इसके बाद तृतीय अंग "अवक्तव्य" की सिद्धि की है पुनः अस्ति नास्ति', अस्तिअवक्तव्य', नास्तिअवक्तव्य', अस्तिनास्ति' अवक्तव्य इन शेष अंगों की सिद्धि की है। इनके विरोध में प्रतिवादियों द्वारा जो तर्क दिये गये हैं उन सभी का आचार्य विद्यानंदि ने अपनी प्रज्ञा विशेषता से पूर्णतथा गहराई के साथ खण्डन किया है । इस प्रकार स्याद्वाद धर्म को ही आचार्य विद्यानंदि ने अर्थ क्रियाकारित्व
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org