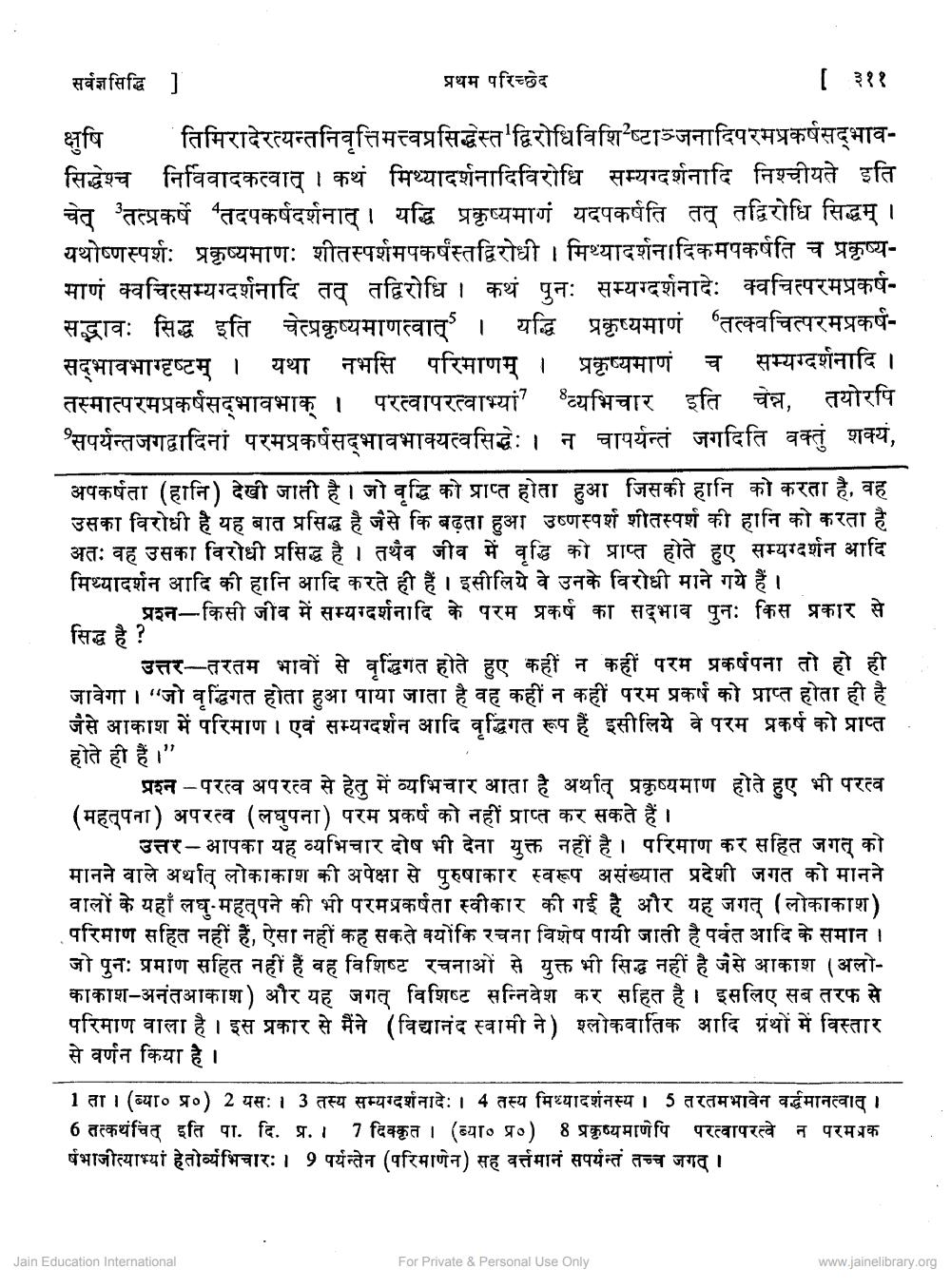________________
सर्वज्ञसिद्धि ] प्रथम परिच्छेद
[ ३११ क्षुषि तिमिरादेरत्यन्तनिवृत्तिमत्त्वप्रसिद्धस्त'विरोधिविशिष्टाञ्जनादिपरमप्रकर्षसद्भावसिद्धेश्च निर्विवादकत्वात् । कथं मिथ्यादर्शनादिविरोधि सम्यग्दर्शनादि निश्चीयते इति चेत् तत्प्रकर्षे तदपकर्षदर्शनात् । यद्धि प्रकृष्यमाणं यदपकर्षति तत् तद्विरोधि सिद्धम् । यथोष्णस्पर्शः प्रकृष्यमाणः शीतस्पर्शमपकर्षस्तद्विरोधी । मिथ्यादर्शनादिकमपकर्षति च प्रकृष्यमाणं क्वचित्सम्यग्दर्शनादि तत् तद्विरोधि । कथं पुनः सम्यग्दर्शनादेः क्वचित्परमप्रकर्षसद्भावः सिद्ध इति चेत्प्रकृष्यमाणत्वात् । यद्धि प्रकृष्यमाणं तत्क्वचित्परमप्रकर्षसद्भावभाग्दृष्टम् । यथा नभसि परिमाणम् । प्रकृष्यमाणं च सम्यग्दर्शनादि । तस्मात्परमप्रकर्षसद्भावभाक् । परत्वापरत्वाभ्यां' व्यभिचार इति चेन्न, तयोरपि 'सपर्यन्तजगद्वादिनां परमप्रकर्षसद्भावभाक्यत्वसिद्धेः । न चापर्यन्तं जगदिति वक्तुं शक्यं, अपकर्षता (हानि) देखी जाती है। जो वृद्धि को प्राप्त होता हुआ जिसकी हानि को करता है, वह उसका विरोधी है यह बात प्रसिद्ध है जैसे कि बढ़ता हुआ उष्णस्पर्श शीतस्पर्श की हानि को करता है अतः वह उसका विरोधी प्रसिद्ध है । तथैव जीव में वृद्धि को प्राप्त होते हुए सम्यग्दर्शन आदि मिथ्यादर्शन आदि की हानि आदि करते ही हैं। इसीलिये वे उनके विरोधी माने गये हैं।
. प्रश्न-किसी जीव में सम्यग्दर्शनादि के परम प्रकर्ष का सद्भाव पुनः किस प्रकार से सिद्ध है ?
उत्तर-तरतम भावों से वृद्धिंगत होते हुए कहीं न कहीं परम प्रकर्षपना तो हो ही जावेगा। "जो वृद्धिंगत होता हुआ पाया जाता है वह कहीं न कहीं परम प्रकर्ष को प्राप्त होता ही है जैसे आकाश में परिमाण । एवं सम्यग्दर्शन आदि वृद्धिंगत रूप हैं इसीलिये वे परम प्रकर्ष को प्राप्त . होते ही हैं।"
प्रश्न -परत्व अपरत्व से हेतु में व्यभिचार आता है अर्थात् प्रकृष्यमाण होते हुए भी परत्व (महत्पना) अपरत्व (लघुपना) परम प्रकर्ष को नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर- आपका यह व्यभिचार दोष भी देना युक्त नहीं है। परिमाण कर सहित जगत् को मानने वाले अर्थात् लोकाकाश की अपेक्षा से पुरुषाकार स्वरूप असंख्यात प्रदेशी जगत को मानने वालों के यहाँ लघु-महत्पने की भी परमप्रकर्षता स्वीकार की गई है और यह जगत् (लोकाकाश) परिमाण सहित नहीं हैं, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि रचना विशेष पायी जाती है पर्वत आदि के समान । जो पुनः प्रमाण सहित नहीं हैं वह विशिष्ट रचनाओं से युक्त भी सिद्ध नहीं है जैसे आकाश (अलोकाकाश-अनंतआकाश) और यह जगत विशिष्ट सन्निवेश कर सहित है। इसलिए सब तरफ से परिमाण वाला है। इस प्रकार से मैंने (विद्यानंद स्वामी ने) श्लोकवातिक आदि ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया है।
1 ता । (ब्या० प्र०) 2 यसः। 3 तस्य सम्यग्दर्शनादेः। 4 तस्य मिथ्यादर्शनस्य। 5 तरतमभावेन वर्द्धमानत्वात् । 6 तत्कथंचित् इति पा. दि. प्र.। 7 दिक्कृत । (ब्या० प्र०) 8 प्रकृष्यमाणेपि परत्वापरत्वे न परमप्रक र्षभाजीत्याभ्यां हेतोर्व्यभिचारः। 9 पर्यन्तेन (परिमाणेन) सह वर्तमान सपर्यन्तं तच्च जगत् ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org