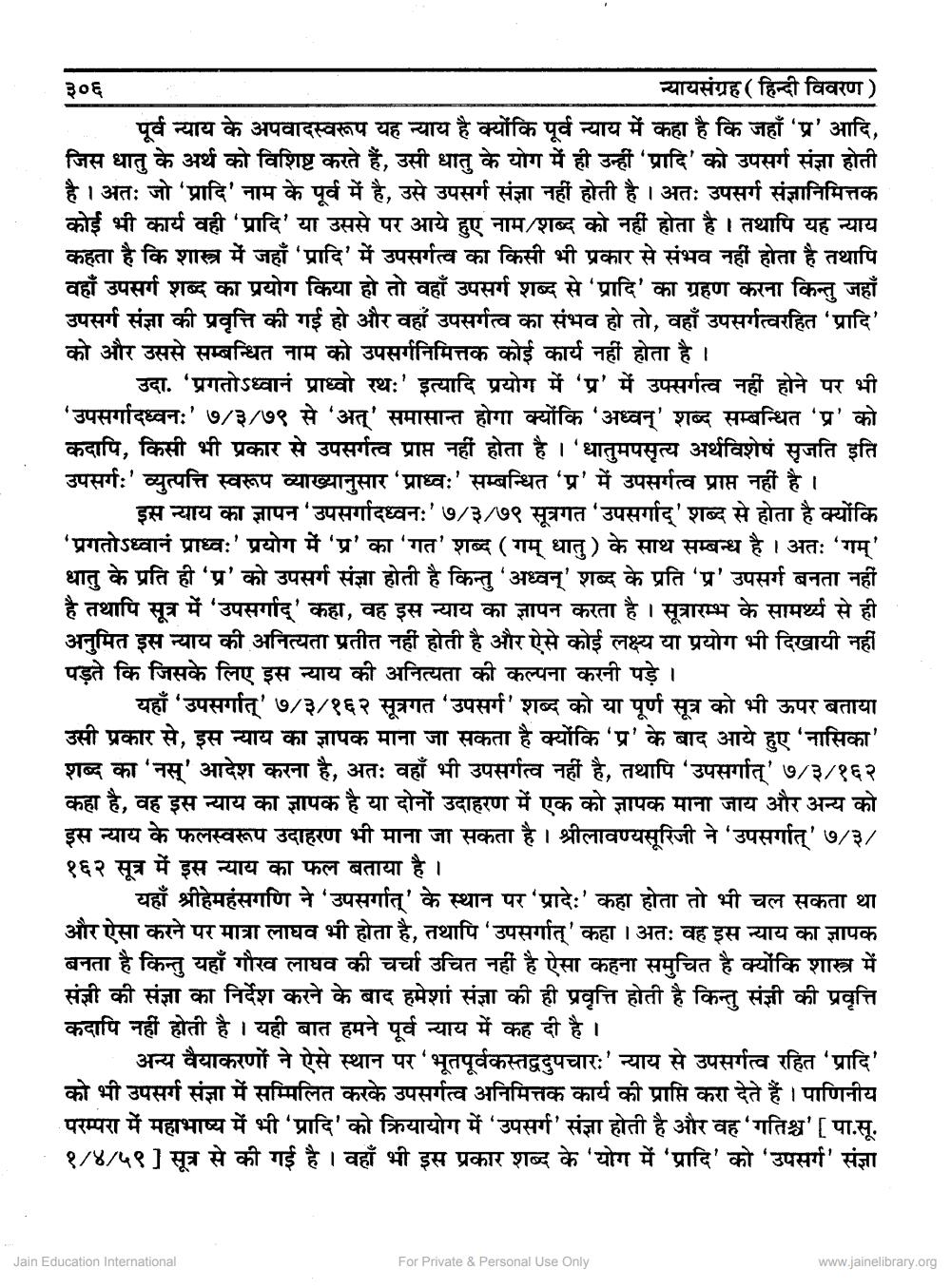________________
न्यायसंग्रह (हिन्दी विवरण) पूर्व न्याय के अपवादस्वरूप यह न्याय है क्योंकि पूर्व न्याय में कहा है कि जहाँ 'प्र' आदि, जिस धातु के अर्थ को विशिष्ट करते हैं, उसी धातु के योग में ही उन्हीं 'प्रादि' को उपसर्ग संज्ञा होती है | अतः जो 'प्रादि' नाम के पूर्व में है, उसे उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है । अतः उपसर्ग संज्ञानिमित्तक कोई भी कार्य वही 'प्रादि' या उससे पर आये हुए नाम / शब्द को नहीं होता है । तथापि यह न्याय कहता है कि शास्त्र में जहाँ 'प्रादि' में उपसर्गत्व का किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता है तथापि वहाँ उपसर्ग शब्द का प्रयोग किया हो तो वहाँ उपसर्ग शब्द से 'प्रादि' का ग्रहण करना किन्तु जहाँ उपसर्ग संज्ञा की प्रवृत्ति की गई हो और वहाँ उपसर्गत्व का संभव हो तो, वहाँ उपसर्गत्वरहित 'प्रादि' को और उससे सम्बन्धित नाम को उपसर्गनिमित्तक कोई कार्य नहीं होता है ।
३०६
उदा. 'प्रगतोऽध्वानं प्राध्वो रथ:' इत्यादि प्रयोग में 'प्र' में उपसर्गत्व नहीं होने पर भी 'उपसर्गादध्वनः' ७/३ / ७९ से 'अत्' समासान्त होगा क्योंकि 'अध्वन्' शब्द सम्बन्धित 'प्र' को कदापि, किसी भी प्रकार से उपसर्गत्व प्राप्त नहीं होता है । 'धातुमपसृत्य अर्थविशेषं सृजति इति उपसर्गः ' व्युत्पत्ति स्वरूप व्याख्यानुसार 'प्राध्वः' सम्बन्धित 'प्र' में उपसर्गत्व प्राप्त नहीं है ।
इस न्याय का ज्ञापन ' उपसर्गादध्वनः ' ७/३/७९ सूत्रगत ' उपसर्गाद्' शब्द से होता क्योंकि 'प्रगतोऽध्वानं प्राध्वः' प्रयोग में 'प्र' का 'गत' शब्द ( गम् धातु) के साथ सम्बन्ध है । अतः 'गम्' धातु के प्रति ही 'प्र' को उपसर्ग संज्ञा होती है किन्तु 'अध्वन्' शब्द के प्रति 'प्र' उपसर्ग बनता नहीं है तथापि सूत्र में 'उपसर्गाद्' कहा, वह इस न्याय का ज्ञापन करता है । सूत्रारम्भ के सामर्थ्य से ही अनुमित इस न्याय की अनित्यता प्रतीत नहीं होती है और ऐसे कोई लक्ष्य या प्रयोग भी दिखायी नहीं पड़ते कि जिसके लिए इस न्याय की अनित्यता की कल्पना करनी पड़े ।
यहाँ 'उपसर्गात्' ७/३/१६२ सूत्रगत ' उपसर्ग' शब्द को या पूर्ण सूत्र को भी ऊपर बताया उसी प्रकार से, इस न्याय का ज्ञापक माना जा सकता है क्योंकि 'प्र' के बाद आये' हुए 'नासिका ' शब्द का 'नस्' आदेश करना है, अतः वहाँ भी उपसर्गत्व नहीं है, तथापि ' उपसर्गात्' ७/३/१६२ कहा है, वह इस न्याय का ज्ञापक है या दोनों उदाहरण में एक को ज्ञापक माना जाय और अन्य को इस न्याय के फलस्वरूप उदाहरण भी माना जा सकता है । श्रीलावण्यसूरिजी ने 'उपसर्गात्' ७/३/ १६२ सूत्र में इस न्याय का फल बताया है ।
यहाँ श्रीमहंसगणि ने 'उपसर्गात्' के स्थान पर 'प्रादेः' कहा होता तो भी चल सकता था और ऐसा करने पर मात्रा लाघव भी होता है, तथापि 'उपसर्गात्' कहा । अतः वह इस न्याय का ज्ञापक बनता है किन्तु यहाँ गौरव लाघव की चर्चा उचित नहीं है ऐसा कहना समुचित है क्योंकि शास्त्र में संज्ञी की संज्ञा का निर्देश करने के बाद हमेशां संज्ञा की ही प्रवृत्ति होती है किन्तु संज्ञी की प्रवृत्ति कदापि नहीं होती है । यही बात हमने पूर्व न्याय में कह दी है ।
अन्य वैयाकरणों ने ऐसे स्थान पर 'भूतपूर्वकस्तद्वदुपचारः ' न्याय से उपसर्गत्व रहित 'प्रादि' को भी उपसर्ग संज्ञा में सम्मिलित करके उपसर्गत्व अनिमित्तक कार्य की प्राप्ति करा देते हैं । पाणिनीय परम्परा में महाभाष्य में भी 'प्रादि' को क्रियायोग में 'उपसर्ग' संज्ञा होती है और वह 'गतिश्च' [ पा.सू. १/४/५९ ] सूत्र से की गई है । वहाँ भी इस प्रकार शब्द के 'योग में 'प्रादि' को 'उपसर्ग' संज्ञा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org