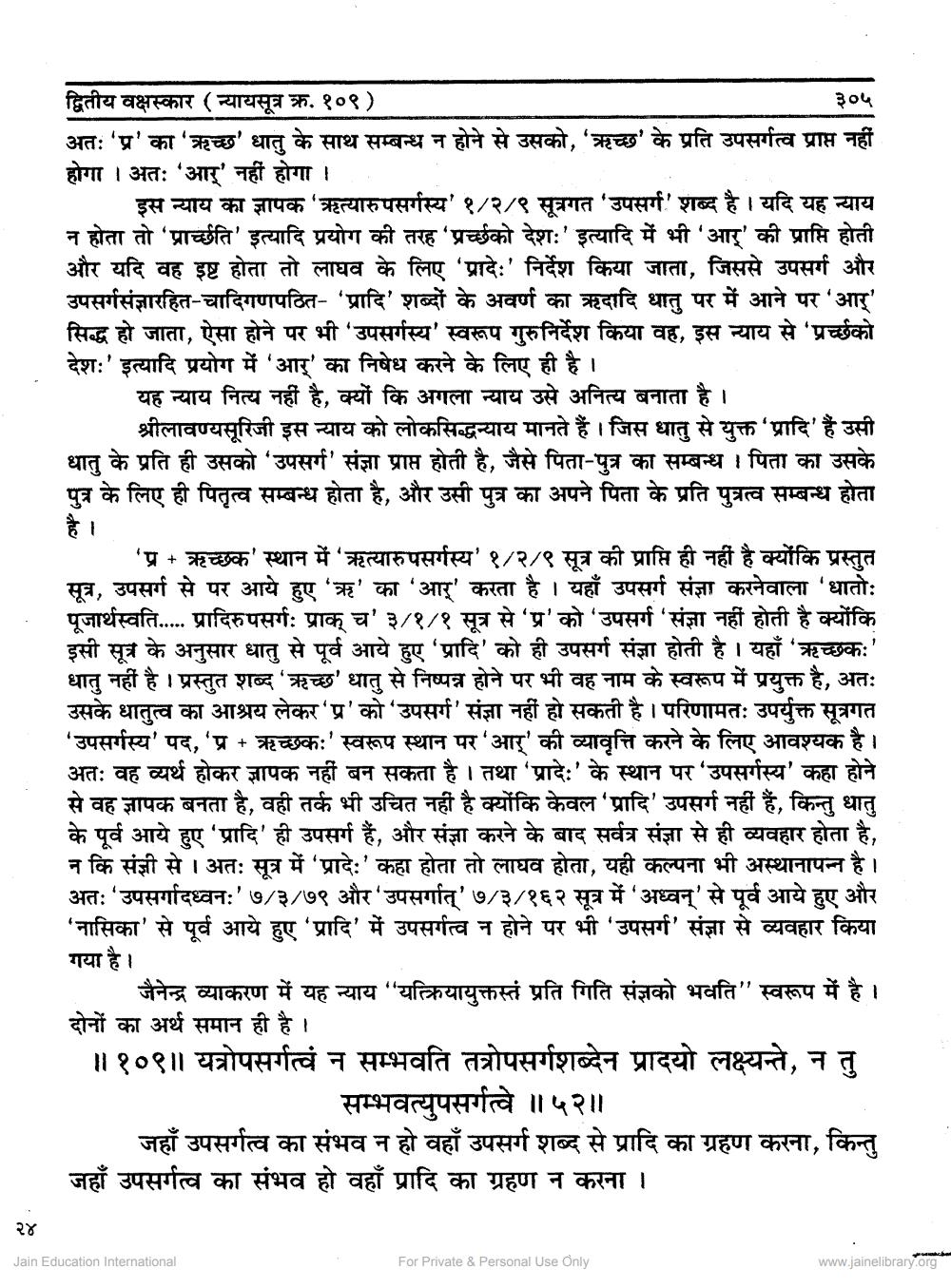________________
૨૪
द्वितीय वक्षस्कार (न्यायसूत्र क्र. १०९ )
३०५
अतः 'प्र' का 'ऋच्छ' धातु के साथ सम्बन्ध न होने से उसको, 'ऋच्छ' के प्रति उपसर्गत्व प्राप्त नहीं होगा । अतः 'आर्' नहीं होगा ।
इस न्याय का ज्ञापक 'ऋत्यारुपसर्गस्य' १/२/९ सूत्रगत 'उपसर्ग' शब्द है । यदि यह न्याय न होता तो 'प्रार्च्छति' इत्यादि प्रयोग की तरह 'प्रछेको देश:' इत्यादि में भी 'आर्' की प्राप्ति होती और यदि वह इष्ट होता तो लाघव के लिए 'प्रादे:' निर्देश किया जाता, जिससे उपसर्ग और उपसर्गसंज्ञारहित-चादिगणपठित- 'प्रादि' शब्दों के अवर्ण का ऋदादि धातु पर में आने पर 'आर्' सिद्ध हो जाता, ऐसा होने पर भी 'उपसर्गस्य' स्वरूप गुरुनिर्देश किया वह, इस न्याय से 'प्रर्च्छको देश:' इत्यादि प्रयोग में 'आर्' का निषेध करने के लिए ही है ।
यह न्याय नित्य नहीं है, क्यों कि अगला न्याय उसे अनित्य बनाता है ।
श्री लावण्यसूरिजी इस न्याय को लोकसिद्धन्याय मानते हैं। जिस धातु से युक्त 'प्रादि' हैं उसी धातु के प्रति ही उसको 'उपसर्ग' संज्ञा प्राप्त होती है, जैसे पिता-पुत्र का सम्बन्ध । पिता का उसके पुत्र के लिए ही पितृत्व सम्बन्ध होता है, और उसी पुत्र का अपने पिता के प्रति पुत्रत्व सम्बन्ध होता है ।
1
'प्र + ऋच्छक' स्थान में 'ऋत्यारुपसर्गस्य' १ / २ / ९ सूत्र की प्राप्ति ही नहीं है क्योंकि प्रस्तुत सूत्र, उपसर्ग से पर आये हुए 'ऋ' का 'आर्' करता है । यहाँ उपसर्ग संज्ञा करनेवाला 'धातोः पूजार्थस्वति...... प्रादिरुपसर्गः प्राक् च' ३/१/१ सूत्र से 'प्र' को 'उपसर्ग 'संज्ञा नहीं होती है क्योंकि इसी सूत्र के अनुसार धातु से पूर्व आये हुए 'प्रादि' को ही उपसर्ग संज्ञा होती है। यहाँ 'ऋच्छकः ' धातु नहीं है । प्रस्तुत शब्द 'ऋच्छ' धातु से निष्पन्न होने पर भी वह नाम के स्वरूप में प्रयुक्त है, अतः उसके धातुत्व का आश्रय लेकर 'प्र' को 'उपसर्ग' संज्ञा नहीं हो सकती है। परिणामतः उपर्युक्त सूत्रगत ‘उपसर्गस्य' पद, ‘प्र + ऋच्छक: ' स्वरूप स्थान पर 'आर' की व्यावृत्ति करने के लिए आवश्यक है अतः वह व्यर्थ होकर ज्ञापक नहीं बन सकता है । तथा 'प्रादेः' के स्थान पर 'उपसर्गस्य' कहा होने से वह ज्ञापक बनता है, वही तर्क भी उचित नहीं है क्योंकि केवल 'प्रादि' उपसर्ग नहीं हैं, किन्तु धातु
1
पूर्व आये हुए 'प्रादि' ही उपसर्ग हैं, और संज्ञा करने के बाद सर्वत्र संज्ञा से ही व्यवहार होता है, न कि संज्ञी से । अतः सूत्र में 'प्रादेः' कहा होता तो लाघव होता, यही कल्पना भी अस्थानापन्न है । अतः ‘उपसर्गादध्वनः' ७/३ / ७९ और 'उपसर्गात्' ७/३/१६२ सूत्र में 'अध्वन्' से पूर्व आये हुए और 'नासिका' से पूर्व आये हुए 'प्रादि' में उपसर्गत्व न होने पर भी 'उपसर्ग' संज्ञा से व्यवहार किया गया है ।
जैनेन्द्र व्याकरण में यह न्याय " यत्क्रियायुक्तस्तं प्रति गिति संज्ञको भवति" स्वरूप में है । दोनों का अर्थ समान ही है ।
॥ १०९॥ यत्रोपसर्गत्वं न सम्भवति तत्रोपसर्गशब्देन प्रादयो लक्ष्यन्ते, न तु सम्भवत्युपसर्गत्वे ॥५२॥
जहाँ उपसर्गत्व का संभव न हो वहाँ उपसर्ग शब्द से प्रादि का ग्रहण करना, किन्तु जहाँ उपसर्गत्व का संभव हो वहाँ प्रादि का ग्रहण न करना ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org