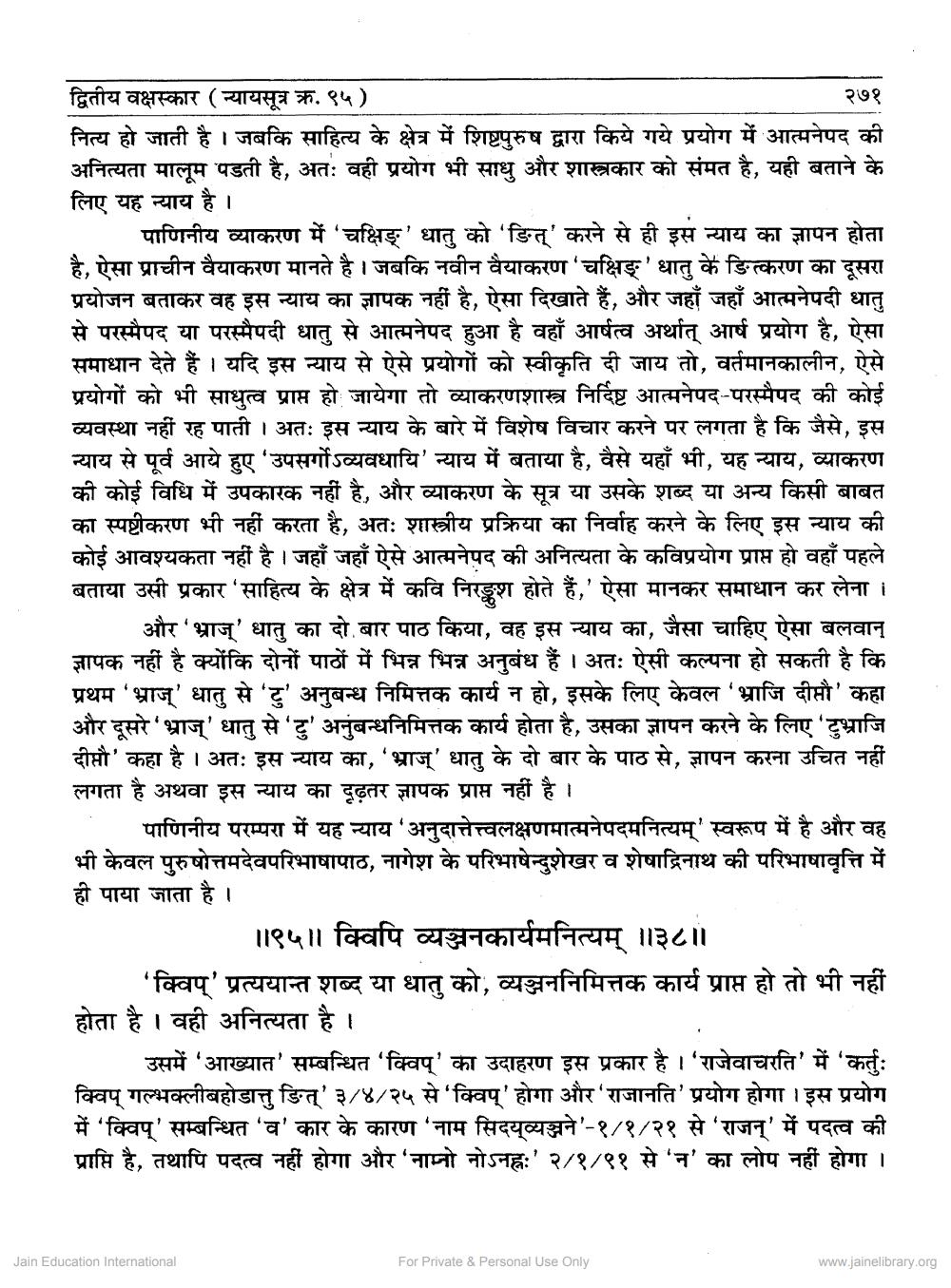________________
द्वितीय वक्षस्कार (न्यायसूत्र क्र. ९५)
२७१ नित्य हो जाती है। जबकि साहित्य के क्षेत्र में शिष्टपुरुष द्वारा किये गये प्रयोग में आत्मनेपद की अनित्यता मालूम पड़ती है, अतः वही प्रयोग भी साधु और शास्त्रकार को संमत है, यही बताने के लिए यह न्याय है।
पाणिनीय व्याकरण में 'चक्षिङ्' धातु को 'ङित्' करने से ही इस न्याय का ज्ञापन होता है, ऐसा प्राचीन वैयाकरण मानते है । जबकि नवीन वैयाकरण 'चक्षिङ्' धातु के ङित्करण का दूसरा प्रयोजन बताकर वह इस न्याय का ज्ञापक नहीं है, ऐसा दिखाते हैं, और जहाँ जहाँ आत्मनेपदी धातु से परस्मैपद या परस्मैपदी धातु से आत्मनेपद हुआ है वहाँ आर्षत्व अर्थात् आर्ष प्रयोग है, ऐसा समाधान देते हैं । यदि इस न्याय से ऐसे प्रयोगों को स्वीकृति दी जाय तो, वर्तमानकालीन, ऐसे प्रयोगों को भी साधुत्व प्राप्त हो जायेगा तो व्याकरणशास्त्र निर्दिष्ट आत्मनेपद-परस्मैपद की कोई व्यवस्था नहीं रह पाती। अतः इस न्याय के बारे में विशेष विचार करने पर लगता है कि जैसे, इस न्याय से पूर्व आये हुए 'उपसर्गोऽव्यवधायि' न्याय में बताया है, वैसे यहाँ भी, यह न्याय, व्याकरण की कोई विधि में उपकारक नहीं है, और व्याकरण के सूत्र या उसके शब्द या अन्य किसी बाबत का स्पष्टीकरण भी नहीं करता है, अतः शास्त्रीय प्रक्रिया का निर्वाह करने के लिए इस न्याय की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ ऐसे आत्मनेपद की अनित्यता के कविप्रयोग प्राप्त हो वहाँ पहले बताया उसी प्रकार 'साहित्य के क्षेत्र में कवि निरङ्कुश होते हैं, ऐसा मानकर समाधान कर लेना ।
और 'भ्राज्' धातु का दो बार पाठ किया, वह इस न्याय का, जैसा चाहिए ऐसा बलवान ज्ञापक नहीं है क्योंकि दोनों पाठों में भिन्न भिन्न अनुबंध हैं । अतः ऐसी कल्पना हो सकती है कि प्रथम 'भ्राज्' धातु से 'टु' अनुबन्ध निमित्तक कार्य न हो, इसके लिए केवल 'भ्राजि दीप्तौ' कहा
और दूसरे 'भ्राज्' धातु से 'टु' अनुबन्धनिमित्तक कार्य होता है, उसका ज्ञापन करने के लिए 'टुभ्राजि दीप्तौ' कहा है । अत: इस न्याय का, 'भ्राज्' धातु के दो बार के पाठ से, ज्ञापन करना उचित नहीं लगता है अथवा इस न्याय का दृढ़तर ज्ञापक प्राप्त नहीं है।
पाणिनीय परम्परा में यह न्याय 'अनुदात्तेत्त्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्' स्वरूप में है और वह भी केवल पुरुषोत्तमदेवपरिभाषापाठ, नागेश के परिभाषेन्दुशेखर व शेषाद्रिनाथ की परिभाषावृत्ति में ही पाया जाता है।
॥९५॥ क्विपि व्यञ्जनकार्यमनित्यम् ॥३८॥ 'क्विप्' प्रत्ययान्त शब्द या धातु को, व्यञ्जननिमित्तक कार्य प्राप्त हो तो भी नहीं होता है । वही अनित्यता है ।
उसमें 'आख्यात' सम्बन्धित 'क्विप्' का उदाहरण इस प्रकार है । 'राजेवाचरति' में 'कर्तुः क्विप् गल्भक्लीबहोडात्तु ङित्' ३/४/२५ से 'क्विप्' होगा और 'राजानति' प्रयोग होगा। इस प्रयोग में 'क्विप्' सम्बन्धित 'व' कार के कारण 'नाम सिदय्व्यञ्जने'-१/१/२१ से 'राजन्' में पदत्व की प्राप्ति है, तथापि पदत्व नहीं होगा और 'नाम्नो नोऽनह्नः' २/१/९१ से 'न' का लोप नहीं होगा।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org