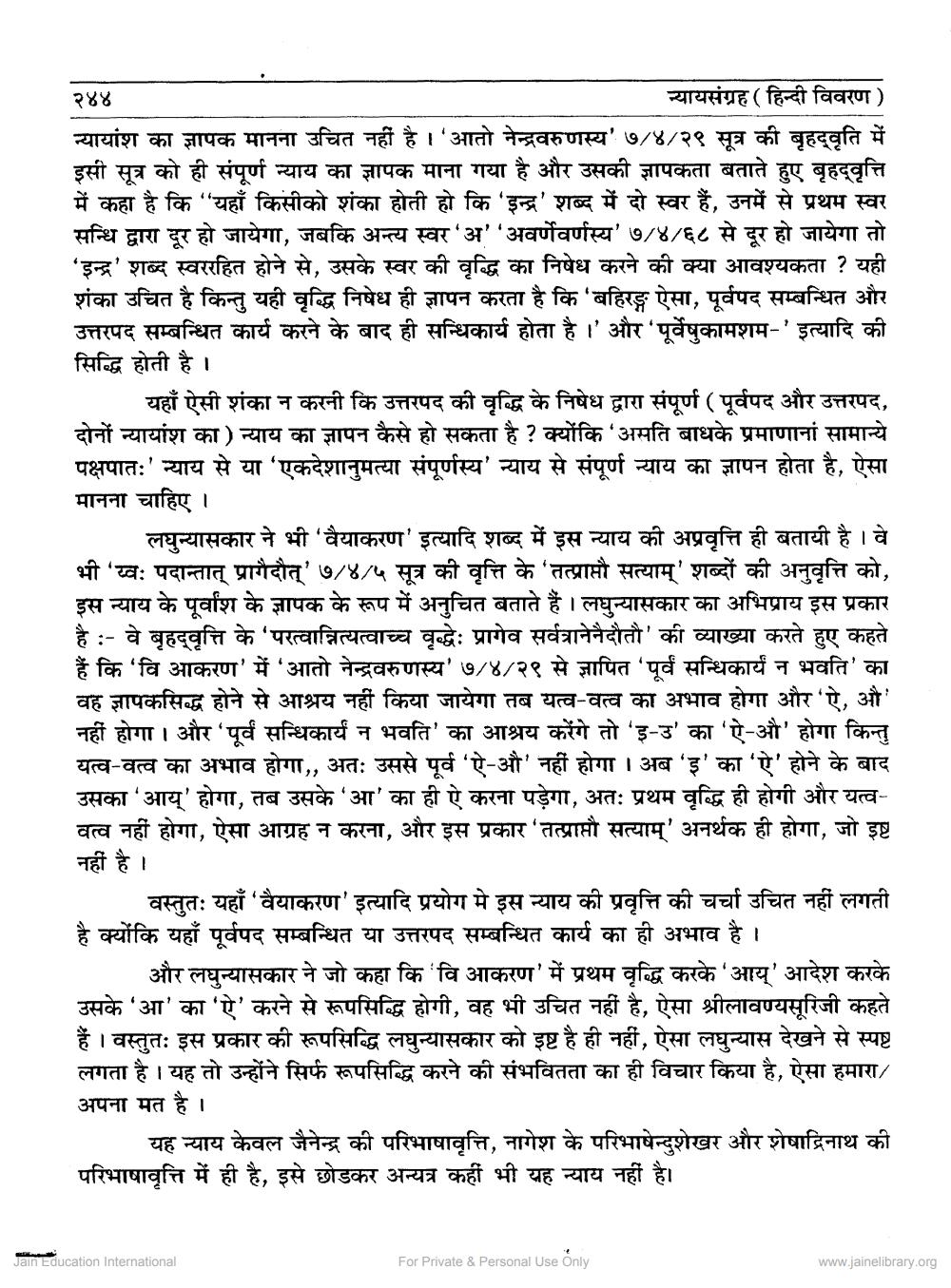________________
२४४
न्यायसंग्रह (हिन्दी विवरण) न्यायांश का ज्ञापक मानना उचित नहीं है । 'आतो नेन्द्रवरुणस्य' ७/४/२९ सूत्र की बृहद्वृति में इसी सूत्र को ही संपूर्ण न्याय का ज्ञापक माना गया है और उसकी ज्ञापकता बताते हुए बृहद्वृत्ति में कहा है कि "यहाँ किसीको शंका होती हो कि 'इन्द्र' शब्द में दो स्वर हैं, उनमें से प्रथम स्वर सन्धि द्वारा दूर हो जायेगा, जबकि अन्त्य स्वर 'अ' 'अवर्णेवर्णस्य' ७/४/६८ से दूर हो जायेगा तो 'इन्द्र' शब्द स्वररहित होने से, उसके स्वर की वृद्धि का निषेध करने की क्या आवश्यकता ? यही शंका उचित है किन्तु यही वृद्धि निषेध ही ज्ञापन करता है कि 'बहिरङ्ग ऐसा, पूर्वपद सम्बन्धित और उत्तरपद सम्बन्धित कार्य करने के बाद ही सन्धिकार्य होता है ।' और 'पूर्वेषुकामशम-' इत्यादि की सिद्धि होती है।
यहाँ ऐसी शंका न करनी कि उत्तरपद की वृद्धि के निषेध द्वारा संपूर्ण (पूर्वपद और उत्तरपद, दोनों न्यायांश का) न्याय का ज्ञापन कैसे हो सकता है ? क्योंकि 'असति बाधके प्रमाणानां सामान्ये पक्षपात:' न्याय से या 'एकदेशानुमत्या संपूर्णस्य' न्याय से संपूर्ण न्याय का ज्ञापन होता है, ऐसा मानना चाहिए।
लघुन्यासकार ने भी 'वैयाकरण' इत्यादि शब्द में इस न्याय की अप्रवृत्ति ही बतायी है । वे भी 'य्वः पदान्तात् प्रागैदौत्' ७/४/५ सूत्र की वृत्ति के 'तत्प्राप्तौ सत्याम्' शब्दों की अनुवृत्ति को, इस न्याय के पूर्वांश के ज्ञापक के रूप में अनुचित बताते हैं । लघुन्यासकार का अभिप्राय इस प्रकार है :- वे बृहद्वृत्ति के 'परत्वान्नित्यत्वाच्च वृद्धेः प्रागेव सर्वत्रानेनैदौतौ' की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 'वि आकरण' में 'आतो नेन्द्रवरुणस्य' ७/४/२९ से ज्ञापित ‘पूर्वं सन्धिकार्यं न भवति' का वह ज्ञापकसिद्ध होने से आश्रय नहीं किया जायेगा तब यत्व-वत्व का अभाव होगा और 'ऐ, औ' नहीं होगा। और 'पूर्वं सन्धिकार्यं न भवति' का आश्रय करेंगे तो 'इ-उ' का 'ऐ-औ' होगा किन्तु यत्व-वत्व का अभाव होगा,, अतः उससे पूर्व 'ऐ-औ' नहीं होगा । अब 'इ' का 'ऐ' होने के बाद उसका 'आय' होगा, तब उसके 'आ' का ही ऐ करना पड़ेगा, अत: प्रथम वृद्धि ही होगी और यत्ववत्व नहीं होगा, ऐसा आग्रह न करना, और इस प्रकार 'तत्प्राप्तौ सत्याम्' अनर्थक ही होगा, जो इष्ट नहीं है।
वस्तुतः यहाँ 'वैयाकरण' इत्यादि प्रयोग मे इस न्याय की प्रवृत्ति की चर्चा उचित नहीं लगती है क्योंकि यहाँ पर्वपद सम्बन्धित या उत्तरपद सम्बन्धित कार्य का ही अभाव है।
__ और लघुन्यासकार ने जो कहा कि 'वि आकरण' में प्रथम वृद्धि करके 'आय' आदेश करके उसके 'आ' का 'ऐ' करने से रूपसिद्धि होगी, वह भी उचित नहीं है, ऐसा श्रीलावण्यसूरिजी कहते हैं । वस्तुतः इस प्रकार की रूपसिद्धि लघुन्यासकार को इष्ट है ही नहीं, ऐसा लघुन्यास देखने से स्पष्ट लगता है । यह तो उन्होंने सिर्फ रूपसिद्धि करने की संभवितता का ही विचार किया है, ऐसा हमारा/ अपना मत है ।
यह न्याय केवल जैनेन्द्र की परिभाषावृत्ति, नागेश के परिभाषेन्दुशेखर और शेषाद्रिनाथ की परिभाषावृत्ति में ही है, इसे छोडकर अन्यत्र कहीं भी यह न्याय नहीं है।
Jan Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org