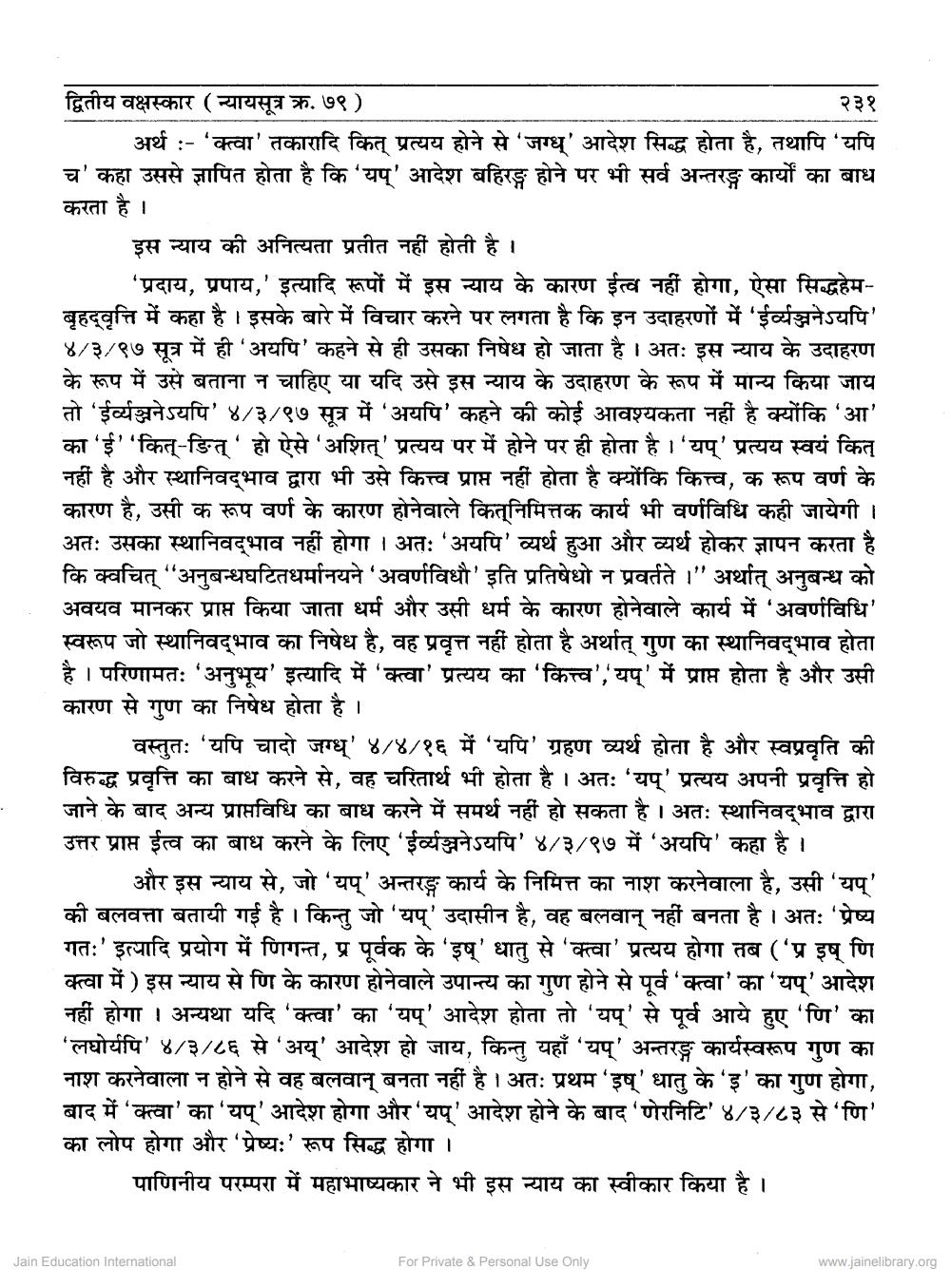________________
द्वितीय वक्षस्कार (न्यायसूत्र क्र. ७९)
२३१ अर्थ :- ‘क्त्वा' तकारादि कित् प्रत्यय होने से 'जग्ध्' आदेश सिद्ध होता है, तथापि 'यपि च' कहा उससे ज्ञापित होता है कि 'यप्' आदेश बहिरङ्ग होने पर भी सर्व अन्तरङ्ग कार्यों का बाध करता है।
इस न्याय की अनित्यता प्रतीत नहीं होती है।
'प्रदाय, प्रपाय,' इत्यादि रूपों में इस न्याय के कारण ईत्व नहीं होगा, ऐसा सिद्धहेमबृहद्वृत्ति में कहा है । इसके बारे में विचार करने पर लगता है कि इन उदाहरणों में 'ईर्व्यञ्जनेऽयपि' ४/३/९७ सूत्र में ही 'अयपि' कहने से ही उसका निषेध हो जाता है । अतः इस न्याय के उदाहरण के रूप में उसे बताना न चाहिए या यदि उसे इस न्याय के उदाहरण के रूप में मान्य किया जाय तो 'ईर्व्यञ्जनेऽयपि' ४/३/९७ सूत्र में 'अयपि' कहने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 'आ' का 'ई' "कित्-ङित् ' हो ऐसे 'अशित्' प्रत्यय पर में होने पर ही होता है । 'यप्' प्रत्यय स्वयं कित् नहीं है और स्थानिवद्भाव द्वारा भी उसे कित्त्व प्राप्त नहीं होता है क्योंकि कित्त्व, क रूप वर्ण के कारण है. उसी क रूप वर्ण के कारण होनेवाले कितनिमित्तक कार्य भी वर्णविधि कही जायेगी। अत: उसका स्थानिवद्भाव नहीं होगा । अतः 'अयपि' व्यर्थ हुआ और व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि क्वचित् "अनुबन्धघटितधर्मानयने 'अवर्णविधौ' इति प्रतिषेधो न प्रवर्तते ।" अर्थात् अनुबन्ध को अवयव मानकर प्राप्त किया जाता धर्म और उसी धर्म के कारण होनेवाले कार्य में 'अवर्णविधि' स्वरूप जो स्थानिवद्भाव का निषेध है, वह प्रवृत्त नहीं होता है अर्थात् गुण का स्थानिवद्भाव होता है । परिणामतः 'अनुभूय' इत्यादि में 'क्त्वा' प्रत्यय का 'कित्त्व', यप्' में प्राप्त होता है और उसी कारण से गण का निषेध होता है ।
वस्तुतः ‘यपि चादो जग्ध्' ४/४/१६ में 'यपि' ग्रहण व्यर्थ होता है और स्वप्रवृति की विरुद्ध प्रवृत्ति का बाध करने से, वह चरितार्थ भी होता है । अतः 'यप्' प्रत्यय अपनी प्रवृत्ति हो जाने के बाद अन्य प्राप्तविधि का बाध करने में समर्थ नहीं हो सकता है । अत: स्थानिवद्भाव द्वारा उत्तर प्राप्त ईत्व का बाध करने के लिए 'ईर्व्यञ्जनेऽयपि' ४/३/९७ में 'अयपि' कहा है।
और इस न्याय से, जो ‘यप्' अन्तरङ्ग कार्य के निमित्त का नाश करनेवाला है, उसी 'यप्' की बलवत्ता बतायी गई है। किन्तु जो 'यप्' उदासीन है, वह बलवान् नहीं बनता है । अतः 'प्रेष्य गतः' इत्यादि प्रयोग में णिगन्त, प्र पूर्वक के 'इष्' धातु से 'क्त्वा' प्रत्यय होगा तब ('प्र इष् णि क्त्वा में ) इस न्याय से णि के कारण होनेवाले उपान्त्य का गुण होने से पूर्व क्त्वा' का 'यप्' आदेश नहीं होगा । अन्यथा यदि 'क्त्वा' का 'यप्' आदेश होता तो ‘यप्' से पूर्व आये हुए 'णि' का 'लघोर्यपि' ४/३/८६ से 'अय्' आदेश हो जाय, किन्तु यहाँ ‘यप्' अन्तरङ्ग कार्यस्वरूप गुण का नाश करनेवाला न होने से वह बलवान् बनता नहीं है। अतः प्रथम 'इष्' धातु के 'इ' का गुण होगा, बाद में ‘क्त्वा' का 'यप्' आदेश होगा और 'यप्' आदेश होने के बाद 'णेरनिटि' ४/३/८३ से "णि' का लोप होगा और 'प्रेष्यः' रूप सिद्ध होगा।
पाणिनीय परम्परा में महाभाष्यकार ने भी इस न्याय का स्वीकार किया है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org