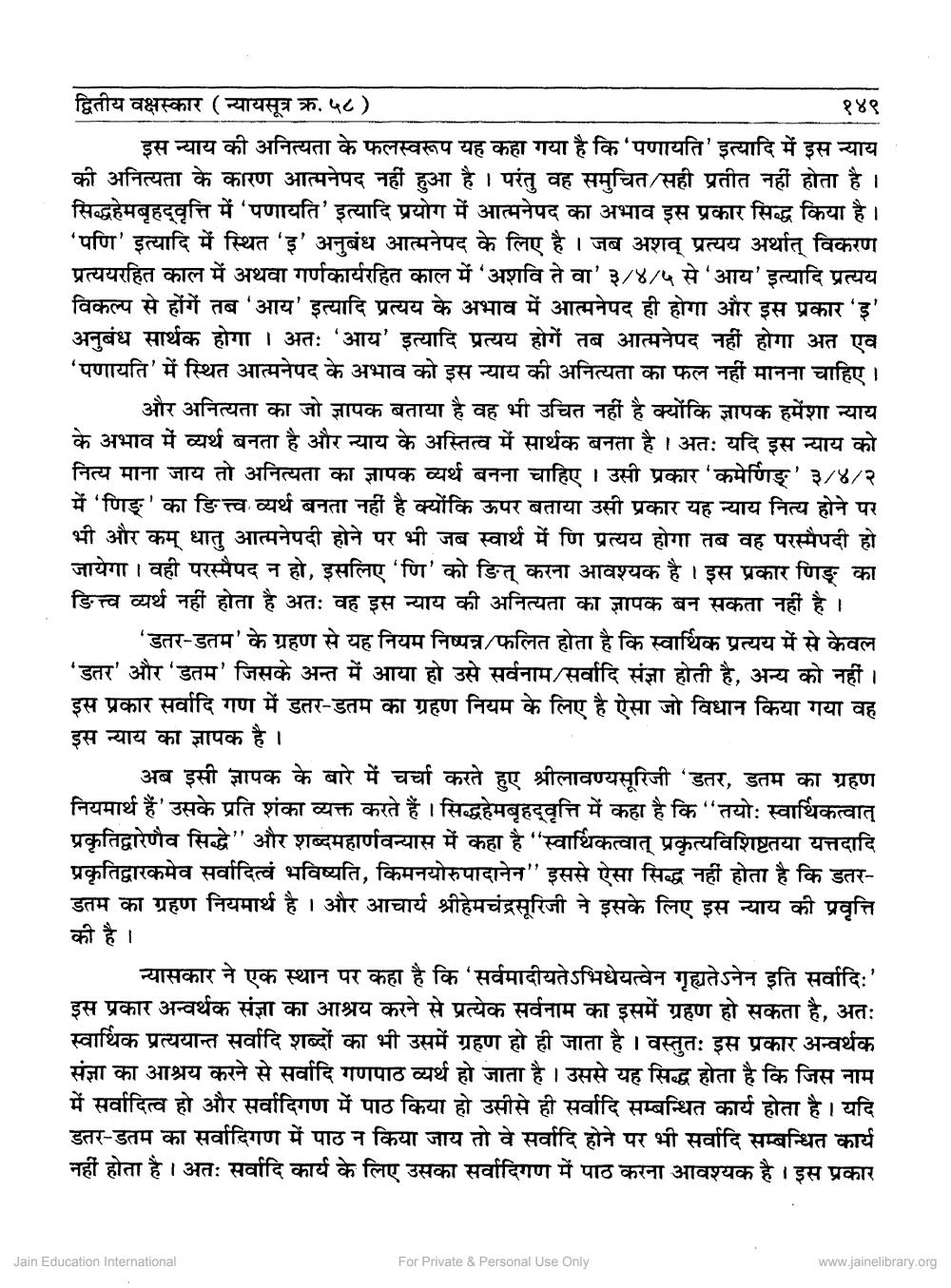________________
द्वितीय वक्षस्कार (न्यायसूत्र क्र. ५८) ।
१४९ इस न्याय की अनित्यता के फलस्वरूप यह कहा गया है कि 'पणायति' इत्यादि में इस न्याय की अनित्यता के कारण आत्मनेपद नहीं हुआ है। परंतु वह समुचित/सही प्रतीत नहीं होता है । सिद्धहेमबृहद्वृत्ति में 'पणायति' इत्यादि प्रयोग में आत्मनेपद का अभाव इस प्रकार सिद्ध किया है। 'पणि' इत्यादि में स्थित 'इ' अनुबंध आत्मनेपद के लिए है । जब अशव् प्रत्यय अर्थात् विकरण प्रत्ययरहित काल में अथवा गर्णकार्यरहित काल में 'अशवि ते वा' ३/४/५ से 'आय' इत्यादि प्रत्यय विकल्प से होंगें तब 'आय' इत्यादि प्रत्यय के अभाव में आत्मनेपद ही होगा और इस प्रकार 'इ' अनुबंध सार्थक होगा । अतः 'आय' इत्यादि प्रत्यय होगें तब आत्मनेपद नहीं होगा अत एव 'पणायति' में स्थित आत्मनेपद के अभाव को इस न्याय की अनित्यता का फल नहीं मानना चाहिए।
और अनित्यता का जो ज्ञापक बताया है वह भी उचित नहीं है क्योंकि ज्ञापक हमेंशा न्याय के अभाव में व्यर्थ बनता है और न्याय के अस्तित्व में सार्थक बनता है । अतः यदि इस न्याय को नित्य माना जाय तो अनित्यता का ज्ञापक व्यर्थ बनना चाहिए । उसी प्रकार 'कमेर्णिङ' ३/४/२ में 'णिङ्' का ङित्त्व व्यर्थ बनता नहीं है क्योंकि ऊपर बताया उसी प्रकार यह न्याय नित्य होने पर भी और कम् धातु आत्मनेपदी होने पर भी जब स्वार्थ में णि प्रत्यय होगा तब वह परस्मैपदी हो जायेगा । वही परस्मैपद न हो, इसलिए 'णि' को ङित् करना आवश्यक है । इस प्रकार णिङ् का ङित्त्व व्यर्थ नहीं होता है अतः वह इस न्याय की अनित्यता का ज्ञापक बन सकता नहीं है।
'डतर-डतम' के ग्रहण से यह नियम निष्पन्न/फलित होता है कि स्वार्थिक प्रत्यय में से केवल 'डतर' और 'डतम' जिसके अन्त में आया हो उसे सर्वनाम/सर्वादि संज्ञा होती है, अन्य को नहीं। इस प्रकार सर्वादि गण में डतर-डतम का ग्रहण नियम के लिए है ऐसा जो विधान किया गया वह इस न्याय का ज्ञापक है ।
अब इसी ज्ञापक के बारे में चर्चा करते हुए श्रीलावण्यसूरिजी 'डतर, डतम का ग्रहण नियमार्थ हैं' उसके प्रति शंका व्यक्त करते हैं । सिद्धहेमबृहद्वृत्ति में कहा है कि "तयोः स्वार्थिकत्वात् प्रकृतिद्वारेणैव सिद्धे" और शब्दमहार्णवन्यास में कहा है "स्वार्थिकत्वात् प्रकृत्यविशिष्टतया यत्तदादि प्रकृतिद्वारकमेव सर्वादित्वं भविष्यति, किमनयोरुपादानेन" इससे ऐसा सिद्ध नहीं होता है कि डतरडतम का ग्रहण नियमार्थ है । और आचार्य श्रीहेमचंद्रसूरिजी ने इसके लिए इस न्याय की प्रवृत्ति की है।
न्यासकार ने एक स्थान पर कहा है कि 'सर्वमादीयतेऽभिधेयत्वेन गृह्यतेऽनेन इति सर्वादिः' इस प्रकार अन्वर्थक संज्ञा का आश्रय करने से प्रत्येक सर्वनाम का इसमें ग्रहण हो सकता है, अतः स्वार्थिक प्रत्ययान्त सर्वादि शब्दों का भी उसमें ग्रहण हो ही जाता है । वस्तुतः इस प्रकार अन्वर्थक संज्ञा का आश्रय करने से सर्वादि गणपाठ व्यर्थ हो जाता है । उससे यह सिद्ध होता है कि जिस नाम में सर्वादित्व हो और सर्वादिगण में पाठ किया हो उसीसे ही सर्वादि सम्बन्धित कार्य होता है। यदि डतर-डतम का सर्वादिगण में पाठ न किया जाय तो वे सर्वादि होने पर भी सर्वादि सम्बन्धित कार्य नहीं होता है। अतः सर्वादि कार्य के लिए उसका सर्वादिगण में पाठ करना आवश्यक है । इस प्रकार
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org