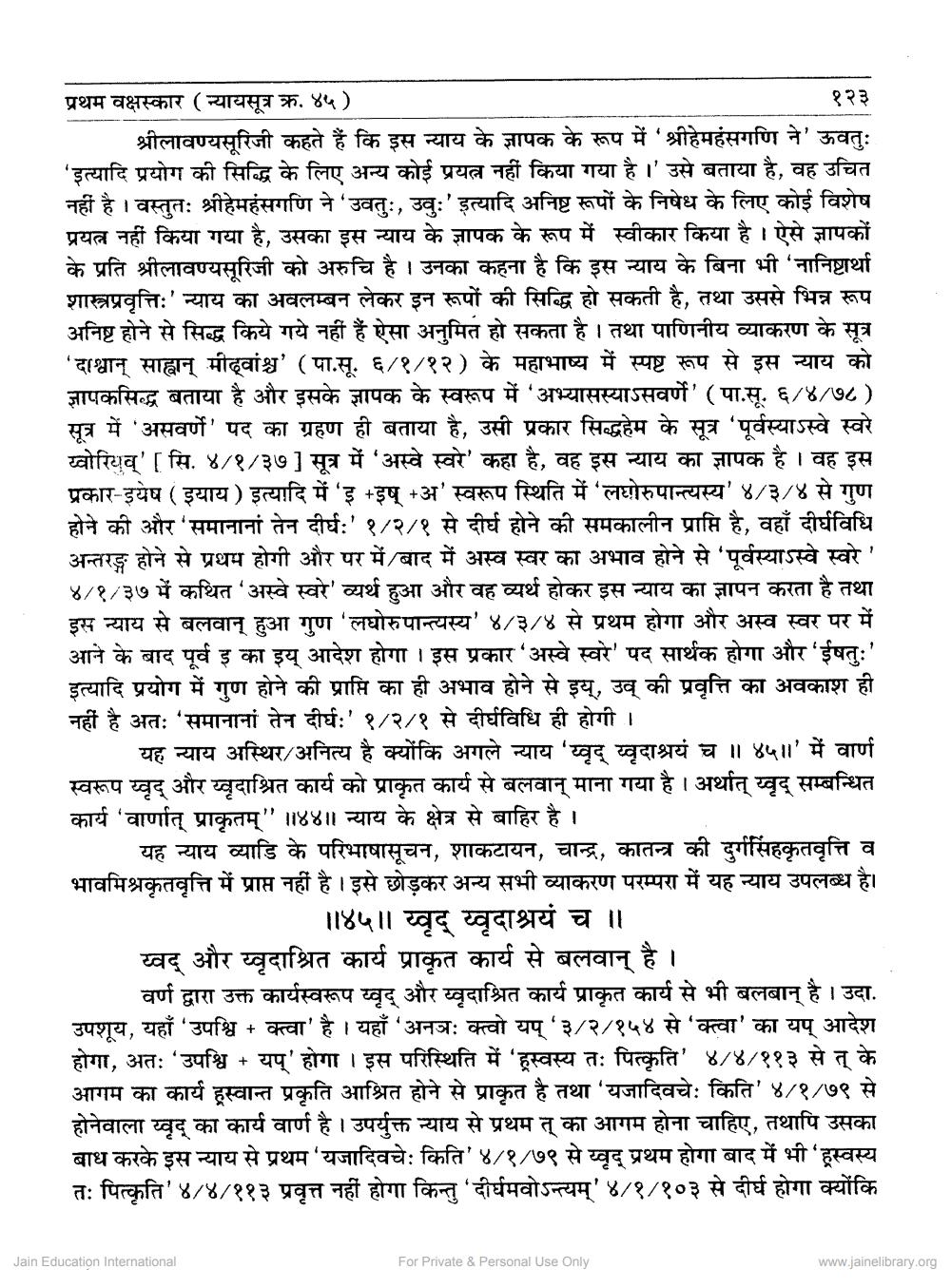________________
प्रथम वक्षस्कार (न्यायसूत्र क्र. ४५)
१२३ श्रीलावण्यसूरिजी कहते हैं कि इस न्याय के ज्ञापक के रूप में 'श्रीहेमहंसगणि ने' ऊवतुः 'इत्यादि प्रयोग की सिद्धि के लिए अन्य कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।' उसे बताया है, वह उचित नहीं है। वस्तुतः श्रीहेमहंसगणि ने 'उवतुः, उवुः' इत्यादि अनिष्ट रूपों के निषेध के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया है, उसका इस न्याय के ज्ञापक के रूप में स्वीकार किया है। ऐसे ज्ञापकों के प्रति श्रीलावण्यसरिजी को अरुचि है। उनका कहना है कि इस न्याय के बिना भी 'नानिवार्था शास्त्रप्रवृत्तिः' न्याय का अवलम्बन लेकर इन रूपों की सिद्धि हो सकती है, तथा उससे भिन्न रूप अनिष्ट होने से सिद्ध किये गये नहीं हैं ऐसा अनुमित हो सकता है । तथा पाणिनीय व्याकरण के सूत्र 'दाश्वान् साह्यान् मीढ्वांश्च' (पा.सू. ६/१/१२) के महाभाष्य में स्पष्ट रूप से इस न्याय को ज्ञापकसिद्ध बताया है और इसके ज्ञापक के स्वरूप में 'अभ्यासस्याऽसवर्णे' (पा.सू. ६/४/७८) सूत्र में 'असवर्णे' पद का ग्रहण ही बताया है, उसी प्रकार सिद्धहेम के सूत्र 'पूर्वस्याऽस्वे स्वरे य्वोरियव्' [ सि. ४/१/३७] सूत्र में 'अस्वे स्वरे' कहा है, वह इस न्याय का ज्ञापक है । वह इस प्रकार-इयेष (इयाय) इत्यादि में 'इ +इष् +अ' स्वरूप स्थिति में लघोरुपान्त्यस्य' ४/३/४ से गुण होने की और 'समानानां तेन दीर्घः' १/२/१ से दीर्घ होने की समकालीन प्राप्ति है, वहाँ दीर्घविधि अन्तरङ्ग होने से प्रथम होगी और पर में/बाद में अस्व स्वर का अभाव होने से 'पूर्वस्याऽस्वे स्वरे' ४/१/३७ में कथित 'अस्वे स्वरे' व्यर्थ हुआ और वह व्यर्थ होकर इस न्याय का ज्ञापन करता है तथा इस न्याय से बलवान् हुआ गुण 'लघोरुपान्त्यस्य' ४/३/४ से प्रथम होगा और अस्व स्वर पर में आने के बाद पूर्व इ का इय् आदेश होगा । इस प्रकार अस्वे स्वरे' पद सार्थक होगा और 'ईषतुः' इत्यादि प्रयोग में गुण होने की प्राप्ति का ही अभाव होने से इय्, उव् की प्रवृत्ति का अवकाश ही नहीं है अतः 'समानानां तेन दीर्घः' १/२/१ से दीर्घविधि ही होगी ।
यह न्याय अस्थिर/अनित्य है क्योंकि अगले न्याय 'वृद् य्वृदाश्रयं च ॥ ४५॥' में वार्ण स्वरूप य्वृद् और य्वदाश्रित कार्य को प्राकृत कार्य से बलवान् माना गया है । अर्थात् य्वृद् सम्बन्धित कार्य 'वार्णात् प्राकृतम्" ॥४४॥ न्याय के क्षेत्र से बाहिर है ।
यह न्याय व्याडि के परिभाषासूचन, शाकटायन, चान्द्र, कातन्त्र की दुर्गसिंहकृतवृत्ति व भावमिश्रकृतवृत्ति में प्राप्त नहीं है । इसे छोड़कर अन्य सभी व्याकरण परम्परा में यह न्याय उपलब्ध है।
॥४५॥ य्वृद् य्वदाश्रयं च ॥ य्वद् और य्वृदाश्रित कार्य प्राकृत कार्य से बलवान् है।
वर्ण द्वारा उक्त कार्यस्वरूप य्वृद् और य्वदाश्रित कार्य प्राकृत कार्य से भी बलबान् है । उदा. उपशूय, यहाँ 'उपश्वि + क्त्वा' है । यहाँ 'अनत्र: क्त्वो यप् '३/२/१५४ से 'क्त्वा' का यप् आदेश होगा, अतः ‘उपश्वि + यप्' होगा । इस परिस्थिति में 'इस्वस्य तः पित्कृति' ४/४/११३ से त् के आगम का कार्य ह्रस्वान्त प्रकृति आश्रित होने से प्राकृत है तथा 'यजादिवचेः किति' ४/१/७९ से होनेवाला य्वृद् का कार्य वार्ण है । उपर्युक्त न्याय से प्रथम त् का आगम होना चाहिए, तथापि उसका बाध करके इस न्याय से प्रथम 'यजादिवचेः किति' ४/१/७९ से य्वृद् प्रथम होगा बाद में भी 'इस्वस्य तः पित्कृति' ४/४/११३ प्रवृत्त नहीं होगा किन्तु 'दीर्घमवोऽन्त्यम्' ४/१/१०३ से दीर्घ होगा क्योंकि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org