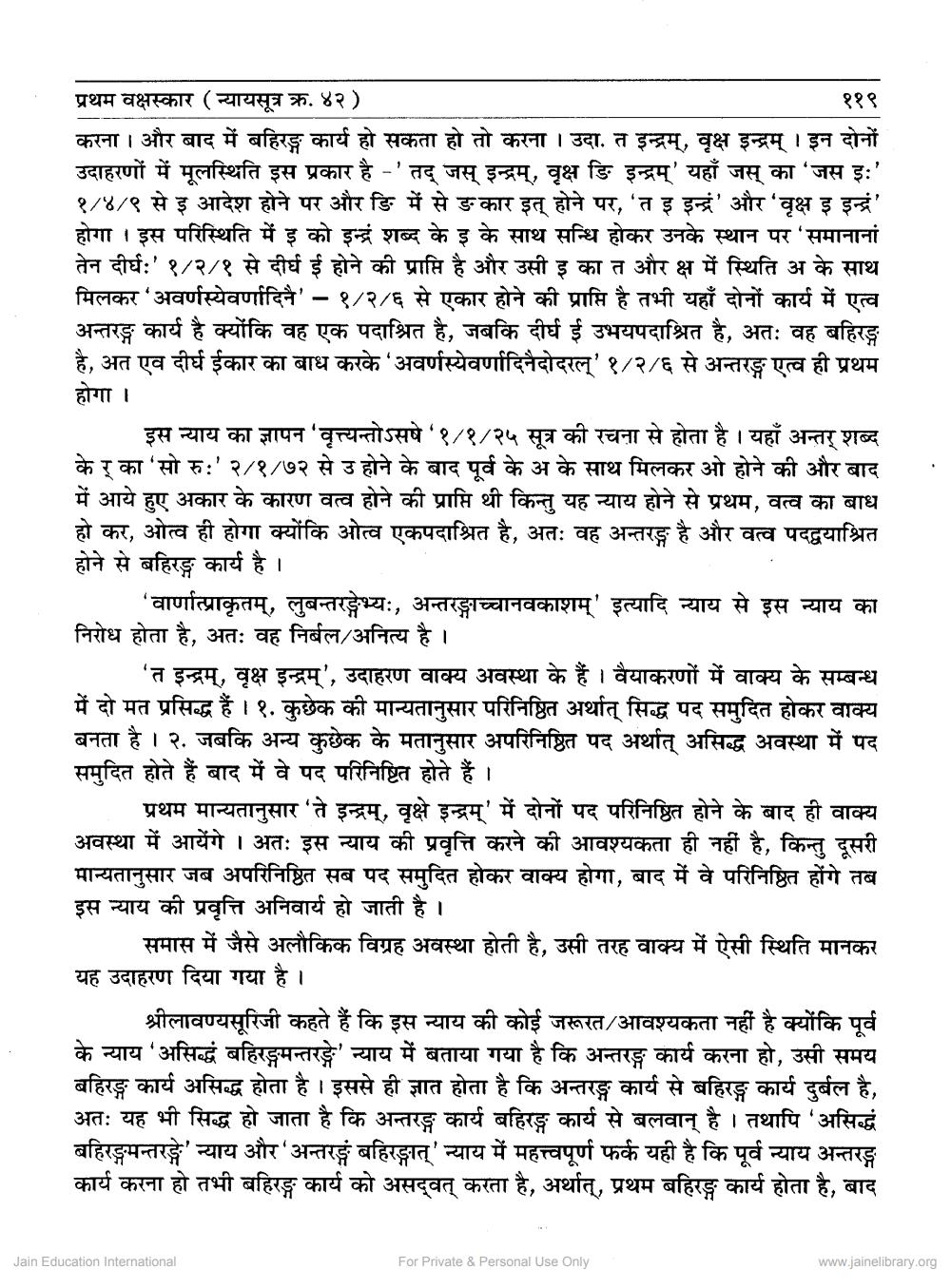________________
११९
प्रथम वक्षस्कार (न्यायसूत्र क्र. ४२) करना । और बाद में बहिरङ्ग कार्य हो सकता हो तो करना । उदा. त इन्द्रम्, वृक्ष इन्द्रम् । इन दोनों उदाहरणों में मूलस्थिति इस प्रकार है - ' तद् जस् इन्द्रम्, वृक्ष ङि इन्द्रम्' यहाँ जस् का 'जस इः' १/४/९ से इ आदेश होने पर और ङि में से ङ कार इत् होने पर, 'त इ इन्द्रं' और 'वृक्ष इ इन्द्रं' होगा। इस परिस्थिति में इको इन्द्रं शब्द के इके साथ सन्धि होकर उनके स्थान पर 'समानानां तेन दीर्घः' १/२/१से दीर्घ ई होने की प्राप्ति है और उसी ड का त और क्ष में स्थिति अके साथ मिलकर 'अवर्णस्येवर्णादिनै' - १/२/६ से एकार होने की प्राप्ति है तभी यहाँ दोनों कार्य में एत्व
अन्तरङ्ग कार्य है क्योंकि वह एक पदाश्रित है, जबकि दीर्घ ई उभयपदाश्रित है, अतः वह बहिरङ्ग है, अत एव दीर्घ ईकार का बाध करके 'अवर्णस्येवर्णादिनैदोदरल्' १/२/६ से अन्तरङ्ग एत्व ही प्रथम होगा।
इस न्याय का ज्ञापन 'वृत्त्यन्तोऽसषे '१/१/२५ सूत्र की रचना से होता है । यहाँ अन्तर् शब्द के र् का ‘सो रुः' २/१/७२ से उ होने के बाद पूर्व के अ के साथ मिलकर ओ होने की और बाद में आये हुए अकार के कारण वत्व होने की प्राप्ति थी किन्तु यह न्याय होने से प्रथम, वत्व का बाध हो कर, ओत्व ही होगा क्योंकि ओत्व एकपदाश्रित है, अतः वह अन्तरङ्ग है और वत्व पदद्वयाश्रित होने से बहिरङ्ग कार्य है।
वार्णात्प्राकृतम्, लुबन्तरङ्गेभ्यः, अन्तरङ्गाच्चानवकाशम्' इत्यादि न्याय से इस न्याय का निरोध होता है, अत: वह निर्बल/अनित्य है।
___ 'त इन्द्रम्, वृक्ष इन्द्रम्', उदाहरण वाक्य अवस्था के हैं । वैयाकरणों में वाक्य के सम्बन्ध में दो मत प्रसिद्ध हैं । १. कुछेक की मान्यतानुसार परिनिष्ठित अर्थात् सिद्ध पद समुदित होकर वाक्य बनता है । २. जबकि अन्य कुछेक के मतानुसार अपरिनिष्ठित पद अर्थात् असिद्ध अवस्था में पद समुदित होते हैं बाद में वे पद परिनिष्टित होते हैं ।
__ प्रथम मान्यतानुसार 'ते इन्द्रम्, वृक्षे इन्द्रम्' में दोनों पद परिनिष्ठित होने के बाद ही वाक्य अवस्था में आयेंगे । अतः इस न्याय की प्रवृत्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है, किन्तु दूसरी मान्यतानुसार जब अपरिनिष्ठित सब पद समुदित होकर वाक्य होगा, बाद में वे परिनिष्ठित होंगे तब इस न्याय की प्रवृत्ति अनिवार्य हो जाती है।
समास में जैसे अलौकिक विग्रह अवस्था होती है, उसी तरह वाक्य में ऐसी स्थिति मानकर यह उदाहरण दिया गया है।
श्रीलावण्यसूरिजी कहते हैं कि इस न्याय की कोई जरूरत/आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूर्व के न्याय 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे' न्याय में बताया गया है कि अन्तरङ्ग कार्य करना हो, उसी समय बहिरङ्ग कार्य असिद्ध होता है । इससे ही ज्ञात होता है कि अन्तरङ्ग कार्य से बहिरङ्ग कार्य दुर्बल है, अतः यह भी सिद्ध हो जाता है कि अन्तरङ्ग कार्य बहिरङ्ग कार्य से बलवान् है । तथापि 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे' न्याय और अन्तरङ्गं बहिरङ्गात्' न्याय में महत्त्वपूर्ण फर्क यही है कि पूर्व न्याय अन्तरङ्ग कार्य करना हो तभी बहिरङ्ग कार्य को असद्वत् करता है, अर्थात्, प्रथम बहिरङ्ग कार्य होता है, बाद
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org