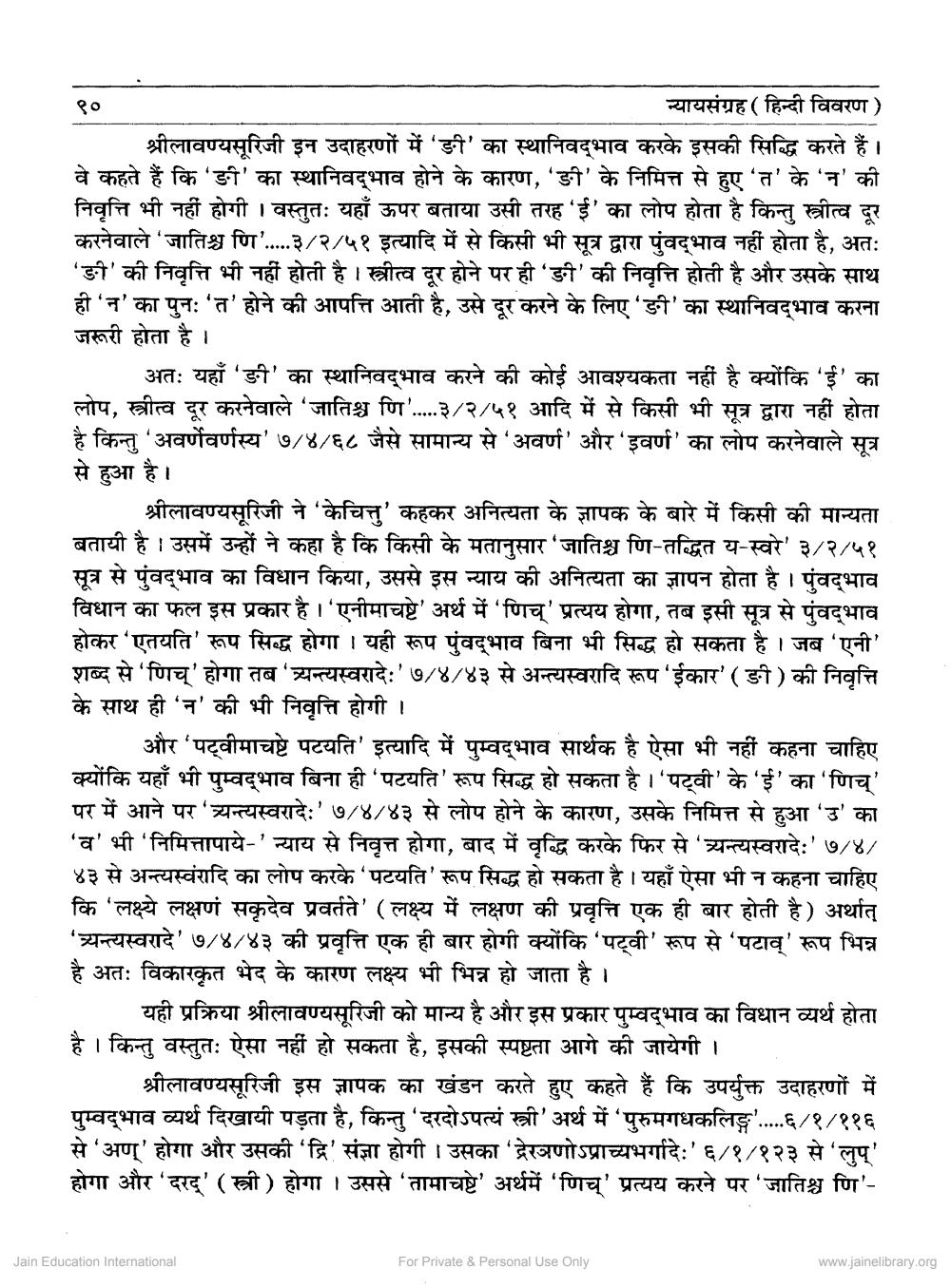________________
न्यायसंग्रह ( हिन्दी विवरण) श्रीलावण्यसूरिजी इन उदाहरणों में 'डी' का स्थानिवद्भाव करके इसकी सिद्धि करते हैं। वे कहते हैं कि 'डी' का स्थानिवद्भाव होने के कारण, 'ङी' के निमित्त से हुए 'त' के 'न' की निवृत्ति भी नहीं होगी । वस्तुतः यहाँ ऊपर बताया उसी तरह 'ई' का लोप होता है किन्तु स्त्रीत्व दूर करनेवाले 'जातिश्च णि'.....३/२/५१ इत्यादि में से किसी भी सूत्र द्वारा पुंवद्भाव नहीं होता है, अतः 'डी' की निवृत्ति भी नहीं होती है । स्त्रीत्व दूर होने पर ही 'डी' की निवृत्ति होती है और उसके साथ ही 'न' का पुनः 'त' होने की आपत्ति आती है, उसे दूर करने के लिए 'ङी' का स्थानिवद्भाव करना जरूरी होता है।
अतः यहाँ 'ङी' का स्थानिवद्भाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 'ई' का लोप, स्त्रीत्व दूर करनेवाले 'जातिश्च णि'.....३/२/५१ आदि में से किसी भी सूत्र द्वारा नहीं होता है किन्तु 'अवर्णेवर्णस्य' ७/४/६८ जैसे सामान्य से 'अवर्ण' और 'इवर्ण' का लोप करनेवाले सूत्र से हुआ है।
श्रीलावण्यसूरिजी ने 'केचित्तु' कहकर अनित्यता के ज्ञापक के बारे में किसी की मान्यता बतायी है। उसमें उन्हों ने कहा है कि किसी के मतानुसार 'जातिश्च णि-तद्धित य-स्वरे' ३/२/५१ सूत्र से पुंवद्भाव का विधान किया, उससे इस न्याय की अनित्यता का ज्ञापन होता है। पुंवद्भाव विधान का फल इस प्रकार है । एनीमाचष्टे' अर्थ में 'णिच्' प्रत्यय होगा, तब इसी सूत्र से पुंवद्भाव होकर एतयति' रूप सिद्ध होगा । यही रूप पुंवद्भाव बिना भी सिद्ध हो सकता है । जब ‘एनी' शब्द से 'णिच्' होगा तब 'त्र्यन्त्यस्वरादेः' ७/४/४३ से अन्त्यस्वरादि रूप 'ईकार' (ङी) की निवृत्ति के साथ ही 'न' की भी निवृत्ति होगी।
और 'पट्वीमाचष्टे पटयति' इत्यादि में पुम्वद्भाव सार्थक है ऐसा भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ भी पुम्वद्भाव बिना ही ‘पटयति' रूप सिद्ध हो सकता है । 'पट्वी' के 'ई' का 'णिच्' पर में आने पर ‘त्र्यन्त्यस्वरादेः' ७/४/४३ से लोप होने के कारण, उसके निमित्त से हुआ 'उ' का 'व' भी 'निमित्तापाये-' न्याय से निवृत्त होगा, बाद में वृद्धि करके फिर से 'त्र्यन्त्यस्वरादेः' ७/४/ ४३ से अन्त्यस्वरादि का लोप करके ‘पटयति' रूप सिद्ध हो सकता है । यहाँ ऐसा भी न कहना चाहिए कि 'लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते' (लक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति एक ही बार होती है) अर्थात् 'त्र्यन्त्यस्वरादे' ७/४/४३ की प्रवृत्ति एक ही बार होगी क्योंकि 'पट्वी' रूप से 'पटाव्' रूप भिन्न है अतः विकारकृत भेद के कारण लक्ष्य भी भिन्न हो जाता है।
यही प्रक्रिया श्रीलावण्यसूरिजी को मान्य है और इस प्रकार पुम्वद्भाव का विधान व्यर्थ होता है । किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं हो सकता है, इसकी स्पष्टता आगे की जायेगी ।
श्रीलावण्यसूरिजी इस ज्ञापक का खंडन करते हुए कहते हैं कि उपर्युक्त उदाहरणों में पुम्वद्भाव व्यर्थ दिखायी पड़ता है, किन्तु 'दरदोऽपत्यं स्त्री' अर्थ में 'पुरुमगधकलिङ्ग'.....६/१/११६ से 'अण्' होगा और उसकी ‘द्रि' संज्ञा होगी । उसका 'द्रेरणोऽप्राच्यभर्गादेः' ६/१/१२३ से लुप्' होगा और 'दरद्' (स्त्री) होगा । उससे 'तामाचष्टे' अर्थमें 'णिच्' प्रत्यय करने पर 'जातिश्च णि'
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org