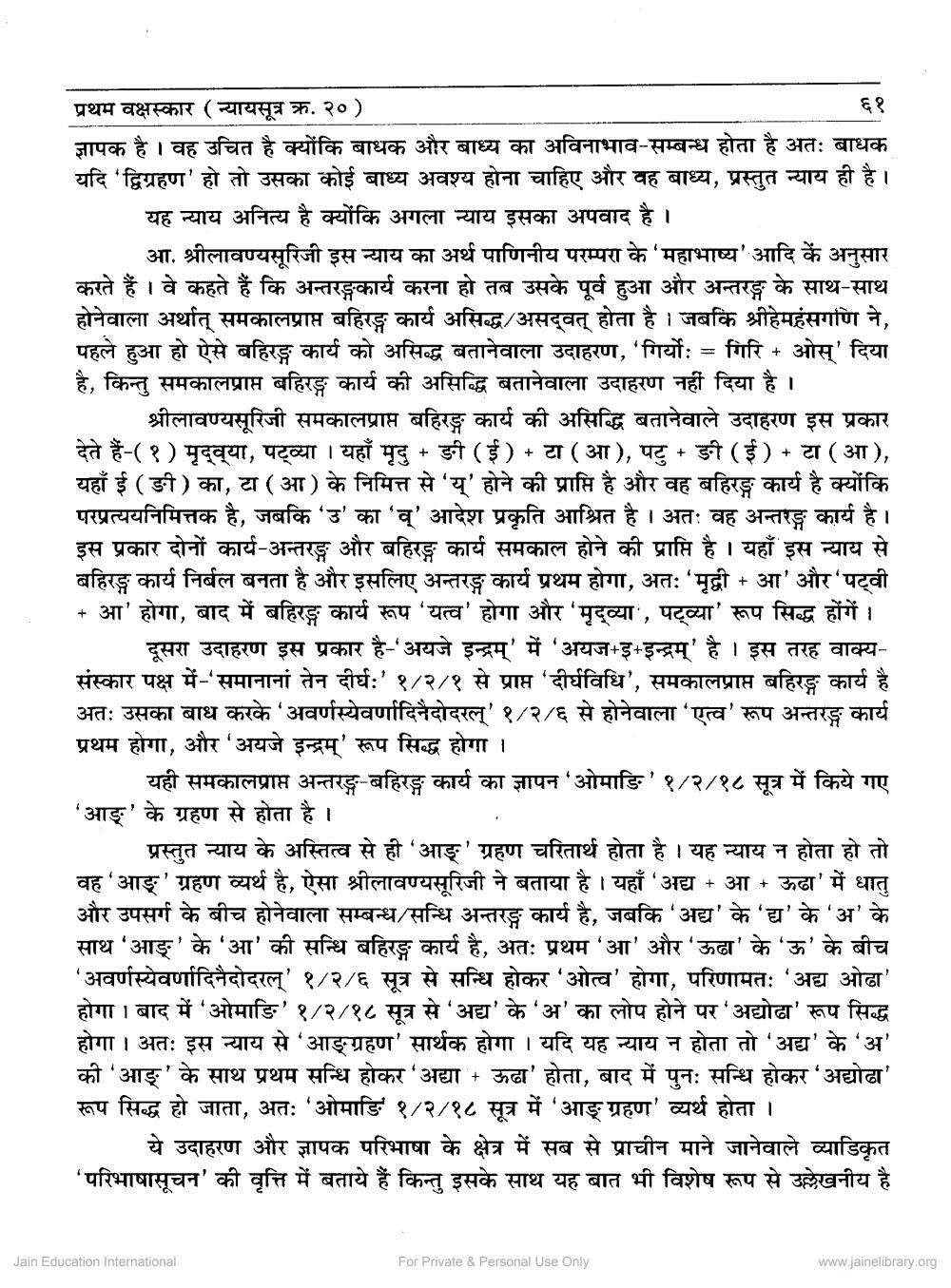________________
प्रथम वक्षस्कार (न्यायसूत्र क्र. २०) ज्ञापक है । वह उचित है क्योंकि बाधक और बाध्य का अविनाभाव-सम्बन्ध होता है अतः बाधक यदि 'द्विग्रहण' हो तो उसका कोई बाध्य अवश्य होना चाहिए और वह बाध्य, प्रस्तुत न्याय ही है।
यह न्याय अनित्य है क्योंकि अगला न्याय इसका अपवाद है।
आ. श्रीलावण्यसूरिजी इस न्याय का अर्थ पाणिनीय परम्परा के 'महाभाष्य' आदि के अनुसार करते हैं । वे कहते हैं कि अन्तरङ्गकार्य करना हो तब उसके पूर्व हुआ और अन्तरङ्ग के साथ-साथ होनेवाला अर्थात् समकालप्राप्त बहिरङ्ग कार्य असिद्ध/असद्वत् होता है । जबकि श्रीहेमहंसगणि ने, पहले हुआ हो ऐसे बहिरङ्ग कार्य को असिद्ध बतानेवाला उदाहरण, 'गिर्योः = गिरि + ओस्' दिया है, किन्तु समकालप्राप्त बहिरङ्ग कार्य की असिद्धि बतानेवाला उदाहरण नहीं दिया है।
श्रीलावण्यसूरिजी समकालप्राप्त बहिरङ्ग कार्य की असिद्धि बतानेवाले उदाहरण इस प्रकार देते हैं-(१) मृव्या , पटव्या । यहाँ मृदु + ङी (ई) + टा (आ), पटु + ङी (ई) + टा (आ), यहाँ ई (ङी) का, टा (आ) के निमित्त से 'य' होने की प्राप्ति है और वह बहिरङ्ग कार्य है क्योंकि परप्रत्ययनिमित्तक है, जबकि 'उ' का 'व्' आदेश प्रकृति आश्रित है । अतः वह अन्तरङ्ग कार्य है। इस प्रकार दोनों कार्य-अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग कार्य समकाल होने की प्राप्ति है । यहाँ इस न्याय से बहिरङ्ग कार्य निर्बल बनता है और इसलिए अन्तरङ्ग कार्य प्रथम होगा, अतः 'मृद्वी + आ' और 'पट्वी + आ' होगा, बाद में बहिरङ्ग कार्य रूप 'यत्व' होगा और 'मृद्व्या, पव्या' रूप सिद्ध होंगे।
__ दूसरा उदाहरण इस प्रकार है-'अयजे इन्द्रम्' में 'अयज+इ+इन्द्रम्' है । इस तरह वाक्यसंस्कार पक्ष में-'समानानां तेन दीर्घः' १/२/१ से प्राप्त 'दीर्घविधि', समकालप्राप्त बहिरङ्ग कार्य है अत: उसका बाध करके 'अवर्णस्येवर्णादिनैदोदरल्' १/२/६ से होनेवाला 'एत्व' रूप अन्तरङ्ग कार्य प्रथम होगा, और 'अयजे इन्द्रम्' रूप सिद्ध होगा।
यही समकालप्राप्त अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग कार्य का ज्ञापन 'ओमाङि' १/२/१८ सूत्र में किये गए 'आङ्' के ग्रहण से होता है।
प्रस्तुत न्याय के अस्तित्व से ही 'आङ्' ग्रहण चरितार्थ होता है । यह न्याय न होता हो तो वह 'आङ्' ग्रहण व्यर्थ है, ऐसा श्रीलावण्यसूरिजी ने बताया है। यहाँ 'अद्य + आ + ऊढा' में धातु
और उपसर्ग के बीच होनेवाला सम्बन्ध/सन्धि अन्तरङ्ग कार्य है, जबकि 'अद्य' के 'द्य' के 'अ' के साथ 'आङ्' के 'आ' की सन्धि बहिरङ्ग कार्य है, अत: प्रथम 'आ' और 'ऊढा' के 'ऊ' के बीच 'अवर्णस्येवर्णादिनैदोदरल्' १/२/६ सूत्र से सन्धि होकर 'ओत्व' होगा, परिणामतः ‘अद्य ओढा' होगा । बाद में 'ओमाङि' १/२/१८ सूत्र से 'अद्य' के 'अ' का लोप होने पर अद्योढा' रूप सिद्ध होगा। अत: इस न्याय से 'आङ्ग्रहण' सार्थक होगा । यदि यह न्याय न होता तो 'अद्य' के 'अ' की 'आङ्' के साथ प्रथम सन्धि होकर 'अद्या + ऊढा' होता, बाद में पुनः सन्धि होकर 'अद्योढा' रूप सिद्ध हो जाता, अतः 'ओमाङि १/२/१८ सूत्र में 'आङ्ग्रहण' व्यर्थ होता ।
ये उदाहरण और ज्ञापक परिभाषा के क्षेत्र में सब से प्राचीन माने जानेवाले व्याडिकृत 'परिभाषासूचन' की वृत्ति में बताये हैं किन्तु इसके साथ यह बात भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org