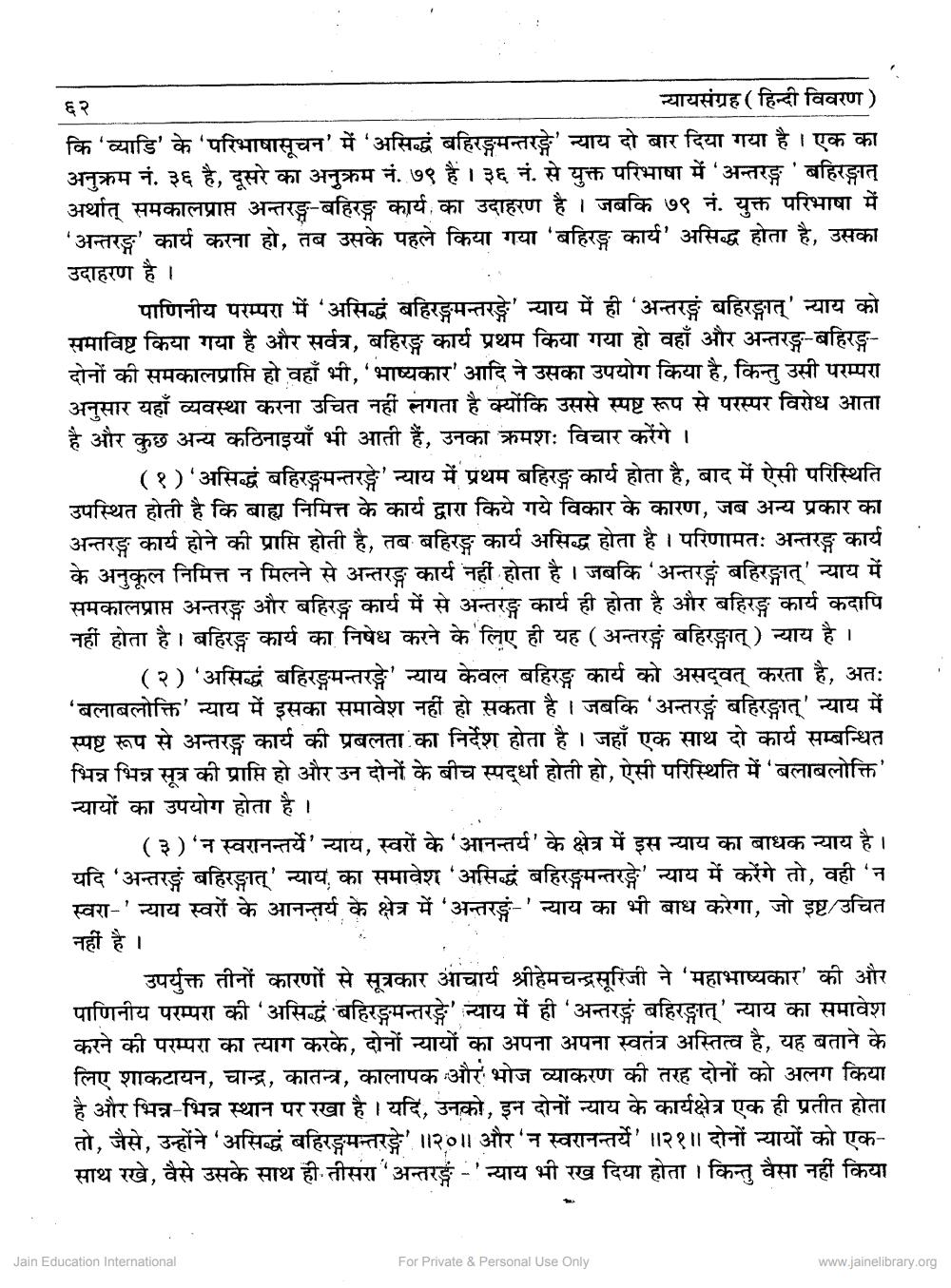________________
६२
न्यायसंग्रह ( हिन्दी विवरण )
कि 'व्याडि ' के 'परिभाषासूचन' में 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे' न्याय दो बार दिया गया है। एक का अनुक्रम नं. ३६ है, दूसरे का अनुक्रम नं. ७९ हैं । ३६ नं. से युक्त परिभाषा में 'अन्तरङ्ग ' बहिरङ्गात् अर्थात् समकालप्राप्त अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग कार्य का उदाहरण है । जबकि ७९ नं. युक्त परिभाषा में 'अन्तरङ्ग' कार्य करना हो, तब उसके पहले किया गया 'बहिरङ्ग कार्य' असिद्ध होता है, उसका उदाहरण है ।
पाणिनीय परम्परा में 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे' न्याय ही 'अन्तरङ्गं बहिरङ्गात्' न्याय को समाविष्ट किया गया है और सर्वत्र, बहिरङ्ग कार्य प्रथम किया गया हो वहाँ और अन्तरङ्ग-बहिरङ्गदोनों की समकालप्राप्ति हो वहाँ भी, ' भाष्यकार' आदि ने उसका उपयोग किया है, किन्तु उसी परम्परा अनुसार यहाँ व्यवस्था करना उचित नहीं लगता है क्योंकि उससे स्पष्ट रूप से परस्पर विरोध आता है और कुछ अन्य कठिनाइयाँ भी आती हैं, उनका क्रमशः विचार करेंगे ।
( १ ) 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे' न्याय में प्रथम बहिरङ्ग कार्य होता है, बाद में ऐसी परिस्थिति उपस्थित होती है कि बाह्य निमित्त के कार्य द्वारा किये गये विकार के कारण, जब अन्य प्रकार का अन्तरङ्ग कार्य होने की प्राप्ति होती है, तब बहिरङ्ग कार्य असिद्ध होता है । परिणामतः अन्तरङ्ग कार्य के अनुकूल निमित्त न मिलने से अन्तरङ्ग कार्य नहीं होता है। जबकि 'अन्तरङ्गं बहिरङ्गात्' न्याय में समकालप्राप्त अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग कार्य में से अन्तरङ्ग कार्य ही होता है और बहिरङ्ग कार्य कदापि नहीं होता है । बहिरङ्ग कार्य का निषेध करने के लिए ही यह ( अन्तरङ्गं बहिरङ्गात् ) न्याय है ।
(२) 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे' न्याय केवल बहिरङ्ग कार्य को असद्वत् करता है, अतः 'बलाबलोक्ति' न्याय में इसका समावेश नहीं हो सकता है । जबकि 'अन्तरङ्ग बहिरङ्गात्' न्याय में स्पष्ट रूप से अन्तरङ्ग कार्य की प्रबलता का निर्देश होता है । जहाँ एक साथ दो कार्य सम्बन्धित भिन्न भिन्न सूत्र की प्राप्ति हो और उन दोनों के बीच स्पर्धा होती हो, ऐसी परिस्थिति में 'बलाबलोक्ति' न्यायों का उपयोग होता है ।
( ३ ) 'न स्वरानन्तर्ये' न्याय, स्वरों के 'आनन्तर्य' के क्षेत्र में इस न्याय का बाधक न्याय है | यदि 'अन्तरङ्गं बहिरङ्गात्' न्याय का समावेश 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे' न्याय में करेंगे तो, वही 'न स्वरा - ' न्याय स्वरों के आनन्तर्य के क्षेत्र में 'अन्तरङ्गं - ' न्याय का भी बाध करेगा, जो इष्ट / उचित नहीं है ।
उपर्युक्त तीनों कारणों से सूत्रकार आचार्य श्रीहेमचन्द्रसूरिजी ने 'महाभाष्यकार' की और पाणिनीय परम्परा की 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे' न्याय में ही 'अन्तरङ्गं बहिरङ्गात्' न्याय का समावेश करने की परम्परा का त्याग करके, दोनों न्यायों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, यह बताने के लिए शाकटायन, चान्द्र, कातन्त्र, कालापक और भोज व्याकरण की तरह दोनों को अलग किया है और भिन्न-भिन्न स्थान पर रखा है। यदि, उनको, इन दोनों न्याय के कार्यक्षेत्र एक ही प्रतीत होता तो, जैसे, उन्होंने 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे' ॥२०॥ और 'न स्वरानन्तर्ये' ॥ २१ ॥ दोनों न्यायों को एकसाथ रखे, वैसे उसके साथ ही तीसरा ' अन्तरङ्ग - न्याय भी रख दिया होता । किन्तु वैसा नहीं किया
,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org