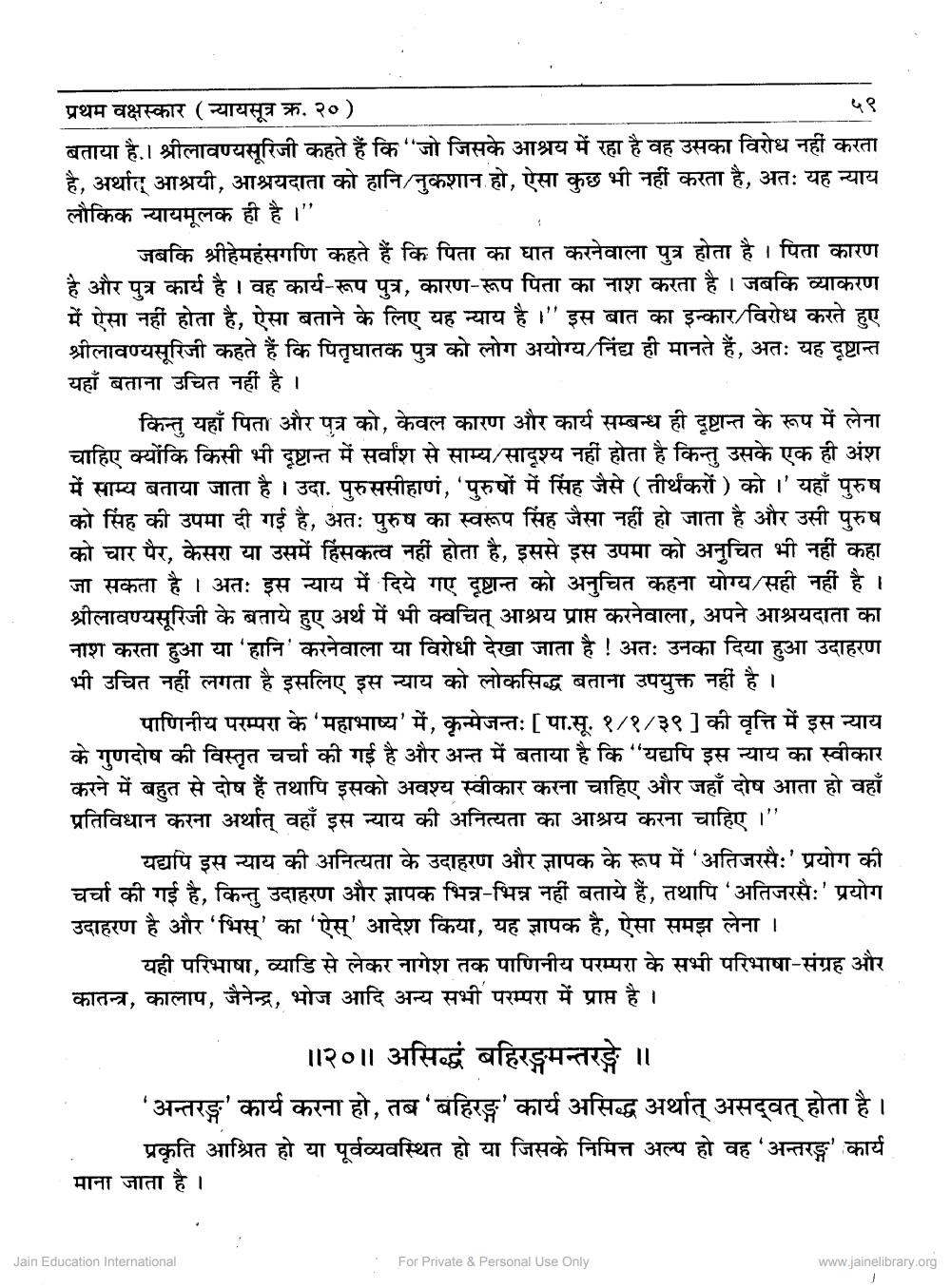________________
प्रथम वक्षस्कार (न्यायसूत्र क्र. २०) बताया है.। श्रीलावण्यसूरिजी कहते हैं कि "जो जिसके आश्रय में रहा है वह उसका विरोध नहीं करता है, अर्थात् आश्रयी, आश्रयदाता को हानि/नुकशान हो, ऐसा कुछ भी नहीं करता है, अतः यह न्याय लौकिक न्यायमूलक ही है।"
जबकि श्रीहेमहंसगणि कहते हैं कि पिता का घात करनेवाला पुत्र होता है । पिता कारण है और पुत्र कार्य है । वह कार्य-रूप पुत्र, कारण-रूप पिता का नाश करता है । जबकि व्याकरण में ऐसा नहीं होता है, ऐसा बताने के लिए यह न्याय है।" इस बात का इन्कार/विरोध करते हुए श्रीलावण्यसूरिजी कहते हैं कि पितृघातक पुत्र को लोग अयोग्य/ निंद्य ही मानते हैं, अतः यह दृष्टान्त यहाँ बताना उचित नहीं है।
किन्तु यहाँ पिता और पुत्र को, केवल कारण और कार्य सम्बन्ध ही दृष्टान्त के रूप में लेना चाहिए क्योंकि किसी भी दृष्टान्त में सर्वांश से साम्य/सादृश्य नहीं होता है किन्तु उसके एक ही अंश में साम्य बताया जाता है । उदा. पुरुससीहाणं, 'पुरुषों में सिंह जैसे (तीर्थंकरों) को ।' यहाँ पुरुष को सिंह की उपमा दी गई है, अतः पुरुष का स्वरूप सिंह जैसा नहीं हो जाता है और उसी पुरुष को चार पैर, केसरा या उसमें हिंसकत्व नहीं होता है, इससे इस उपमा को अनुचित भी नहीं कहा जा सकता है । अतः इस न्याय में दिये गए दृष्टान्त को अनुचित कहना योग्य/सही नहीं है । श्रीलावण्यसरिजी के बताये हए अर्थ में भी क्वचित आश्रय प्राप्त करनेवाला, अपने आश्रयदाता का नाश करता हुआ या 'हानि करनेवाला या विरोधी देखा जाता है ! अतः उनका दिया हुआ उदाहरण भी उचित नहीं लगता है इसलिए इस न्याय को लोकसिद्ध बताना उपयुक्त नहीं है।
पाणिनीय परम्परा के 'महाभाष्य' में, कृन्मेजन्त: [ पा.सू. १/१/३९ ] की वृत्ति में इस न्याय के गुणदोष की विस्तृत चर्चा की गई है और अन्त में बताया है कि "यद्यपि इस न्याय का स्वीकार करने में बहुत से दोष हैं तथापि इसको अवश्य स्वीकार करना चाहिए और जहाँ दोष आता हो वहाँ प्रतिविधान करना अर्थात् वहाँ इस न्याय की अनित्यता का आश्रय करना चाहिए ।'
यद्यपि इस न्याय की अनित्यता के उदाहरण और ज्ञापक के रूप में 'अतिजरसैः' प्रयोग की चर्चा की गई है, किन्तु उदाहरण और ज्ञापक भिन्न-भिन्न नहीं बताये हैं, तथापि 'अतिजरसैः' प्रयोग उदाहरण है और 'भिस्' का 'ऐस्' आदेश किया, यह ज्ञापक है, ऐसा समझ लेना ।।
यही परिभाषा, व्याडि से लेकर नागेश तक पाणिनीय परम्परा के सभी परिभाषा-संग्रह और कातन्त्र, कालाप, जैनेन्द्र, भोज आदि अन्य सभी परम्परा में प्राप्त है।
॥२०॥ असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥ 'अन्तरङ्ग' कार्य करना हो, तब 'बहिरङ्ग' कार्य असिद्ध अर्थात् असद्वत् होता है।
प्रकृति आश्रित हो या पूर्वव्यवस्थित हो या जिसके निमित्त अल्प हो वह 'अन्तरङ्ग' कार्य माना जाता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org