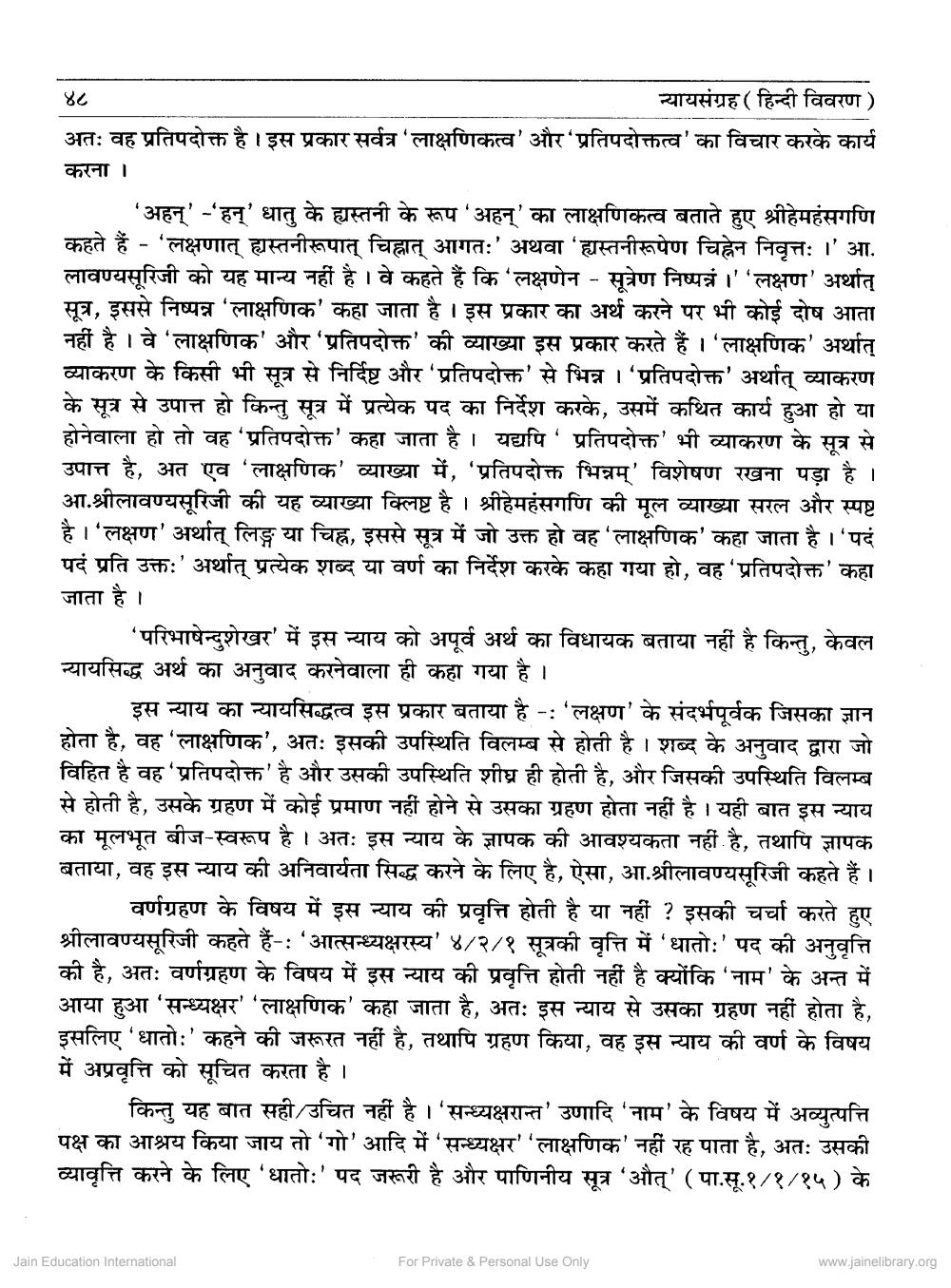________________
४८
न्यायसंग्रह (हिन्दी विवरण) अतः वह प्रतिपदोक्त है। इस प्रकार सर्वत्र लाक्षणिकत्व' और 'प्रतिपदोक्तत्व' का विचार करके कार्य करना।
'अहन्' -'हन्' धातु के शस्तनी के रूप 'अहन्' का लाक्षणिकत्व बताते हुए श्रीहेमहंसगणि कहते हैं - ‘लक्षणात् हस्तनीरूपात् चिह्नात् आगतः' अथवा 'ह्यस्तनीरूपेण चिह्नन निवृत्तः ।' आ. लावण्यसूरिजी को यह मान्य नहीं है । वे कहते हैं कि 'लक्षणेन - सूत्रेण निष्पन्नं ।' 'लक्षण' अर्थात् सूत्र, इससे निष्पन्न 'लाक्षणिक' कहा जाता है । इस प्रकार का अर्थ करने पर भी कोई दोष आता नहीं है । वे 'लाक्षणिक' और 'प्रतिपदोक्त' की व्याख्या इस प्रकार करते हैं । 'लाक्षणिक' अर्थात् व्याकरण के किसी भी सूत्र से निर्दिष्ट और 'प्रतिपदोक्त' से भिन्न । 'प्रतिपदोक्त' अर्थात् व्याकरण के सूत्र से उपात्त हो किन्तु सूत्र में प्रत्येक पद का निर्देश करके, उसमें कथित कार्य हुआ हो या होनेवाला हो तो वह 'प्रतिपदोक्त' कहा जाता है। यद्यपि — प्रतिपदोक्त' भी व्याकरण के सूत्र से उपात्त है, अत एव 'लाक्षणिक' व्याख्या में, 'प्रतिपदोक्त भिन्नम्' विशेषण रखना पड़ा है । आ.श्रीलावण्यसूरिजी की यह व्याख्या क्लिष्ट है । श्रीहेमहंसगणि की मूल व्याख्या सरल और स्पष्ट है। ‘लक्षण' अर्थात् लिङ्ग या चिह्न, इससे सूत्र में जो उक्त हो वह 'लाक्षणिक' कहा जाता है । ‘पदं पदं प्रति उक्तः' अर्थात् प्रत्येक शब्द या वर्ण का निर्देश करके कहा गया हो, वह 'प्रतिपदोक्त' कहा जाता है।
'परिभाषेन्दुशेखर' में इस न्याय को अपूर्व अर्थ का विधायक बताया नहीं है किन्तु, केवल न्यायसिद्ध अर्थ का अनुवाद करनेवाला ही कहा गया है।
इस न्याय का न्यायसिद्धत्व इस प्रकार बताया है -: 'लक्षण' के संदर्भपूर्वक जिसका ज्ञान होता है, वह 'लाक्षणिक', अतः इसकी उपस्थिति विलम्ब से होती है। शब्द के अनुवाद द्वारा जो विहित है वह 'प्रतिपदोक्त' है और उसकी उपस्थिति शीघ्र ही होती है, और जिसकी उपस्थिति विलम्ब से होती है, उसके ग्रहण में कोई प्रमाण नहीं होने से उसका ग्रहण होता नहीं है। यही बात इस न्याय का मूलभूत बीज-स्वरूप है । अत: इस न्याय के ज्ञापक की आवश्यकता नहीं है, तथापि ज्ञापक बताया, वह इस न्याय की अनिवार्यता सिद्ध करने के लिए है, ऐसा, आ.श्रीलावण्यसूरिजी कहते हैं।
___ वर्णग्रहण के विषय में इस न्याय की प्रवृत्ति होती है या नहीं ? इसकी चर्चा करते हुए श्रीलावण्यसूरिजी कहते हैं-: 'आत्सन्ध्यक्षरस्य' ४/२/१ सूत्रकी वृत्ति में 'धातोः' पद की अनुवृत्ति की है, अतः वर्णग्रहण के विषय में इस न्याय की प्रवृत्ति होती नहीं है क्योंकि 'नाम' के अन्त में आया हुआ 'सन्ध्यक्षर' 'लाक्षणिक' कहा जाता है, अतः इस न्याय से उसका ग्रहण नहीं होता है, इसलिए 'धातोः' कहने की जरूरत नहीं है, तथापि ग्रहण किया, वह इस न्याय की वर्ण के विषय में अप्रवृत्ति को सूचित करता है।
किन्तु यह बात सही/उचित नहीं है । 'सन्ध्यक्षरान्त' उणादि 'नाम' के विषय में अव्युत्पत्ति पक्ष का आश्रय किया जाय तो 'गो' आदि में 'सन्ध्यक्षर' 'लाक्षणिक' नहीं रह पाता है, अत: उसकी व्यावृत्ति करने के लिए 'धातोः' पद जरूरी है और पाणिनीय सूत्र ‘औत्' (पा.सू.१/१/१५) के
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org